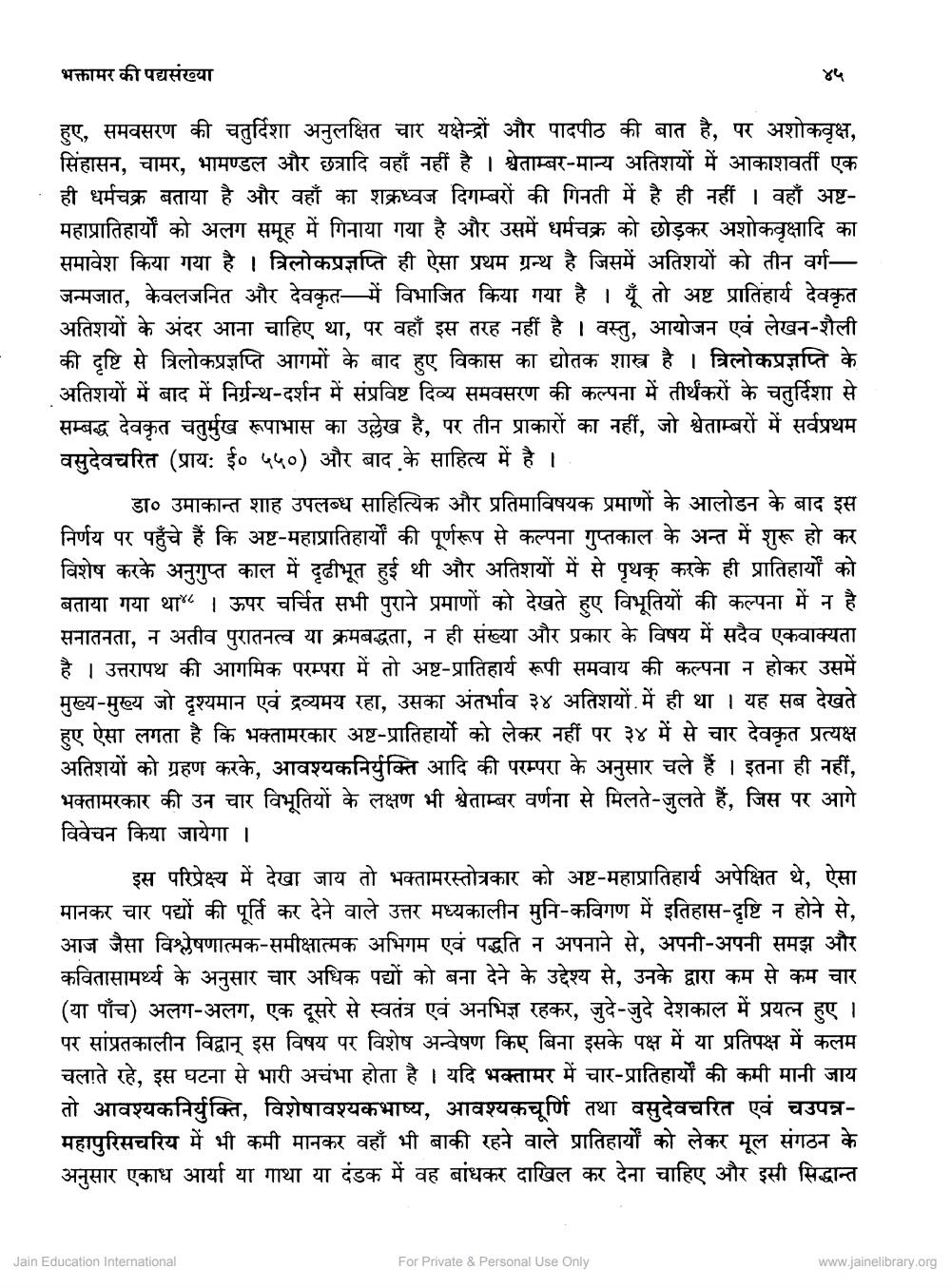________________
भक्तामर की पद्यसंख्या
४५
हुए, समवसरण की चतुर्दिशा अनुलक्षित चार यक्षेन्द्रों और पादपीठ की बात है, पर अशोकवृक्ष, सिंहासन, चामर, भामण्डल और छत्रादि वहाँ नहीं है । श्वेताम्बर-मान्य अतिशयों में आकाशवर्ती एक ही धर्मचक्र बताया है और वहाँ का शक्रध्वज दिगम्बरों की गिनती में है ही नहीं । वहाँ अष्टमहाप्रातिहार्यों को अलग समूह में गिनाया गया है और उसमें धर्मचक्र को छोड़कर अशोकवृक्षादि का समावेश किया गया है । त्रिलोकप्रज्ञप्ति ही ऐसा प्रथम ग्रन्थ है जिसमें अतिशयों को तीन वर्गजन्मजात, केवलजनित और देवकृत—में विभाजित किया गया है । यूँ तो अष्ट प्रातिहार्य देवकृत अतिशयों के अंदर आना चाहिए था, पर वहाँ इस तरह नहीं है । वस्तु, आयोजन एवं लेखन-शैली की दृष्टि से त्रिलोकप्रज्ञप्ति आगमों के बाद हुए विकास का द्योतक शास्त्र है । त्रिलोकप्रज्ञप्ति के अतिशयों में बाद में निर्ग्रन्थ-दर्शन में संप्रविष्ट दिव्य समवसरण की कल्पना में तीर्थंकरों के चतुर्दिशा से सम्बद्ध देवकृत चतुर्मुख रूपाभास का उल्लेख है, पर तीन प्राकारों का नहीं, जो श्वेताम्बरों में सर्वप्रथम वसुदेवचरित (प्राय: ई० ५५०) और बाद के साहित्य में है ।
___ डा० उमाकान्त शाह उपलब्ध साहित्यिक और प्रतिमाविषयक प्रमाणों के आलोडन के बाद इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि अष्ट-महाप्रातिहार्यों की पूर्णरूप से कल्पना गुप्तकाल के अन्त में शुरू हो कर विशेष करके अनुगुप्त काल में दृढीभूत हुई थी और अतिशयों में से पृथक् करके ही प्रातिहार्यों को बताया गया था । ऊपर चर्चित सभी पुराने प्रमाणों को देखते हुए विभूतियों की कल्पना में न है सनातनता, न अतीव पुरातनत्व या क्रमबद्धता, न ही संख्या और प्रकार के विषय में सदैव एकवाक्यता है । उत्तरापथ की आगमिक परम्परा में तो अष्ट-प्रातिहार्य रूपी समवाय की कल्पना न होकर उसमें मुख्य-मुख्य जो दृश्यमान एवं द्रव्यमय रहा, उसका अंतर्भाव ३४ अतिशयों में ही था । यह सब देखते हुए ऐसा लगता है कि भक्तामरकार अष्ट-प्रातिहार्यो को लेकर नहीं पर ३४ में से चार देवकृत प्रत्यक्ष अतिशयों को ग्रहण करके, आवश्यकनियुक्ति आदि की परम्परा के अनुसार चले हैं । इतना ही नहीं, भक्तामरकार की उन चार विभूतियों के लक्षण भी श्वेताम्बर वर्णना से मिलते-जुलते हैं, जिस पर आगे विवेचन किया जायेगा ।
इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो भक्तामरस्तोत्रकार को अष्ट-महाप्रातिहार्य अपेक्षित थे, ऐसा मानकर चार पद्यों की पूर्ति कर देने वाले उत्तर मध्यकालीन मुनि-कविगण में इतिहास-दृष्टि न होने से, आज जैसा विश्लेषणात्मक-समीक्षात्मक अभिगम एवं पद्धति न अपनाने से, अपनी-अपनी समझ और कवितासामर्थ्य के अनुसार चार अधिक पद्यों को बना देने के उद्देश्य से, उनके द्वारा कम से कम चार (या पाँच) अलग-अलग, एक दूसरे से स्वतंत्र एवं अनभिज्ञ रहकर, जुदे-जुदे देशकाल में प्रयत्न हुए । पर सांप्रतकालीन विद्वान् इस विषय पर विशेष अन्वेषण किए बिना इसके पक्ष में या प्रतिपक्ष में कलम चलाते रहे, इस घटना से भारी अचंभा होता है । यदि भक्तामर में चार-प्रातिहार्यों की कमी मानी जाय तो आवश्यकनियुक्ति, विशेषावश्यकभाष्य, आवश्यकचूर्णि तथा वसुदेवचरित एवं चउपन्नमहापुरिसचरिय में भी कमी मानकर वहाँ भी बाकी रहने वाले प्रातिहार्यों को लेकर मूल संगठन के अनुसार एकाध आर्या या गाथा या दंडक में वह बांधकर दाखिल कर देना चाहिए और इसी सिद्धान्त
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org