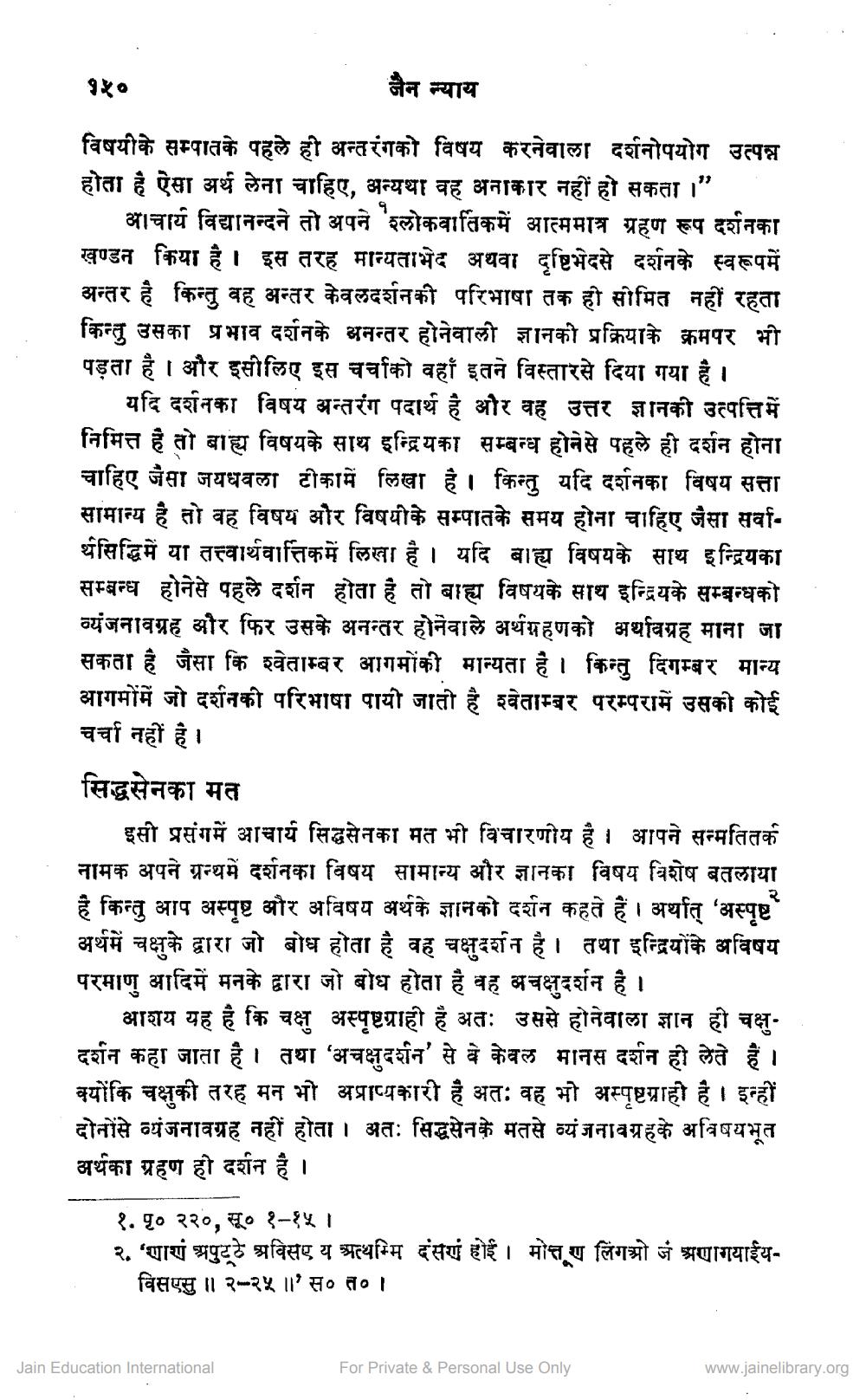________________
जैन न्याय
विषयीके सम्पातके पहले ही अन्तरंगको विषय करनेवाला दर्शनोपयोग उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए, अन्यथा वह अनाकार नहीं हो सकता।"
आचार्य विद्यानन्दने तो अपने 'श्लोकवार्तिकमें आत्ममात्र ग्रहण रूप दर्शनका खण्डन किया है। इस तरह मान्यताभेद अथवा दृष्टिभेदसे दर्शनके स्वरूपमें अन्तर है किन्तु वह अन्तर केवलदर्शनकी परिभाषा तक ही सीमित नहीं रहता किन्तु उसका प्रभाव दर्शनके अनन्तर होनेवाली ज्ञानकी प्रक्रियाके क्रमपर भी पड़ता है । और इसीलिए इस चर्चाको वहाँ इतने विस्तारसे दिया गया है।
यदि दर्शनका विषय अन्तरंग पदार्थ है और वह उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति में निमित्त है तो बाह्य विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होने से पहले ही दर्शन होना चाहिए जैसा जयधवला टीकामें लिखा है। किन्तु यदि दर्शनका विषय सत्ता सामान्य है तो वह विषय और विषयोके सम्पातके समय होना चाहिए जैसा सर्वार्थसिद्धि में या तत्त्वार्थवात्तिकमें लिखा है। यदि बाह्य विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे पहले दर्शन होता है तो बाह्य विषयके साथ इन्द्रियके सम्बन्धको व्यंजनावग्रह और फिर उसके अनन्तर होनेवाले अर्थग्रहणको अर्थावग्रह माना जा सकता है जैसा कि श्वेताम्बर आगमोंकी मान्यता है । किन्तु दिगम्बर मान्य आगमों में जो दर्शनकी परिभाषा पायी जाती है श्वेताम्बर परम्परामें उसकी कोई चर्चा नहीं है। सिद्धसेनका मत
इसी प्रसंगमें आचार्य सिद्धसेनका मत भी विचारणीय है। आपने सन्मतितर्क नामक अपने ग्रन्थमें दर्शनका विषय सामान्य और ज्ञानका विषय विशेष बतलाया है किन्तु आप अस्पृष्ट और अविषय अर्थके ज्ञानको दर्शन कहते हैं । अर्थात् 'अस्पृष्ट अर्थमें चक्षुके द्वारा जो बोध होता है वह चक्षुदर्शन है। तथा इन्द्रियोंके अविषय परमाणु आदिमें मनके द्वारा जो बोध होता है वह अचक्षुदर्शन है ।
आशय यह है कि चक्षु अस्पृष्टग्राही है अतः उससे होनेवाला ज्ञान ही चक्षु. दर्शन कहा जाता है। तथा 'अचक्षुदर्शन' से वे केवल मानस दर्शन ही लेते हैं। क्योंकि चक्षुकी तरह मन भी अप्राप्यकारी है अतः वह भो अस्पृष्टग्राही है । इन्हीं दोनोंसे व्यंजनावग्रह नहीं होता। अतः सिद्धसेनके मतसे व्यंजनावग्रहके अविषयभूत अर्थका ग्रहण हो दर्शन है ।
१. पृ० २२०, सू० १-१५ । २. 'णाणं अपुठे अविसए य अत्थम्मि दंसणं होई । मोत्त ण लिंगओ जं अणागयाईयविसएसु ॥ २-२५ ॥' स० त० ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org