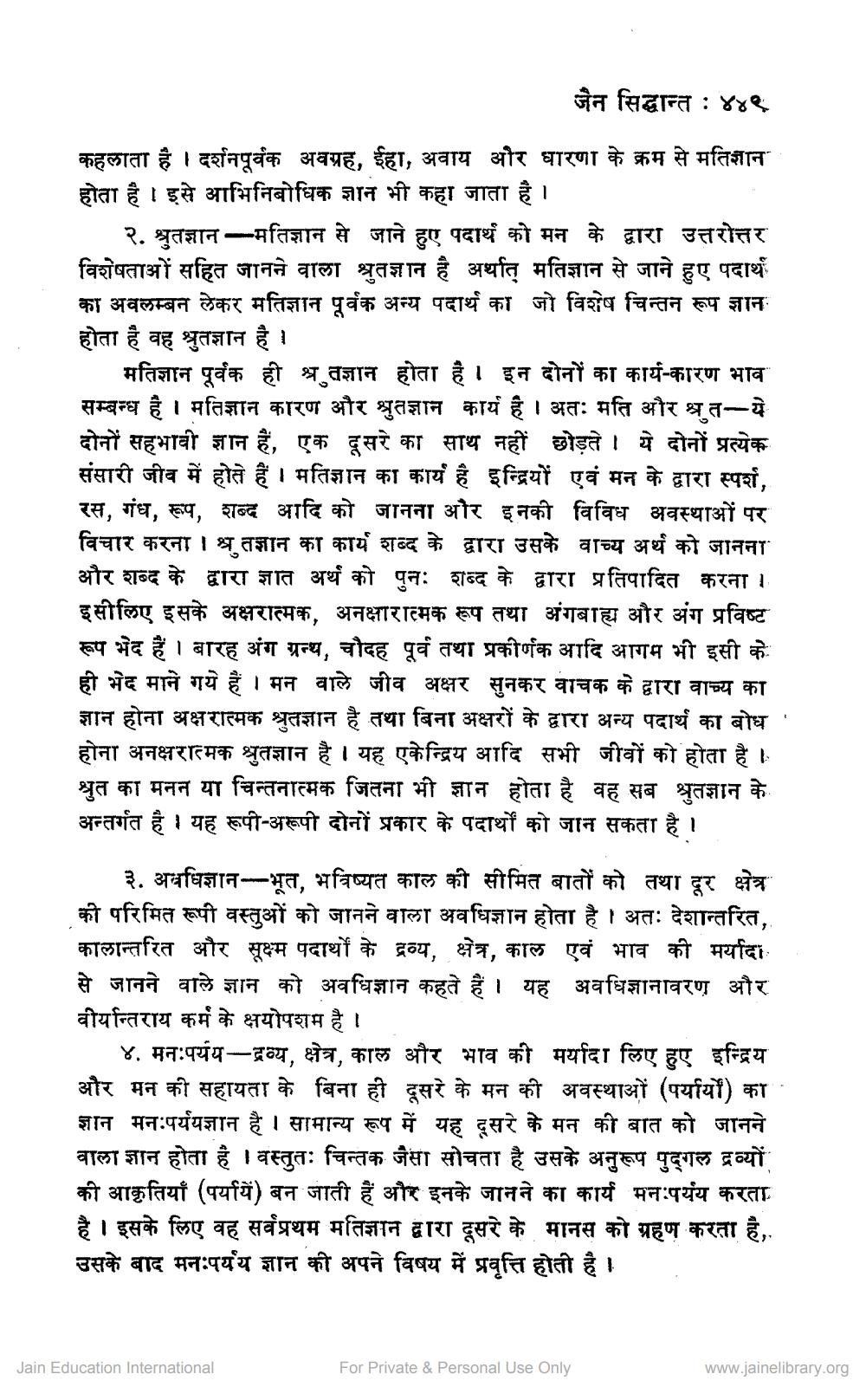________________
जैन सिद्धान्त : ४४९ कहलाता है । दर्शनपूर्वक अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के क्रम से मतिज्ञान होता है । इसे आभिनिबोधिक ज्ञान भी कहा जाता है।
२. श्रुतज्ञान-मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ को मन के द्वारा उत्तरोत्तर विशेषताओं सहित जानने वाला श्रुतज्ञान है अर्थात् मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलम्बन लेकर मतिज्ञान पूर्वक अन्य पदार्थ का जो विशेष चिन्तन रूप ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है।
मतिज्ञान पूर्वक ही श्र तज्ञान होता है। इन दोनों का कार्य-कारण भाव सम्बन्ध है । मतिज्ञान कारण और श्रुतज्ञान कार्य है । अतः मति और श्रुत-ये दोनों सहभावी ज्ञान हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते । ये दोनों प्रत्येक संसारी जीव में होते हैं । मतिज्ञान का कार्य है इन्द्रियों एवं मन के द्वारा स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द आदि को जानना और इनकी विविध अवस्थाओं पर विचार करना । श्रु तज्ञान का कार्य शब्द के द्वारा उसके वाच्य अर्थ को जानना
और शब्द के द्वारा ज्ञात अर्थ को पुनः शब्द के द्वारा प्रतिपादित करना । इसीलिए इसके अक्षरात्मक, अनक्षारात्मक रूप तथा अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट रूप भेद हैं । बारह अंग ग्रन्थ, चौदह पूर्व तथा प्रकीर्णक आदि आगम भी इसी के ही भेद माने गये हैं । मन वाले जीव अक्षर सुनकर वाचक के द्वारा वाच्य का ज्ञान होना अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है तथा बिना अक्षरों के द्वारा अन्य पदार्थ का बोध । होना अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । यह एकेन्द्रिय आदि सभी जीवों को होता है । श्रुत का मनन या चिन्तनात्मक जितना भी ज्ञान होता है वह सब श्रुतज्ञान के अन्तर्गत है । यह रूपी-अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जान सकता है।
३. अवधिज्ञान-भूत, भविष्यत काल की सीमित बातों को तथा दूर क्षेत्र की परिमित रूपी वस्तुओं को जानने वाला अवधिज्ञान होता है । अतः देशान्तरित, कालान्तरित और सूक्ष्म पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की मर्यादा से जानने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं। यह अवधिज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम है।
४. मनःपर्यय-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हए इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही दूसरे के मन की अवस्थाओं (पर्यायॊ) का ज्ञान मनःपर्ययज्ञान है । सामान्य रूप में यह दूसरे के मन की बात को जानने वाला ज्ञान होता है । वस्तुतः चिन्तक जैसा सोचता है उसके अनुरूप पुद्गल द्रव्यों की आकृतियाँ (पर्यायें) बन जाती हैं और इनके जानने का कार्य मनःपर्यय करता है। इसके लिए वह सर्वप्रथम मतिज्ञान द्वारा दूसरे के मानस को ग्रहण करता है, उसके बाद मनःपर्यय ज्ञान की अपने विषय में प्रवृत्ति होती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org