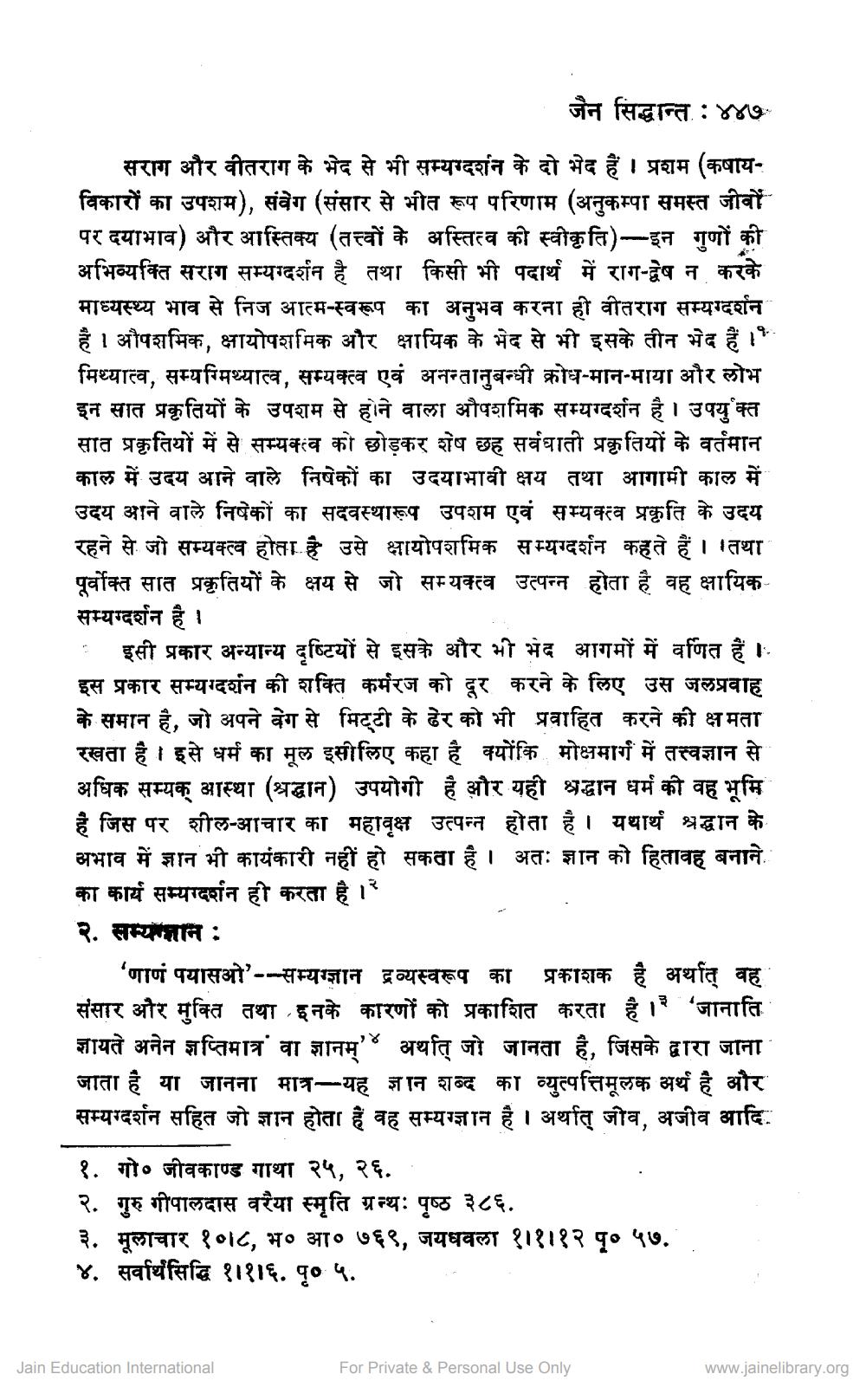________________
जैन सिद्धान्त : ४४७
सराग और वीतराग के भेद से भी सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं । प्रशम ( कषायविकारों का उपशम), संवेग (संसार से भीत रूप परिणाम (अनुकम्पा समस्त जीवों पर दयाभाव ) और आस्तिक्य (तत्त्वों के अस्तित्व की स्वीकृति ) ) - इन गुणों की अभिव्यक्ति सराग सम्यग्दर्शन है तथा किसी भी पदार्थ में राग-द्वेष न करके माध्यस्थ्य भाव से निज आत्म-स्वरूप का अनुभव करना ही वीतराग सम्यग्दर्शन है । औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक के भेद से भी इसके तीन भेद हैं । " मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व एवं अनन्तानुबन्धी क्रोध- मान-माया और लोभ इन सात प्रकृतियों के उपशम से होने वाला औपशमिक सम्यग्दर्शन है । उपर्युक्त सात प्रकृतियों में से सम्यक्त्व को छोड़कर शेष छह सर्वघाती प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय तथा आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्थारूप उपशम एवं सम्यक्त्व प्रकृति के उदय रहने से जो सम्यक्त्व होता है उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह क्षायिकसम्यग्दर्शन है ।
इसी प्रकार अन्यान्य दृष्टियों से इसके और भी भेद आगमों में वर्णित हैं | - इस प्रकार सम्यग्दर्शन की शक्ति कर्मरज को दूर करने के लिए उस जलप्रवाह के समान है, जो अपने वेग से मिट्टी के ढेर को भी प्रवाहित करने की क्षमता रखता है । इसे धर्म का मूल इसीलिए कहा है क्योंकि मोक्षमार्ग में तत्त्वज्ञान से अधिक सम्यक् आस्था ( श्रद्धान) उपयोगी है और यही श्रद्धान धर्म की वह भूमि है जिस पर शील- आचार का महावृक्ष उत्पन्न होता है । यथार्थ श्रद्धान के अभाव में ज्ञान भी कार्यकारी नहीं हो सकता है । अतः ज्ञान को हितावह बनाने का कार्य सम्यग्दर्शन ही करता है ।
२. सम्योज्ञान :
'णाणं पयासओ' -- सम्यग्ज्ञान द्रव्यस्वरूप का प्रकाशक है अर्थात् वह संसार और मुक्ति तथा इनके कारणों को प्रकाशित करता है । ३ 'जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्तिमात्र वा ज्ञानम् ४ अर्थात् जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र - यह ज्ञान शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है और सम्यग्दर्शन सहित जो ज्ञान होता हैं वह सम्यग्ज्ञान है । अर्थात् जीव, अजीव आदि.
१. गो० जीवकाण्ड गाथा २५, २६.
२. गुरु गोपालदास वरैया स्मृति ग्रन्थः पृष्ठ ३८६.
३. मूलाचार १०१८, भ० आ० ७६९, जयधवला १।१।१२ पू० ५७. ४. सर्वार्थसिद्धि १।११६. पृ० ५.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org