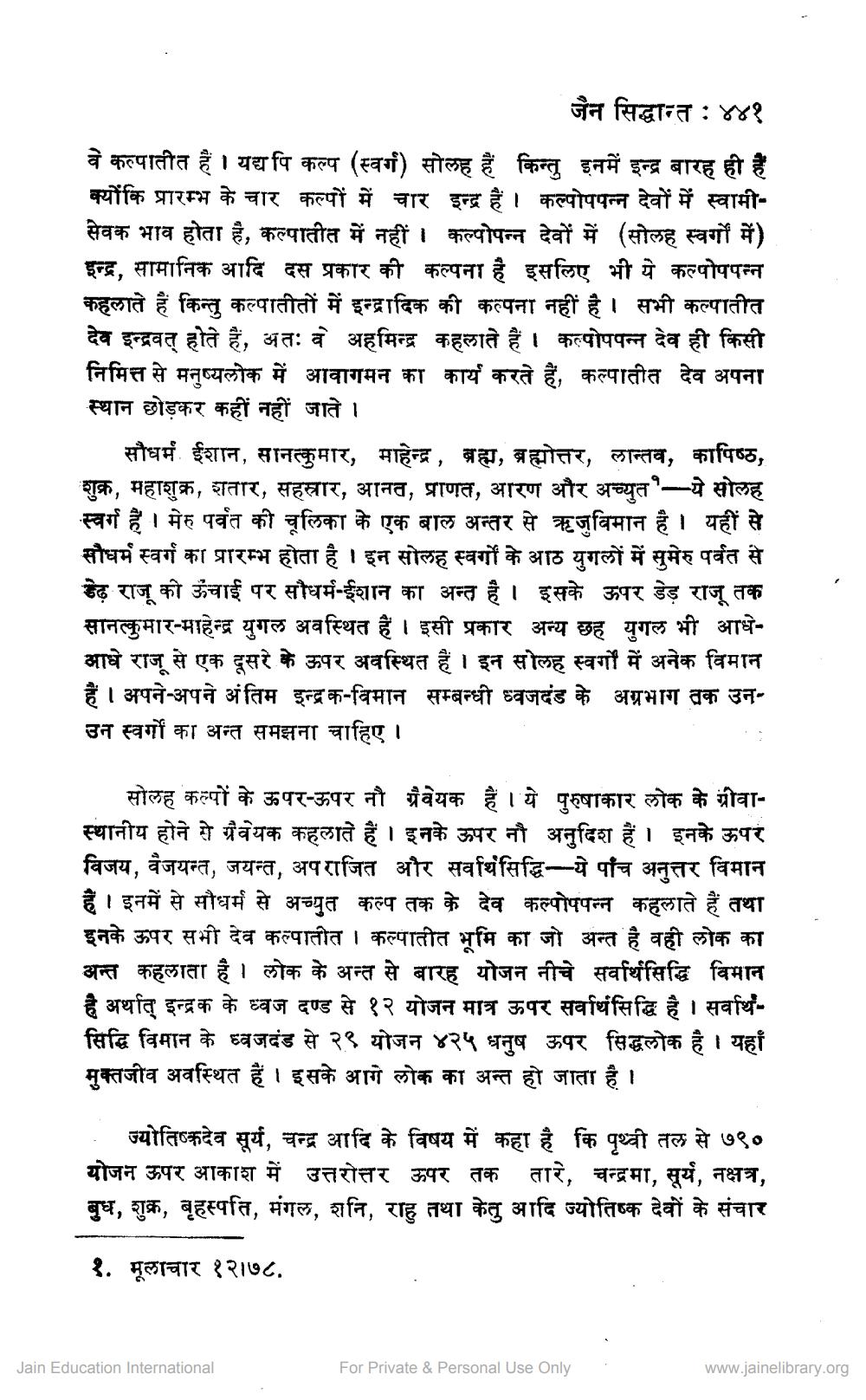________________
जैन सिद्धान्त : ४४१ वे कल्पातीत है । यद्यपि कल्प (स्वर्ग) सोलह हैं किन्तु इनमें इन्द्र बारह ही है क्योंकि प्रारम्भ के चार कल्पों में चार इन्द्र हैं। कल्पोपपन्न देवों में स्वामीसेवक भाव होता है, कल्पातीत में नहीं। कल्पोपन्न देवों में (सोलह स्वर्गों में) इन्द्र, सामानिक आदि दस प्रकार की कल्पना है इसलिए भी ये कल्पोपपन्न कहलाते हैं किन्तु कल्पातीतों में इन्द्रादिक की कल्पना नहीं है। सभी कल्पातीत देव इन्द्रवत् होते हैं, अतः वे अहमिन्द्र कहलाते हैं । कल्पोपपन्न देव ही किसी निमित्त से मनुष्यलोक में आवागमन का कार्य करते हैं, कल्पातीत देव अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते ।
सौधर्म ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र , ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत-ये सोलह स्वर्ग है । मेरु पर्वत की चूलिका के एक बाल अन्तर से ऋजुविमान है। यहीं से सौधर्म स्वर्ग का प्रारम्भ होता है । इन सोलह स्वर्गों के आठ युगलों में सुमेरु पर्वत से डेढ़ राजू को ऊंचाई पर सौधर्म-ईशान का अन्त है । इसके ऊपर डेड़ राजू तक सानत्कुमार-माहेन्द्र युगल अवस्थित हैं । इसी प्रकार अन्य छह युगल भी आधेआधे राजू से एक दूसरे के ऊपर अवस्थित हैं । इन सोलह स्वर्गों में अनेक विमान है । अपने-अपने अंतिम इन्द्र क-विमान सम्बन्धी ध्वजदंड के अग्रभाग तक उनउन स्वर्गों का अन्त समझना चाहिए ।
सोलह कल्पों के ऊपर-ऊपर नौ ग्रैवेयक हैं । ये पुरुषाकार लोक के ग्रीवास्थानीय होने से ग्रैवेयक कहलाते हैं । इनके ऊपर नौ अनुदिश हैं। इनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि-ये पांच अनुत्तर विमान है । इनमें से सौधर्म से अच्युत कल्प तक के देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं तथा इनके ऊपर सभी देव कल्पातीत । कल्पातीत भूमि का जो अन्त है वही लोक का अन्त कहलाता है। लोक के अन्त से बारह योजन नीचे सर्वार्थसिद्धि विमान है अर्थात् इन्द्रक के ध्वज दण्ड से १२ योजन मात्र ऊपर सर्वार्थसिद्धि है । सर्वार्थसिद्धि विमान के ध्वजदंड से २९ योजन ४२५ धनुष ऊपर सिद्धलोक है । यहाँ मुक्तजीव अवस्थित हैं । इसके आगे लोक का अन्त हो जाता है ।
ज्योतिष्कदेव सूर्य, चन्द्र आदि के विषय में कहा है कि पृथ्वी तल से ७९० योजन ऊपर आकाश में उत्तरोत्तर ऊपर तक तारे, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु तथा केतु आदि ज्योतिष्क देवों के संचार
१. मूलाचार १२।७८.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org