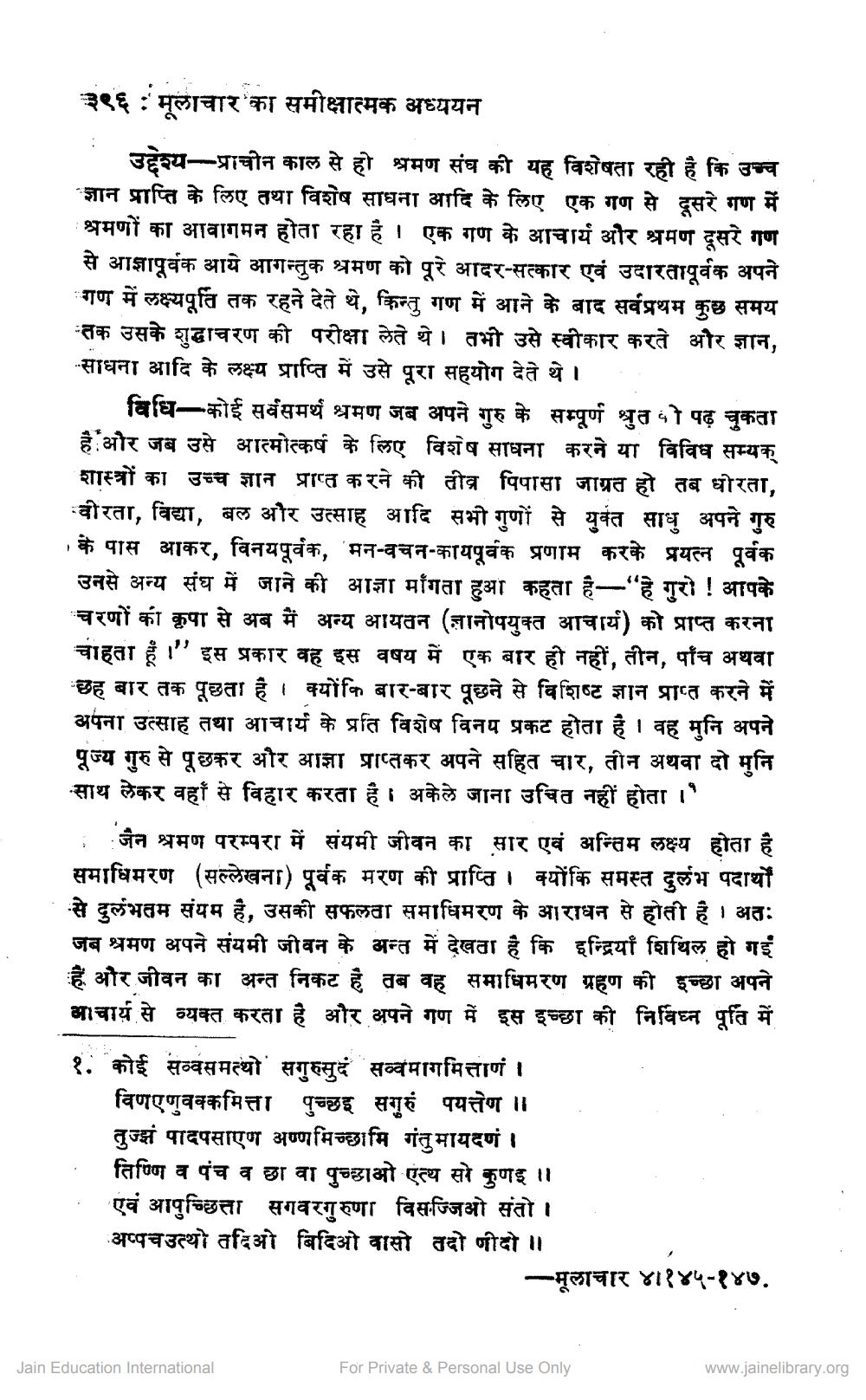________________
३९६ : मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन - उद्देश्य-प्राचीन काल से हो श्रमण संघ की यह विशेषता रही है कि उच्च ज्ञान प्राप्ति के लिए तथा विशेष साधना आदि के लिए एक गण से दूसरे गण में श्रमणों का आवागमन होता रहा है । एक गण के आचार्य और श्रमण दूसरे गण से आज्ञापूर्वक आये आगन्तुक श्रमण को पूरे आदर-सत्कार एवं उदारतापूर्वक अपने गण में लक्ष्यपूर्ति तक रहने देते थे, किन्तु गण में आने के बाद सर्वप्रथम कुछ समय -तक उसके शुद्धाचरण की परीक्षा लेते थे। तभी उसे स्वीकार करते और ज्ञान, “साधना आदि के लक्ष्य प्राप्ति में उसे पूरा सहयोग देते थे।
विधि-कोई सर्वसमर्थ श्रमण जब अपने गुरु के सम्पूर्ण श्रुत को पढ़ चुकता है और जब उसे आत्मोत्कर्ष के लिए विशेष साधना करने या विविध सम्यक् शास्त्रों का उच्च ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र पिपासा जाग्रत हो तब धोरता, वीरता, विद्या, बल और उत्साह आदि सभी गुणों से युक्त साधु अपने गुरु । के पास आकर, विनयपूर्वक, मन-वचन-कायपूर्वक प्रणाम करके प्रयत्न पूर्वक उनसे अन्य संघ में जाने की आज्ञा मांगता हुआ कहता है-“हे गुरो ! आपके चरणों की कृपा से अब मैं अन्य आयतन (ज्ञानोपयुक्त आचार्य) को प्राप्त करना चाहता हूँ।" इस प्रकार वह इस वषय में एक बार ही नहीं, तीन, पाँच अथवा छह बार तक पूछता है। क्योंकि बार-बार पूछने से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने में अपना उत्साह तथा आचार्य के प्रति विशेष विनय प्रकट होता है । वह मुनि अपने पूज्य गुरु से पूछकर और आज्ञा प्राप्तकर अपने सहित चार, तीन अथवा दो मुनि साथ लेकर वहाँ से विहार करता है। अकेले जाना उचित नहीं होता ।' . जैन श्रमण परम्परा में संयमी जीवन का सार एवं अन्तिम लक्ष्य होता है समाधिमरण (सल्लेखना) पूर्वक मरण की प्राप्ति। क्योंकि समस्त दुर्लभ पदार्थों से दुर्लभतम संयम है, उसकी सफलता समाधिमरण के आराधन से होती है । अतः जब श्रमण अपने संयमी जीवन के अन्त में देखता है कि इन्द्रियाँ शिथिल हो गई हैं और जीवन का अन्त निकट है तब वह समाधिमरण ग्रहण की इच्छा अपने आचार्य से व्यक्त करता है और अपने गण में इस इच्छा की निर्विघ्न पूर्ति में १. कोई सव्वसमत्थो सगुरुसुदं सव्वमागमित्ताणं ।
विणएणुवक्कमित्ता पुच्छइ सगुरुं पयत्तेण ॥ तुझं पादपसाएण अण्णमिच्छामि गंतु मायदणं । तिण्णि व पंच व छा वा पुच्छाओ एत्थ सो कुणइ ।। एवं आपुच्छित्ता सगवरगुरुणा विसज्जिओ संतो। अप्पच उत्थो तदिओ बिदिओ वासो तदो णीदो॥
-मूलाचार ४।१४५-१४७.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org