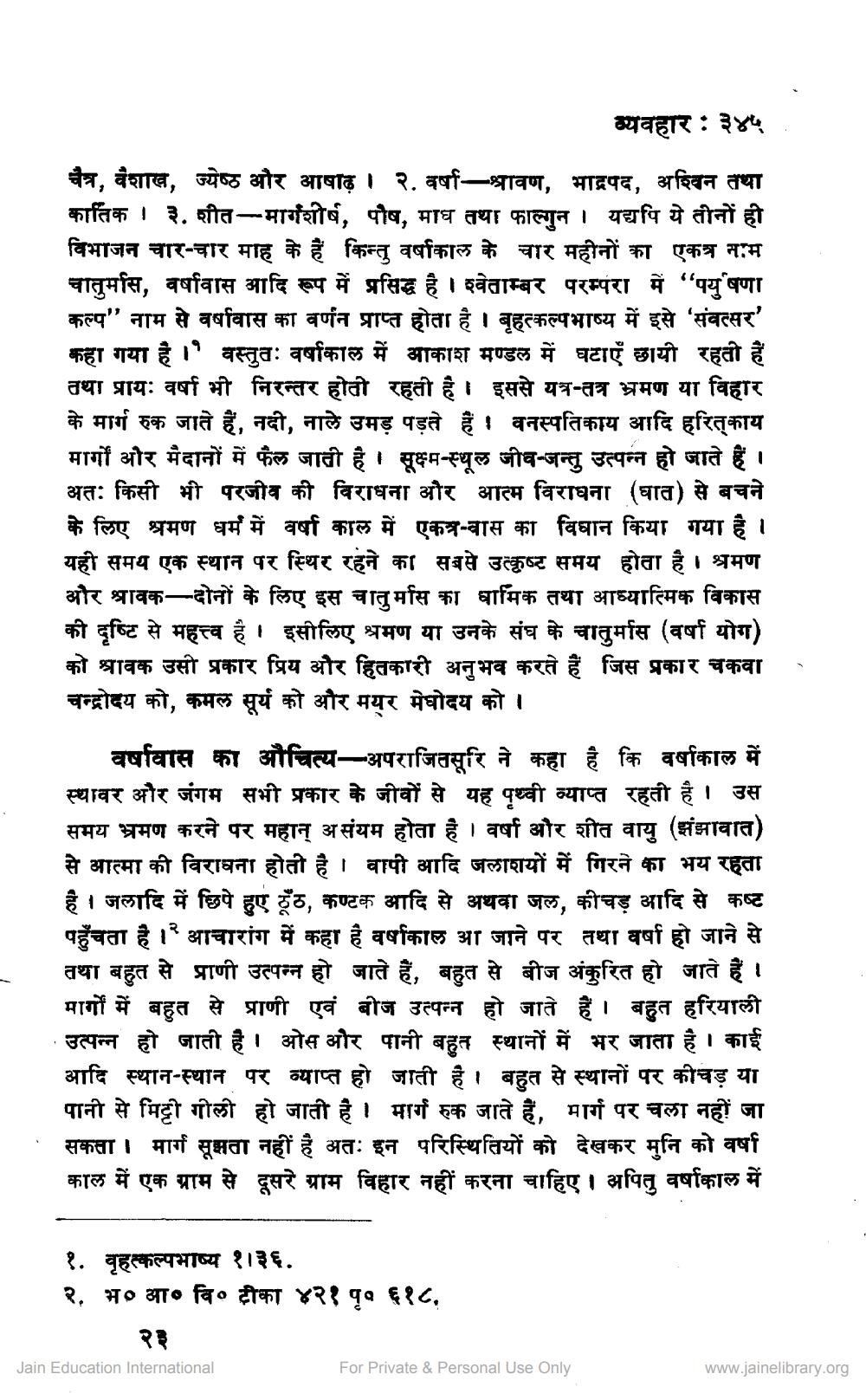________________
व्यवहार : ३४५
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ । २. वर्षा-श्रावण, भाद्रपद, अश्विन तथा कार्तिक । ३. शीत-मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन । यद्यपि ये तीनों ही विभाजन चार-चार माह के हैं किन्तु वर्षाकाल के चार महीनों का एकत्र नाम चातुर्मास, वर्षावास आदि रूप में प्रसिद्ध है । श्वेताम्बर परम्परा में “पयुषणा कल्प" नाम से वर्षावास का वर्णन प्राप्त होता है । बृहत्कल्पभाष्य में इसे 'संवत्सर' कहा गया है ।' वस्तुतः वर्षाकाल में आकाश मण्डल में घटाएं छायी रहती हैं तथा प्रायः वर्षा भी निरन्तर होती रहती है। इससे यत्र-तत्र भ्रमण या विहार के मार्ग रुक जाते हैं, नदी, नाले उमड़ पड़ते हैं। वनस्पतिकाय आदि हरित्काय मार्गों और मैदानों में फैल जाती है। सूक्ष्म-स्थूल जीव-जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं । अतः किसी भी परजीव की विराधना और आत्म विराधना (घात) से बचने के लिए श्रमण धर्म में वर्षा काल में एकत्र-वास का विधान किया गया है। यही समय एक स्थान पर स्थिर रहने का सबसे उत्कृष्ट समय होता है । श्रमण
और श्रावक-दोनों के लिए इस चातुर्मास का धार्मिक तथा आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से महत्त्व है। इसीलिए श्रमण या उनके संघ के चातुर्मास (वर्षा योग) को श्रावक उसी प्रकार प्रिय और हितकारी अनुभव करते हैं जिस प्रकार चकवा. चन्द्रोदय को, कमल सूर्य को और मयर मेघोदय को ।
वर्षावास का औचित्य-अपराजितसूरि ने कहा है कि वर्षाकाल में स्थावर और जंगम सभी प्रकार के जीवों से यह पृथ्वी व्याप्त रहती है। उस समय भ्रमण करने पर महान् असंयम होता है । वर्षा और शीत वायु (झंझावात) से आत्मा की विराधना होती है। वापी आदि जलाशयों में गिरने का भय रहता है। जलादि में छिपे हुए हूँठ, कण्टक आदि से अथवा जल, कीचड़ आदि से कष्ट पहुँचता है। आचारांग में कहा है वर्षाकाल आ जाने पर तथा वर्षा हो जाने से तथा बहुत से प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत से बीज अंकुरित हो जाते हैं । मार्गों में बहुत से प्राणी एवं बीज उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत हरियाली . उत्पन्न हो जाती है। ओस और पानी बहुत स्थानों में भर जाता है । काई
आदि स्थान-स्थान पर व्याप्त हो जाती है। बहुत से स्थानों पर कीचड़ या पानी से मिट्टी गीली हो जाती है। मार्ग रुक जाते हैं, मार्ग पर चला नहीं जा सकता। मार्ग सूझता नहीं है अतः इन परिस्थितियों को देखकर मुनि को वर्षा काल में एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार नहीं करना चाहिए। अपितु वर्षाकाल में
१. वृहत्कल्पभाष्य १।३६. २. भ० आ० वि० टीका ४२१ पृ० ६१८.
२३ Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org