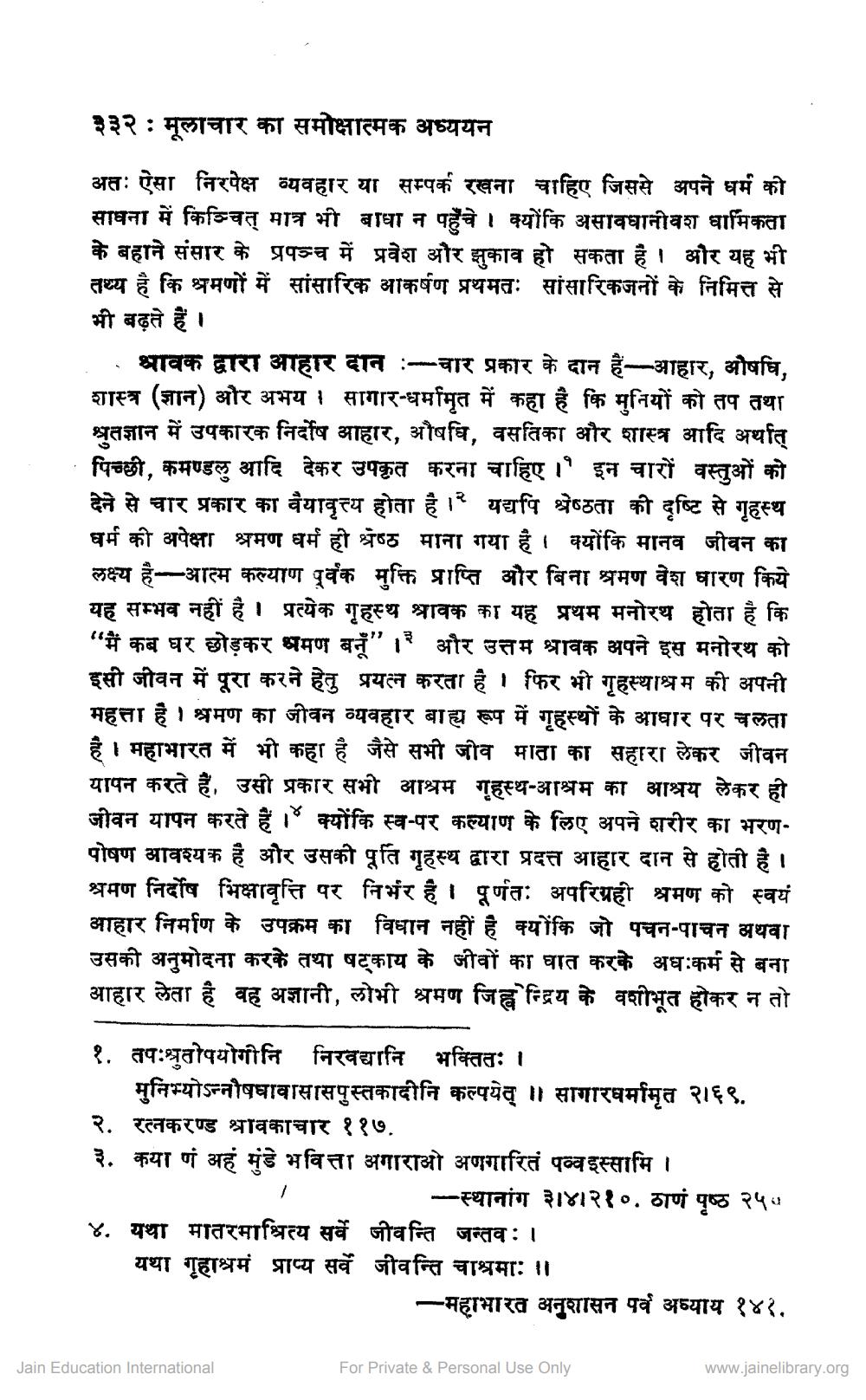________________
३३२ : मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन
अतः ऐसा निरपेक्ष व्यवहार या सम्पर्क रखना चाहिए जिससे अपने धर्म की साधना में किञ्चित् मात्र भी बाधा न पहुँचे । क्योंकि असावधानीवश धार्मिकता के बहाने संसार के प्रपञ्च में प्रवेश और झुकाव हो सकता है । और यह भी तथ्य है कि श्रमणों में सांसारिक आकर्षण प्रथमतः सांसारिकजनों के निमित्त से भी बढ़ते हैं ।
श्रावक द्वारा आहार दान :-चार प्रकार के दान हैं—आहार, औषधि, शास्त्र (ज्ञान) और अभय । सागारधर्मामृत में कहा है कि मुनियों को तप तथा श्रुतज्ञान में उपकारक निर्दोष आहार, औषधि, वसतिका और शास्त्र आदि अर्थात् पिच्छी, कमण्डलु आदि देकर उपकृत करना चाहिए ।' इन चारों वस्तुओं को देने से चार प्रकार का वैयावृत्त्य होता है । यद्यपि श्रेष्ठता की दृष्टि से गृहस्थ धर्म की अपेक्षा श्रमण धर्म ही श्रेष्ठ माना गया है । क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है-- आत्म कल्याण पूर्वक मुक्ति प्राप्ति और बिना श्रमण वेश धारण किये यह सम्भव नहीं है । प्रत्येक गृहस्थ श्रावक का यह प्रथम मनोरथ होता है कि "मैं कब घर छोड़कर भ्रमण बनूँ" । और उत्तम श्रावक अपने इस मनोरथ को इसी जीवन में पूरा करने हेतु प्रयत्न करता है । फिर भी गृहस्थाश्रम की अपनी महत्ता है | श्रमण का जीवन व्यवहार बाह्य रूप में गृहस्थों के आधार पर चलता है । महाभारत में भी कहा है जैसे सभी जीव माता का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते हैं। क्योंकि स्व-पर कल्याण के लिए अपने शरीर का भरणपोषण आवश्यक है और उसकी पूर्ति गृहस्थ द्वारा प्रदत्त आहार दान से होती है ।
श्रमण को स्वयं पचन- पाचन अथवा
श्रमण निर्दोष भिक्षावृत्ति पर निर्भर है । पूर्णतः अपरिग्रही आहार निर्माण के उपक्रम का विधान नहीं है क्योंकि जो उसकी अनुमोदना करके तथा षट्काय के जीवों का घात करके आहार लेता है वह अज्ञानी, लोभी श्रमण जिह्व ेन्द्रिय के
अधः कर्म से बना वशीभूत होकर न तो
१. तपः श्रुतोपयोगीनि निरवद्यानि भक्तितः ।
मुनिभ्योऽन्नोषघावासासपुस्तकादीनि कल्पयेत् ॥ सागारधर्मामृत २।६९.
२. रत्नकरण्ड श्रावकाचार ११७.
३. कया णं अहं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारितं पव्वइस्सामि ।
४. यथा मातरमाश्रित्य सर्वे यथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्वे
Jain Education International
- स्थानांग ३|४| २१०. ठाणं पृष्ठ २५०
जीवन्ति जन्तव: । जीवन्ति चाश्रमाः ॥
- महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय १४१.
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org