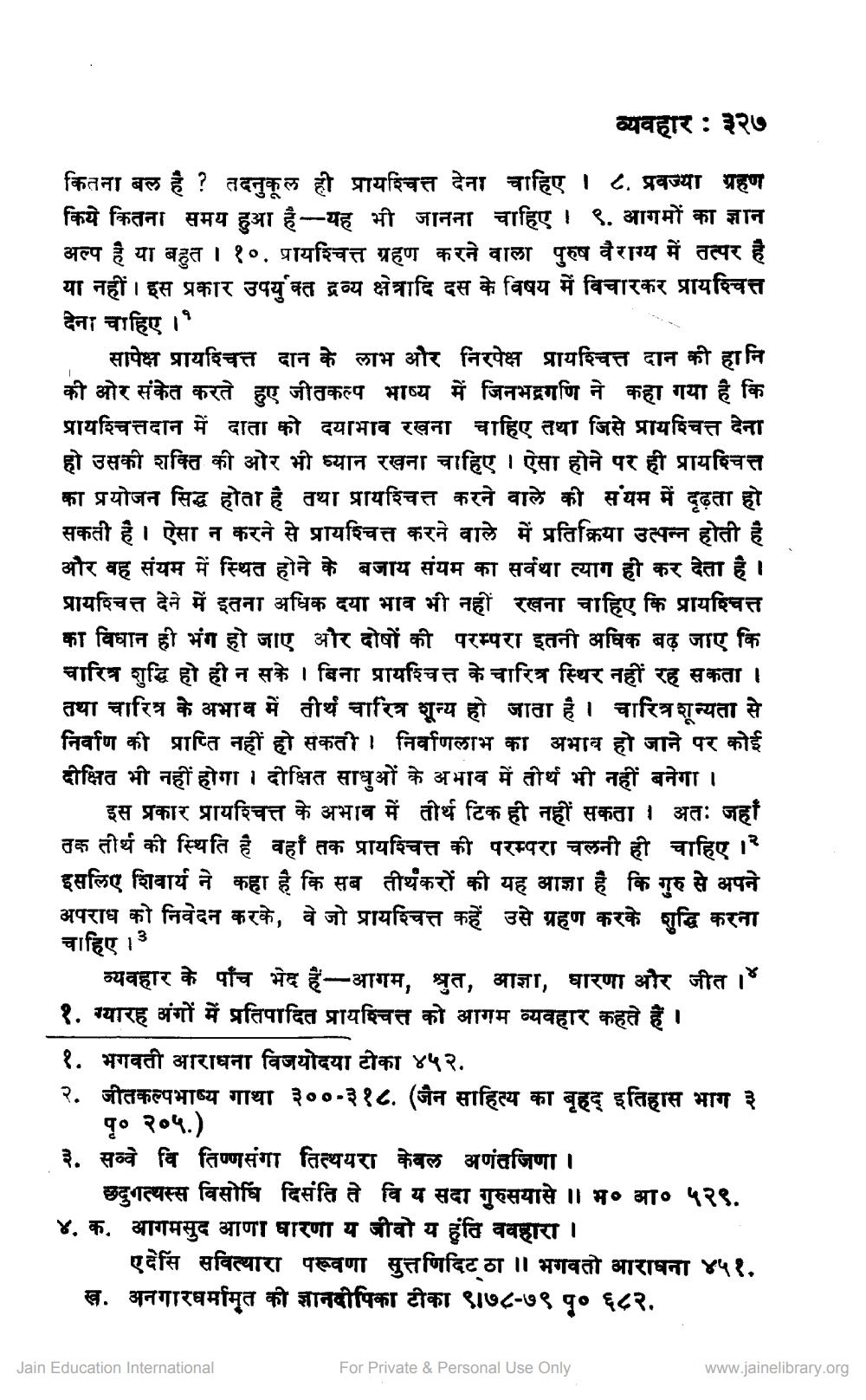________________
व्यवहार : ३२७
कितना बल है ? तदनुकूल ही प्रायश्चित्त देना चाहिए । ८. प्रवज्या ग्रहण किये कितना समय हुआ है-यह भी जानना चाहिए । ९. आगमों का ज्ञान अल्प है या बहुत । १०. प्रायश्चित्त ग्रहण करने वाला पुरुष वैराग्य में तत्पर है या नहीं। इस प्रकार उपयुक्त द्रव्य क्षेत्रादि दस के विषय में विचारकर प्रायश्चित्त देना चाहिए।' . सापेक्ष प्रायश्चित्त दान के लाभ और निरपेक्ष प्रायश्चित्त दान की हानि की ओर संकेत करते हुए जीतकल्प भाष्य में जिनभद्रगणि ने कहा गया है कि प्रायश्चित्तदान में दाता को दयाभाव रखना चाहिए तथा जिसे प्रायश्चित्त देना हो उसकी शक्ति की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा होने पर ही प्रायश्चित्त का प्रयोजन सिद्ध होता है तथा प्रायश्चित्त करने वाले की संयम में दृढ़ता हो सकती है। ऐसा न करने से प्रायश्चित्त करने वाले में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह संयम में स्थित होने के बजाय संयम का सर्वथा त्याग ही कर देता है । प्रायश्चित्त देने में इतना अधिक दया भाव भी नहीं रखना चाहिए कि प्रायश्चित्त का विधान ही भंग हो जाए और दोषों की परम्परा इतनी अधिक बढ़ जाए कि चारित्र शुद्धि हो ही न सके । बिना प्रायश्चित्त के चारित्र स्थिर नहीं रह सकता । तथा चारित्र के अभाव में तीर्थ चारित्र शून्य हो जाता है । चारित्र शून्यता से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। निर्वाणलाभ का अभाव हो जाने पर कोई दीक्षित भी नहीं होगा । दीक्षित साधुओं के अभाव में तीर्थ भी नहीं बनेगा।
इस प्रकार प्रायश्चित्त के अभाव में तीर्थ टिक ही नहीं सकता। अतः जहाँ तक तीर्थ की स्थिति है वहाँ तक प्रायश्चित्त की परम्परा चलनी ही चाहिए । इसलिए शिवार्य ने कहा है कि सब तीर्थंकरों की यह आज्ञा है कि गुरु से अपने अपराध को निवेदन करके, वे जो प्रायश्चित्त कहें उसे ग्रहण करके शुद्धि करना चाहिए।
व्यवहार के पाँच भेद है-आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत ।। १. ग्यारह अंगों में प्रतिपादित प्रायश्चित्त को आगम व्यवहार कहते हैं । १. भगवती आराधना विजयोदया टोका ४५२. २. जीतकल्पभाष्य गाथा ३००.३१८. (जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग ३
पृ० २०५.) ३. सव्वे वि तिण्णसंगा तित्थयरा केवल अणंतजिणा।
छदुगत्यस्स विसोषिं दिसंति ते वि य सदा गुरुसयासे ॥ भ. आ० ५२९. ४. क. आगमसुद आणा धारणा य जीवो य हुंति ववहारा ।
एदेसि सवित्थारा पख्वणा सुत्तणिदिटठा ॥ भगवतो आराधना ४५१. __ स्व. अनगारधर्मामृत की ज्ञानदीपिका टीका ९७८-७९ पृ० ६८२.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org