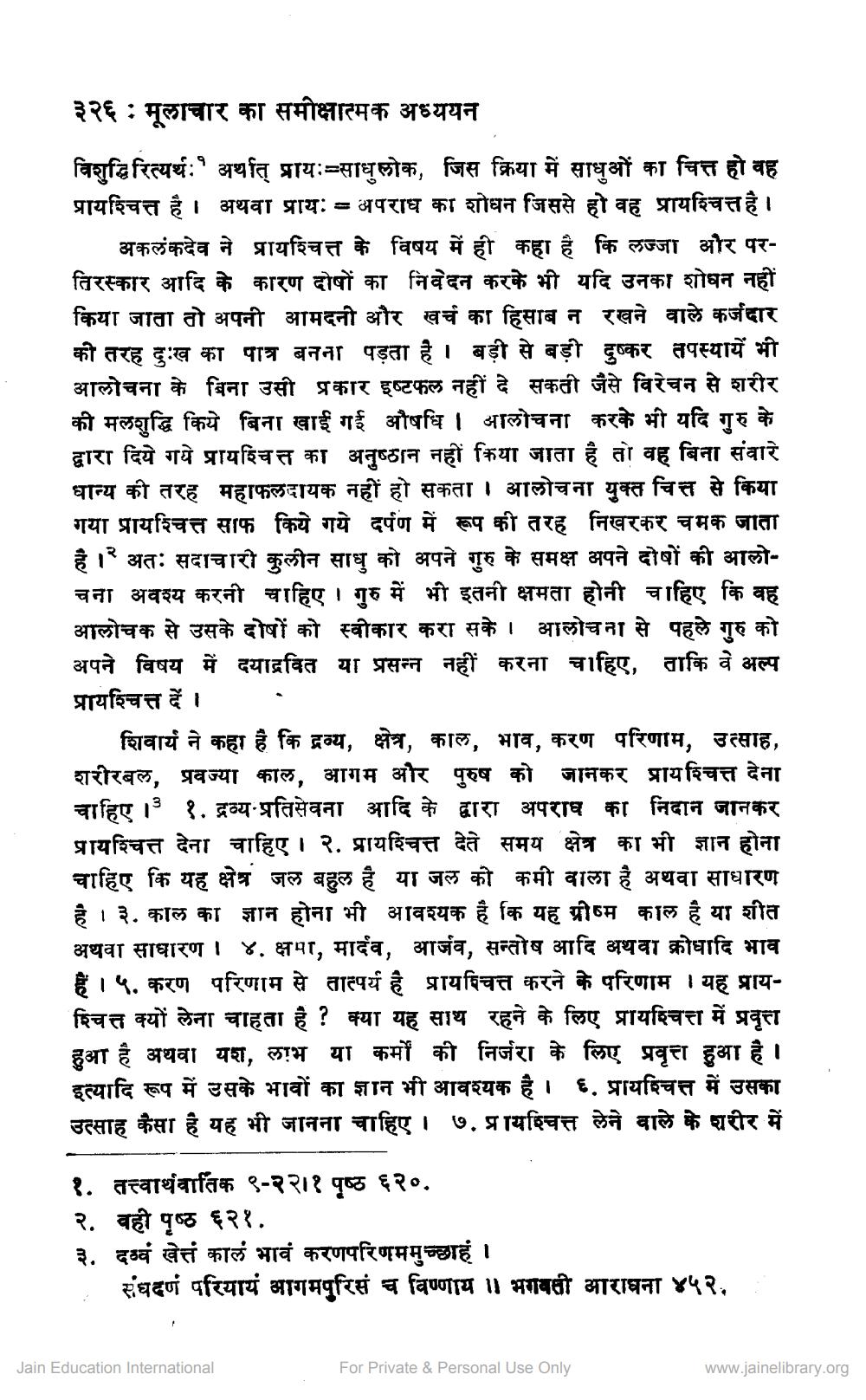________________
३२६ : मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन विशुद्धिरित्यर्थः' अर्थात् प्रायः साधुलोक, जिस क्रिया में साधुओं का चित्त हो वह प्रायश्चित्त है। अथवा प्रायः = अपराध का शोधन जिससे हो वह प्रायश्चित्त है।
अकलंकदेव ने प्रायश्चित्त के विषय में ही कहा है कि लज्जा और परतिरस्कार आदि के कारण दोषों का निवेदन करके भी यदि उनका शोधन नहीं किया जाता तो अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब न रखने वाले कर्जदार की तरह दुःख का पात्र बनना पड़ता है। बड़ी से बड़ी दुष्कर तपस्यायें भी आलोचना के बिना उसी प्रकार इष्टफल नहीं दे सकती जैसे विरेचन से शरीर की मलशुद्धि किये बिना खाई गई औषधि | आलोचना करके भी यदि गुरु के द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का अनुष्ठान नहीं किया जाता है तो वह बिना संवारे धान्य की तरह महाफलदायक नहीं हो सकता। आलोचना युक्त चित्त से किया गया प्रायश्चित्त साफ किये गये दर्पण में रूप की तरह निखरकर चमक जाता है। अतः सदाचारी कुलीन साधु को अपने गुरु के समक्ष अपने दोषों की आलोचना अवश्य करनी चाहिए । गुरु में भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह आलोचक से उसके दोषों को स्वीकार करा सके । आलोचना से पहले गुरु को अपने विषय में दयाद्रवित या प्रसन्न नहीं करना चाहिए, ताकि वे अल्प प्रायश्चित्त दें।
शिवार्य ने कहा है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, करण परिणाम, उत्साह, शरीरबल, प्रवज्या काल, आगम और पुरुष को जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए। १. द्रव्य प्रतिसेवना आदि के द्वारा अपराध का निदान जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । २. प्रायश्चित्त देते समय क्षेत्र का भी ज्ञान होना चाहिए कि यह क्षेत्र जल बहुल है या जल को कमी वाला है अथवा साधारण है । ३. काल का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि यह ग्रीष्म काल है या शीत अथवा साधारण । ४. क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष आदि अथवा क्रोधादि भाव है । ५. करण परिणाम से तात्पर्य है प्रायश्चित्त करने के परिणाम । यह प्रायश्चित्त क्यों लेना चाहता है ? क्या यह साथ रहने के लिए प्रायश्चित्त में प्रवृत्त हुआ है अथवा यश, लाभ या कर्मों की निर्जरा के लिए प्रवृत्त हुआ है । इत्यादि रूप में उसके भावों का ज्ञान भी आवश्यक है। ६. प्रायश्चित्त में उसका उत्साह कैसा है यह भी जानना चाहिए। ७. प्रायश्चित्त लेने वाले के शरीर में
१. तत्त्वार्थवार्तिक ९-२२।१ पृष्ठ ६२०. २. वही पृष्ठ ६२१. ३. दव्वं खेत्तं कालं भावं करणपरिणममुच्छाहं ।
संघदणं परियायं आगमपुरिसं च विण्णाय ॥ भगवती आराधना ४५२.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org