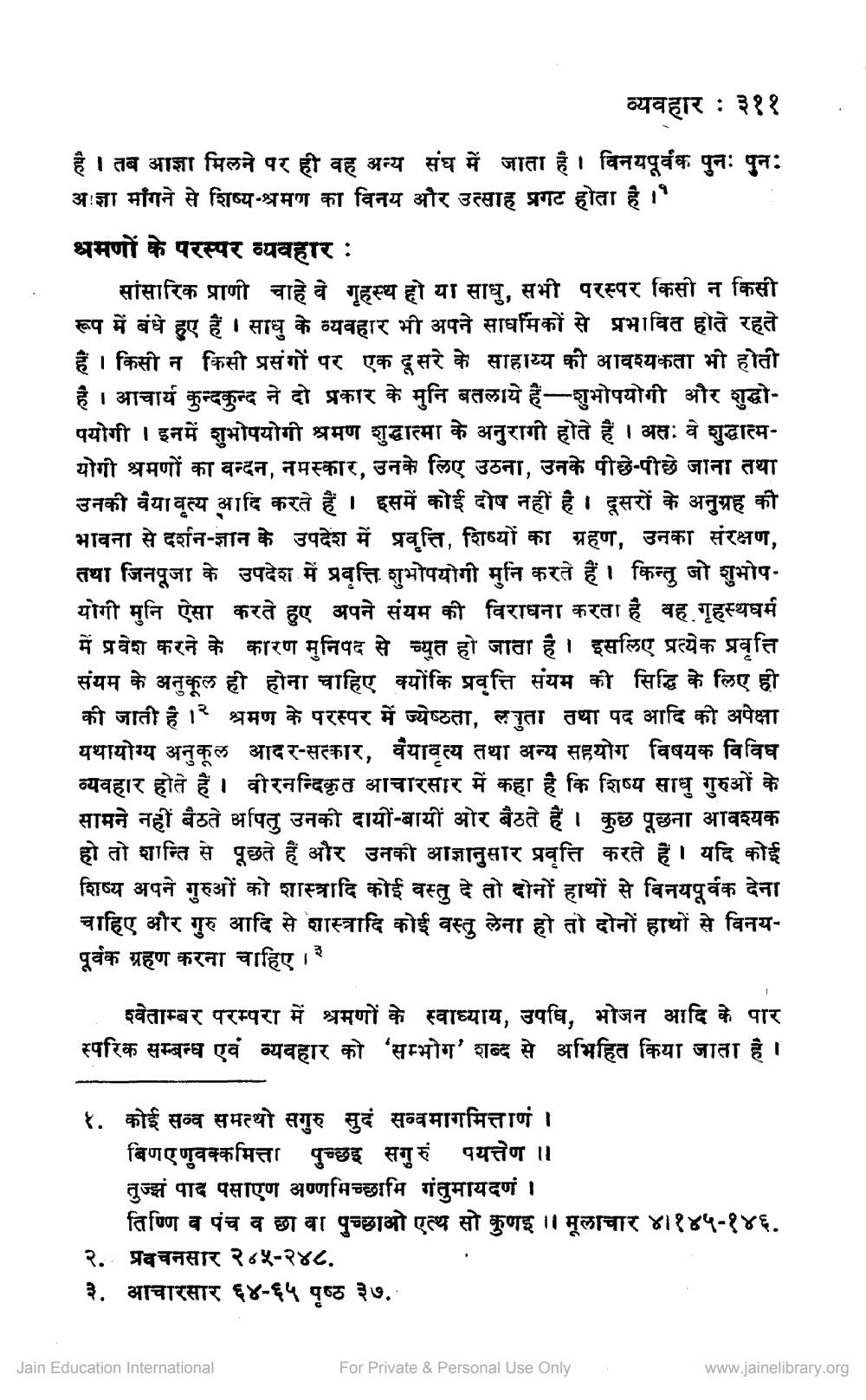________________
व्यवहार : ३११ है । तब आज्ञा मिलने पर ही वह अन्य संघ में जाता है। विनयपूर्वक पुनः पुनः आज्ञा मांगने से शिष्य श्रमण का विनय और उत्साह प्रगट होता है।' श्रमणों के परस्पर व्यवहार :
सांसारिक प्राणी चाहे वे गृहस्थ हो या साधु, सभी परस्पर किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं । साधु के व्यवहार भी अपने सार्मिकों से प्रभावित होते रहते हैं । किसी न किसी प्रसंगों पर एक दूसरे के साहाय्य की आवश्यकता भी होती है । आचार्य कुन्दकुन्द ने दो प्रकार के मुनि बतलाये हैं-शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । इनमें शुभोपयोगी श्रमण शुद्धात्मा के अनुरागी होते हैं । अतः वे शुद्धात्मयोगी श्रमणों का वन्दन, नमस्कार, उनके लिए उठना, उनके पीछे-पीछे जाना तथा उनकी वैया वृत्य आदि करते हैं । इसमें कोई दोष नहीं है । दूसरों के अनुग्रह की भावना से दर्शन-ज्ञान के उपदेश में प्रवृत्ति, शिष्यों का ग्रहण, उनका संरक्षण, तथा जिनपूजा के उपदेश में प्रवत्ति शुभोपयोगी मुनि करते हैं। किन्तु जो शुभोप. योगी मुनि ऐसा करते हुए अपने संयम की विराधना करता है वह गृहस्थधर्म में प्रवेश करने के कारण मुनिपद से च्युत हो जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रवृत्ति संयम के अनुकूल ही होना चाहिए क्योंकि प्रवृत्ति संयम की सिद्धि के लिए ही की जाती है ।२ श्रमण के परस्पर में ज्येष्ठता, लता तथा पद आदि की अपेक्षा यथायोग्य अनुकूल आदर-सत्कार, वैयावृत्य तथा अन्य सहयोग विषयक विविध व्यवहार होते हैं। वीरनन्दिकृत आचारसार में कहा है कि शिष्य साधु गुरुओं के सामने नहीं बैठते अपितु उनकी दायों-बायीं ओर बैठते हैं। कुछ पूछना आवश्यक हो तो शान्ति से पूछते हैं और उनकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करते हैं। यदि कोई शिष्य अपने गुरुओं को शास्त्रादि कोई वस्तु दे तो दोनों हाथों से विनयपूर्वक देना चाहिए और गुरु आदि से शास्त्रादि कोई वस्तु लेना हो तो दोनों हाथों से विनयपूर्वक ग्रहण करना चाहिए । ३
श्वेताम्बर परम्परा में श्रमणों के स्वाध्याय, उपघि, भोजन आदि के पार स्परिक सम्बन्ध एवं व्यवहार को 'सम्भोग' शब्द से अभिहित किया जाता है ।
१. कोई सव्व समत्थो सगुरु सुदं सन्वमागमित्ताणं ।
बिणएणुवक्कमित्ता पुच्छइ सगुरुं पयत्तेण ।। तुझं पाद पसाएण अण्णमिच्छामि गंतुमायदणं ।
तिणि व पंच व छा वा पुच्छाओ एत्थ सो कुणइ ।। मूलाचार ४।१४५-१४६. २. प्रवचनसार २४५-२४८. ३. आचारसार ६४-६५ पृष्ठ ३७.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org