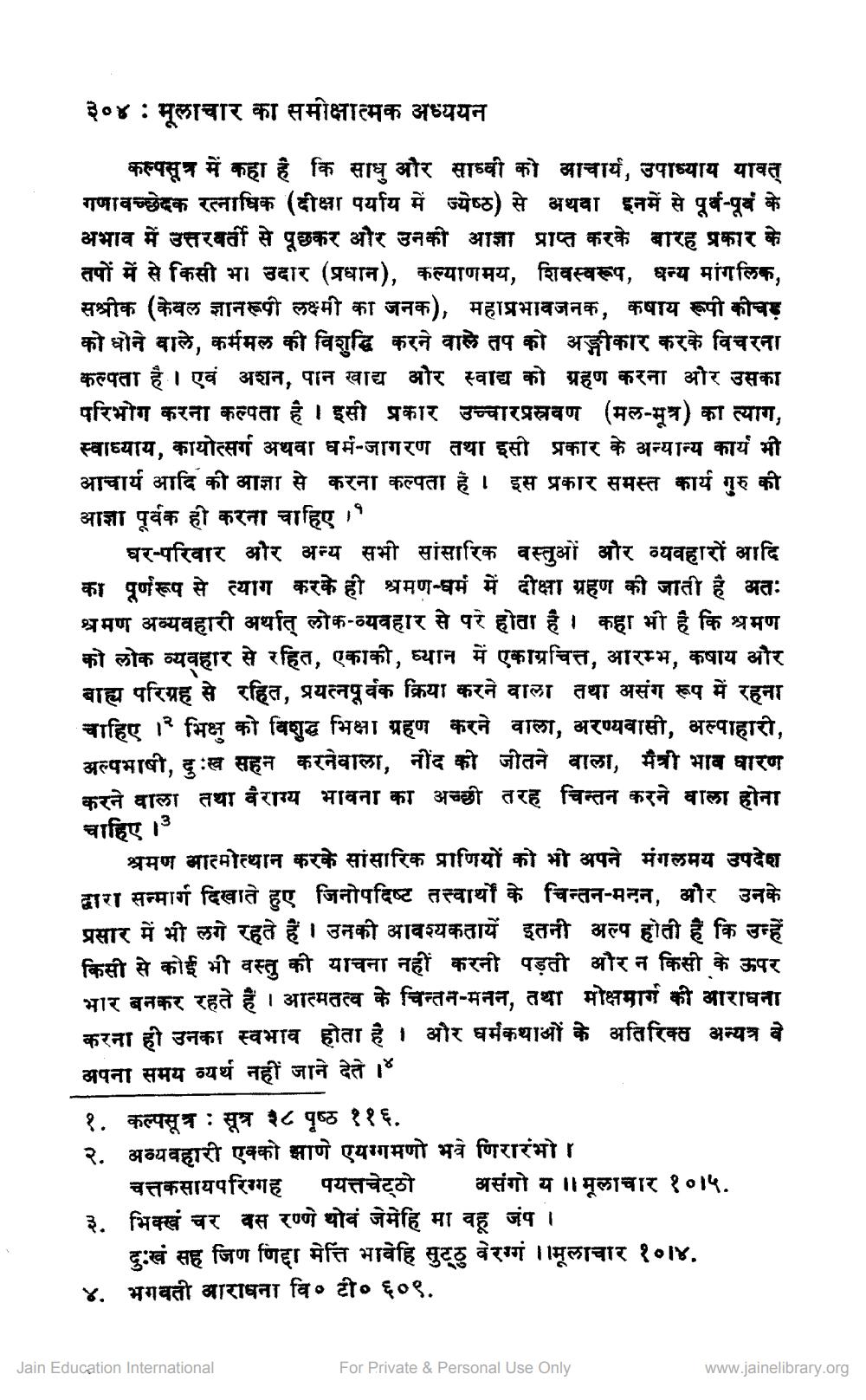________________
३०४ : मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन
कल्पसूत्र में कहा है कि साधु और आचार्य, उपाध्याय यावत् गणावच्छेदक रत्नाधिक (दीक्षा पर्याय में अथवा इनमें से पूर्व-पूर्व के अभाव में उत्तरवर्ती से पूछकर और उनकी आज्ञा प्राप्त करके बारह प्रकार के तपों में से किसी भा उदार (प्रधान), कल्याणमय, शिवस्वरूप, धन्य मांगलिक, सीक (केवल ज्ञानरूपी लक्ष्मी का जनक ), महाप्रभावजनक, कषाय रूपी कीचड़ को धोने वाले, कर्ममल की विशुद्धि करने वाले तप को अङ्गीकार करके विचरना कल्पता है । एवं अशन, पान खाद्य और स्वाद्य को ग्रहण करना और उसका परिभोग करना कल्पता है । इसी प्रकार उच्चारप्रस्रवण ( मल-मूत्र) का त्याग, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग अथवा धर्म-जागरण तथा इसी प्रकार के अन्यान्य कार्य भी आचार्य आदि की आज्ञा से करना कल्पता है । इस प्रकार समस्त कार्य गुरु की आज्ञा पूर्वक ही करना चाहिए ।"
साध्वी को ज्येष्ठ) से
घर-परिवार और अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं और व्यवहारों आदि का पूर्णरूप से त्याग करके ही श्रमण-धर्म में दीक्षा ग्रहण की जाती है अतः श्रमण अव्यवहारी अर्थात् लोक व्यवहार से परे होता है । कहा भी है कि श्रमण को लोक व्यवहार से रहित, एकाकी, ध्यान में एकाग्रचित्त, आरम्भ, कषाय और बाह्य परिग्रह से रहित, प्रयत्नपूर्वक क्रिया करने वाला तथा असंग रूप में रहना चाहिए । भिक्षु को विशुद्ध भिक्षा ग्रहण करने वाला, अरण्यवासी, अल्पाहारी, अल्पभाषी, दुःख सहन करनेवाला, नींद की जीतने वाला, मैत्री भाव धारण करने वाला तथा वैराग्य भावना का अच्छी तरह चिन्तन करने वाला होना चाहिए |
श्रमण आत्मोत्थान करके सांसारिक प्राणियों को भी अपने मंगलमय उपदेश द्वारा सन्मार्ग दिखाते हुए जिनोपदिष्ट तत्वार्थों के चिन्तन-मनन और उनके प्रसार में भी लगे रहते हैं । उनकी आवश्यकतायें इतनी अल्प होती हैं कि उन्हें किसी से कोई भी वस्तु की याचना नहीं करनी पड़ती और न किसी के ऊपर भार बनकर रहते हैं । आत्मतत्व के चिन्तन-मनन, तथा मोक्षमार्ग की आराधना करना ही उनका स्वभाव होता है । और धर्मकथाओं के अतिरिक्त अन्यत्र वे अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देते । *
१. कल्पसूत्र : सूत्र ३८ पृष्ठ ११६.
२. अव्यवहारी एक्को झाणे एयग्गमणो भवे णिरारंभो ।
चत्तकसायपरिग्गह पयत्तचेट्ठो असंगो य || मूलाचार १०१५.
३. भिक्खं चर वस रण्णे थोवं जेमेहि मा वहू जंप ।
दुःखं सह जिण गिद्दा मेति भावेहि सुठु वेरग्गं । । मूलाचार १०/४. ४. भगवती आराधना वि० टी० ६०९.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org