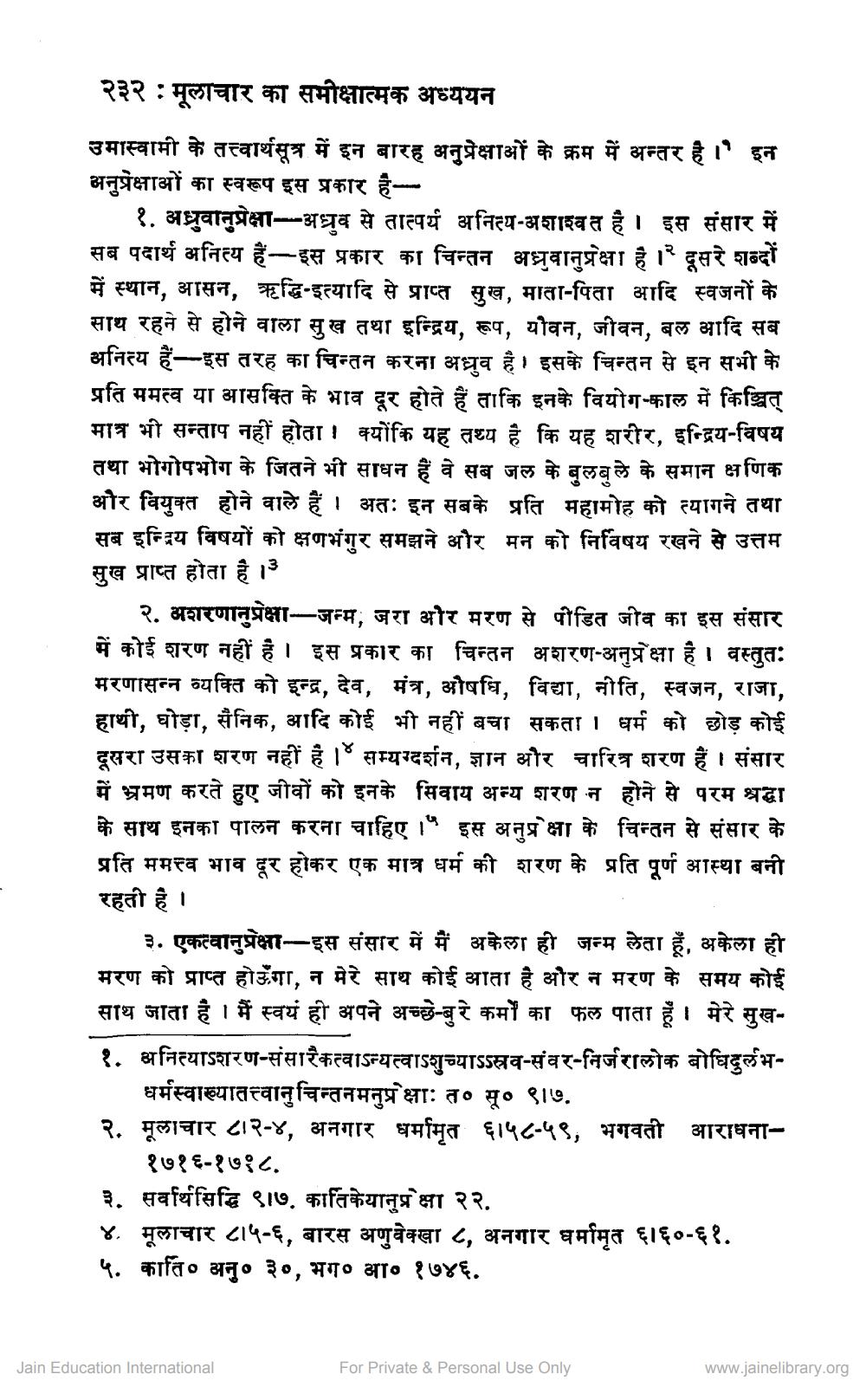________________
२३२ : मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन
उमास्वामी के तत्त्वार्थसूत्र में इन बारह अनुप्रेक्षाओं के क्रम में अन्तर है।' इन अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप इस प्रकार है
१. अध्रुवानुप्रेक्षा--अध्रुव से तात्पर्य अनित्य-अशाश्वत है। इस संसार में सब पदार्थ अनित्य हैं- इस प्रकार का चिन्तन अधूवानुप्रक्षा है। दूसरे शब्दों में स्थान, आसन, ऋद्धि-इत्यादि से प्राप्त सुख, माता-पिता आदि स्वजनों के साथ रहने से होने वाला सुख तथा इन्द्रिय, रूप, यौवन, जीवन, बल आदि सब अनित्य हैं-इस तरह का चिन्तन करना अध्रुव है। इसके चिन्तन से इन सभी के प्रति ममत्व या आसक्ति के भाव दूर होते हैं ताकि इनके वियोग-काल में किञ्चित् मात्र भी सन्ताप नहीं होता। क्योंकि यह तथ्य है कि यह शरीर, इन्द्रिय-विषय तथा भोगोपभोग के जितने भी साधन हैं वे सब जल के बुलबुले के समान क्षणिक और वियुक्त होने वाले हैं । अतः इन सबके प्रति महामोह को त्यागने तथा सब इन्द्रिय विषयों को क्षणभंगुर समझने और मन को निविषय रखने से उत्तम सुख प्राप्त होता है।
२. अशरणानुप्रेक्षा-जन्म, जरा और मरण से पीडित जीव का इस संसार में कोई शरण नहीं है। इस प्रकार का चिन्तन अशरण-अनुप्रेक्षा है । वस्तुतः मरणासन्न व्यक्ति को इन्द्र, देव, मंत्र, औषधि, विद्या, नीति, स्वजन, राजा, हाथी, घोड़ा, सैनिक, आदि कोई भी नहीं बचा सकता । धर्म को छोड़ कोई दूसरा उसका शरण नहीं है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र शरण हैं । संसार में भ्रमण करते हुए जीवों को इनके सिवाय अन्य शरण न होने से परम श्रद्धा के साथ इनका पालन करना चाहिए। इस अनुप्रक्षा के चिन्तन से संसार के प्रति ममत्त्व भाव दूर होकर एक मात्र धर्म की शरण के प्रति पूर्ण आस्था बनी रहती है।
३. एकत्वानुप्रेक्षा-इस संसार में मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ, अकेला ही मरण को प्राप्त होऊँगा, न मेरे साथ कोई आता है और न मरण के समय कोई साथ जाता है । मैं स्वयं ही अपने अच्छे-बुरे कर्मों का फल पाता हूँ। मेरे सुख१. अनित्याऽशरण-संसारैकत्वाऽन्यत्वाऽशुच्याऽऽस्रव-संवर-निर्जरालोक बोधिदुर्लभ
धर्मस्वाख्यातत्त्वानु चिन्तनमनुप्रेक्षाः त० सू० ९।७. २. मूलाचार ८।२-४, अनगार धर्मामृत ६।५८-५९, भगवती आराधना
१७१६-१७१८. ३. सर्वार्थसिद्धि ९।७. कार्तिकेयानुप्रेक्षा २२. ४. मूलाचार ८५-६, बारस अणुवेक्खा ८, अनगार धर्मामृत ६।६०-६१. ५. काति० अनु० ३०, भग० आ० १७४६.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org