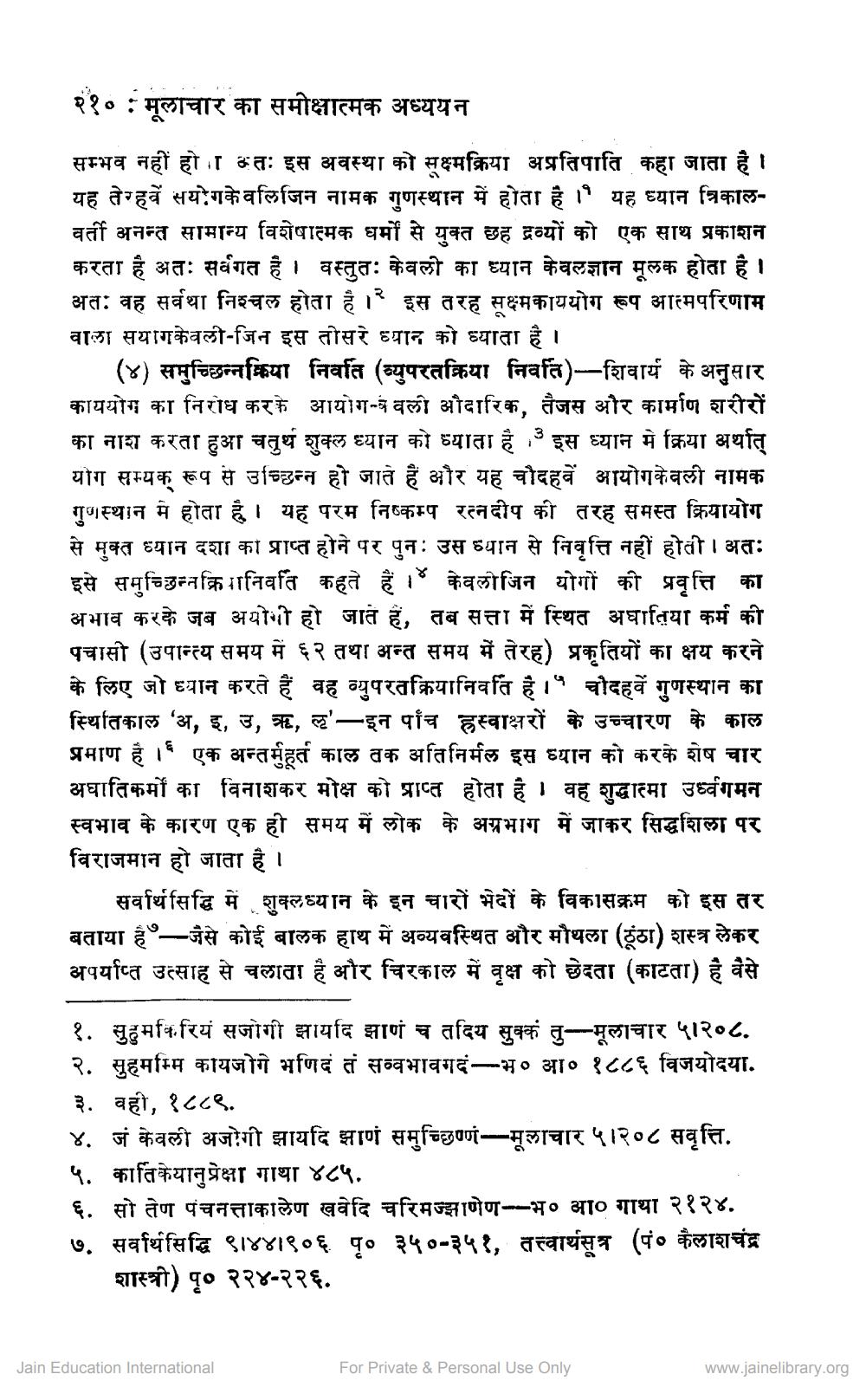________________
२१० : मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन सम्भव नहीं हो । अतः इस अवस्था को सुक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति कहा जाता है। यह तेरहवें सयोगके वलिजिन नामक गुणस्थान में होता है । यह ध्यान त्रिकालवर्ती अनन्त सामान्य विशेषात्मक धर्मों से युक्त छह द्रव्यों को एक साथ प्रकाशन करता है अतः सर्वगत है । वस्तुतः केवली का ध्यान केवलज्ञान मूलक होता है। अतः वह सर्वथा निश्चल होता है। इस तरह सक्ष्मकाययोग रूप आत्मपरिणाम वाला सयागकेवली-जिन इस तीसरे ध्यान को ध्याता है।
(४) समुच्छिन्नक्रिया निवति (व्युपरतक्रिया निवति)-शिवार्य के अनुसार काययोग का निरोध करके आयोग- वली औदारिक, तैजस और कार्माण शरीरों का नाश करता हुआ चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्याता है । इस ध्यान मे क्रिया अर्थात् योग सम्यक् रूप से उच्छिन्न हो जाते हैं और यह चौदहवें आयोगकेवली नामक गुणस्थान में होता है। यह परम निष्कम्प रत्नदीप की तरह समस्त क्रियायोग से मुक्त ध्यान दशा का प्राप्त होने पर पुनः उस ध्यान से निवृत्ति नहीं होती। अतः इसे समुच्छिन्न क्रिमानिति कहते हैं। केवलोजिन योगों की प्रवृत्ति का अभाव करके जब अयोगी हो जाते हैं, तब सत्ता में स्थित अघातिया कर्म की पचासी (उपान्त्य समय में ६२ तथा अन्त समय में तेरह) प्रकृतियों का क्षय करने के लिए जो ध्यान करते हैं वह व्युपरतक्रियानिवति है।५ चौदहवें गुणस्थान का स्थितिकाल 'अ, इ, उ, ऋ, ल'-इन पाँच ह्रस्वाक्षरों के उच्चारण के काल प्रमाण है। एक अन्तर्मुहूर्त काल तक अतिनिर्मल इस ध्यान को करके शेष चार अघातिकर्मों का विनाशकर मोक्ष को प्राप्त होता है । वह शुद्धात्मा उर्ध्वगमन स्वभाव के कारण एक ही समय में लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्धशिला पर विराजमान हो जाता है।
सर्वार्थसिद्धि में शुक्लध्यान के इन चारों भेदों के विकासक्रम को इस तर बताया है जैसे कोई बालक हाथ में अव्यवस्थित और मौथला (ठूठा) शस्त्र लेकर अपर्याप्त उत्साह से चलाता है और चिरकाल में वृक्ष को छेदता (काटता) है वैसे
१. सुहुमकिरियं सजोगी झायर्याद झाणं च तदिय सुक्कं तु-मूलाचार ५।२०८. २. सुहमम्मि कायजोगे भणिदं तं सव्वभावगदं-भ० आ० १८८६ विजयोदया. ३. वही, १८८९. ४. जं केवली अजोगी झायदि झाणं समुच्छिण्णं-मूलाचार ५।२०८ सवृत्ति. ५. कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा ४८५. ६. सो तेण पंचनत्ताकालेण खवेदि चरिमज्झाणेण-भ० आ० गाथा २१२४. ७. सर्वार्थसिद्धि ९।४४।९०६. पृ० ३५०-३५१, तत्त्वार्थसूत्र (पं० कैलाशचंद्र
शास्त्री) पृ० २२४-२२६.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org