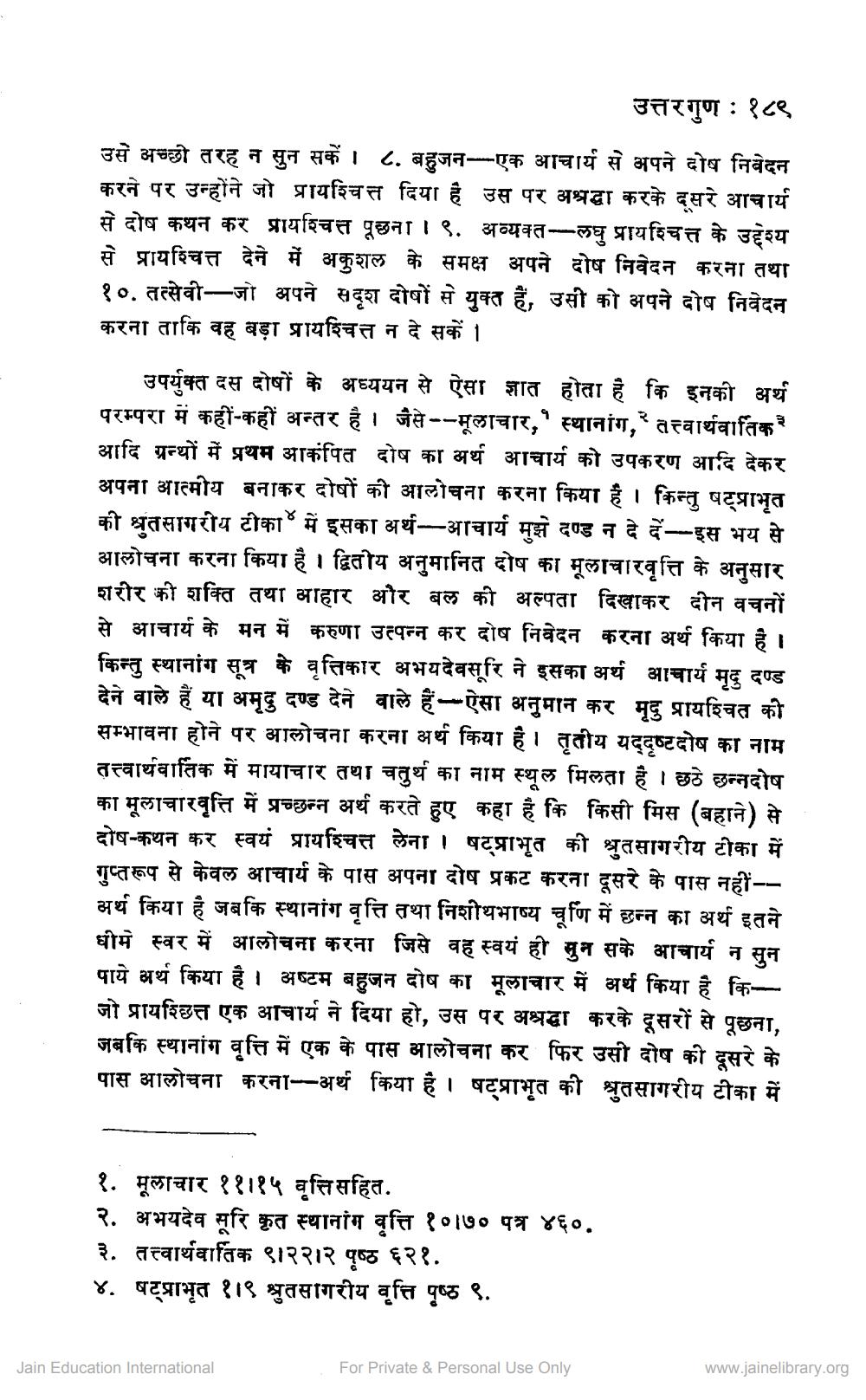________________
उत्तरगुण : १८९ उसे अच्छी तरह न सुन सकें। ८. बहुजन-एक आचार्य से अपने दोष निवेदन करने पर उन्होंने जो प्रायश्चित्त दिया है उस पर अश्रद्धा करके दुसरे आचार्य से दोष कथन कर प्रायश्चित्त पूछना । ९. अव्यक्त-लघु प्रायश्चित्त के उद्देश्य से प्रायश्चित्त देने में अकुशल के समक्ष अपने दोष निवेदन करना तथा १०. तत्सेवी-जो अपने सदृश दोषों से युक्त है, उसी को अपने दोष निवेदन करना ताकि वह बड़ा प्रायश्चित्त न दे सकें।
उपर्युक्त दस दोषों के अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि इनकी अर्थ परम्परा में कहीं-कहीं अन्तर है । जैसे--मूलाचार,' स्थानांग, तत्त्वार्थवार्तिक आदि ग्रन्थों में प्रथम आकंपित दोष का अर्थ आचार्य को उपकरण आदि देकर अपना आत्मीय बनाकर दोषों की आलोचना करना किया है । किन्तु षट्प्राभृत की श्रुतसागरीय टीका' में इसका अर्थ-आचार्य मुझे दण्ड न दे दें-इस भय से आलोचना करना किया है । द्वितीय अनुमानित दोष का मूलाचारवृत्ति के अनुसार शरीर की शक्ति तथा आहार और बल की अल्पता दिखाकर दीन वचनों से आचार्य के मन में करुणा उत्पन्न कर दोष निवेदन करना अर्थ किया है । किन्तु स्थानांग सूत्र के वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने इसका अर्थ आचार्य मृदु दण्ड देने वाले हैं या अमृदु दण्ड देने वाले हैं-ऐसा अनुमान कर मृदु प्रायश्चित की सम्भावना होने पर आलोचना करना अर्थ किया है। तृतीय यदृष्ट दोष का नाम तत्त्वार्थवार्तिक में मायाचार तथा चतुर्थ का नाम स्थूल मिलता है । छठे छन्नदोष का मूलाचारवृत्ति में प्रच्छन्न अर्थ करते हुए कहा है कि किसी मिस (बहाने) से दोष-कथन कर स्वयं प्रायश्चित्त लेना । षट्प्राभृत की श्रुतसागरीय टीका में गुप्तरूप से केवल आचार्य के पास अपना दोष प्रकट करना दूसरे के पास नहीं-- अर्थ किया है जबकि स्थानांग वृत्ति तथा निशीथभाष्य चूणि में छन्न का अर्थ इतने धीमे स्वर में आलोचना करना जिसे वह स्वयं ही सुन सके आचार्य न सुन पाये अर्थ किया है। अष्टम बहुजन दोष का मूलाचार में अर्थ किया है किजो प्रायश्छित्त एक आचार्य ने दिया हो, उस पर अश्रद्धा करके दूसरों से पूछना, जबकि स्थानांग वृत्ति में एक के पास आलोचना कर फिर उसी दोष को दूसरे के पास आलोचना करना-अर्थ किया है । षट्प्राभूत की श्रुतसागरीय टीका में
१. मूलाचार ११११५ वृत्ति सहित. २. अभयदेव सरि कृत स्थानांग वृत्ति १०७० पत्र ४६०. ३. तत्त्वार्थवार्तिक ९।२२।२ पृष्ठ ६२१. ४. षट्प्राभृत १९ श्रुतसागरीय वृत्ति पृष्ठ ९.
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org