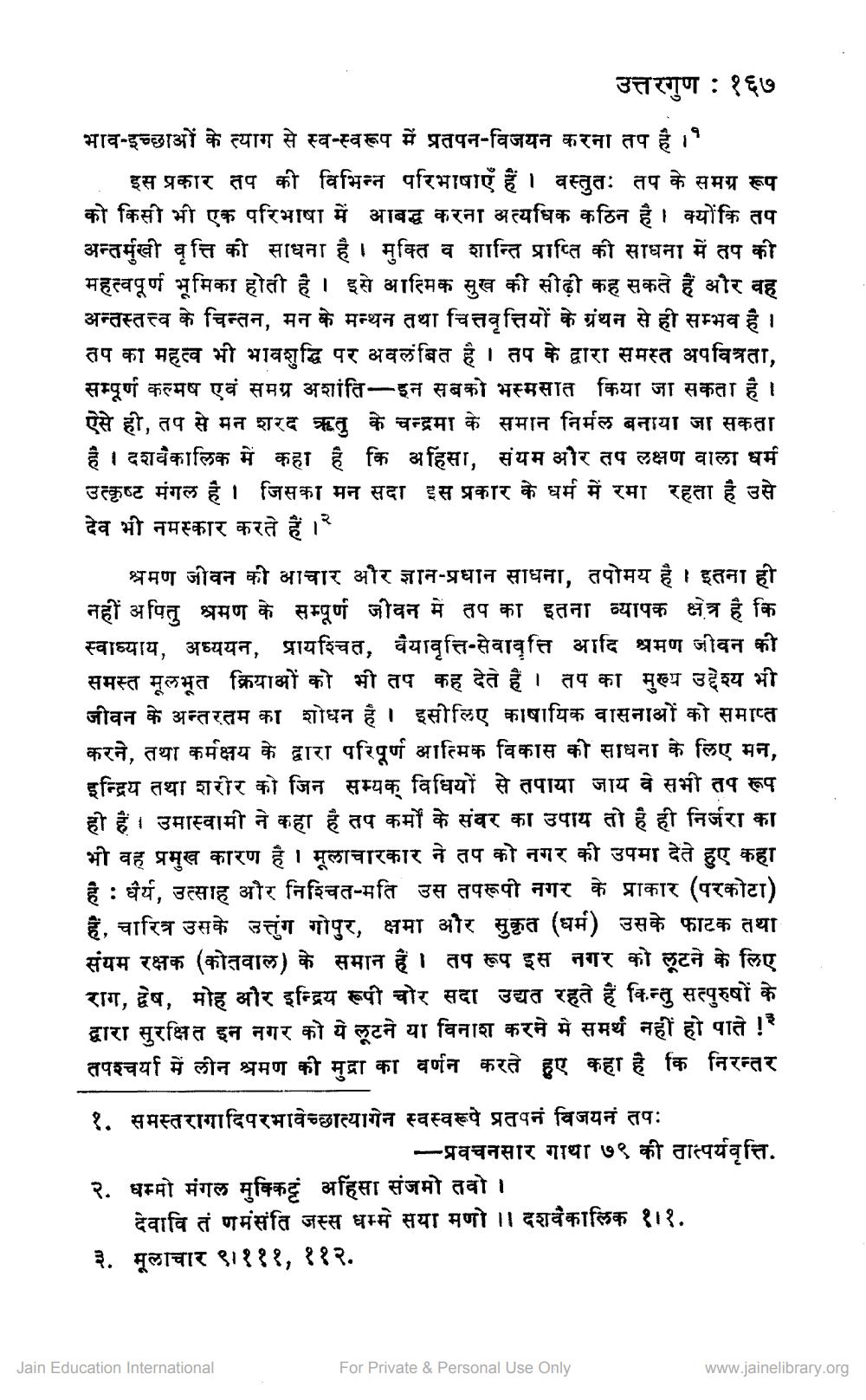________________
उत्तरगुण : १६७ भाव-इच्छाओं के त्याग से स्व-स्वरूप में प्रतपन-विजयन करना तप है।' - इस प्रकार तप की विभिन्न परिभाषाएँ हैं। वस्तुतः तप के समग्र रूप को किसी भी एक परिभाषा में आबद्ध करना अत्यधिक कठिन है। क्योंकि तप अन्तर्मुखी वृत्ति की साधना है । मुक्ति व शान्ति प्राप्ति की साधना में तप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे आत्मिक सुख की सीढ़ी कह सकते हैं और वह अन्तस्तत्त्व के चिन्तन, मन के मन्थन तथा चित्तवृत्तियों के ग्रंथन से ही सम्भव है। तप का महत्व भी भावशुद्धि पर अवलंबित है । तप के द्वारा समस्त अपवित्रता, सम्पूर्ण कल्मष एवं समग्र अशांति-इन सबको भस्मसात किया जा सकता है। ऐसे ही, तप से मन शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल बनाया जा सकता है । दशवकालिक में कहा है कि अहिंसा, संयम और तप लक्षण वाला धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जिसका मन सदा इस प्रकार के धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं ।२
श्रमण जीवन की आचार और ज्ञान-प्रधान साधना, तपोमय है । इतना ही नहीं अपितु श्रमण के सम्पूर्ण जीवन में तप का इतना व्यापक क्षेत्र है कि स्वाध्याय, अध्ययन, प्रायश्चित, वैयावृत्ति-सेवावृत्ति आदि श्रमण जीवन की समस्त मूलभूत क्रियाओं को भी तप कह देते हैं । तप का मुख्य उद्देश्य भी जीवन के अन्तरतम का शोधन है। इसीलिए काषायिक वासनाओं को समाप्त करने, तथा कर्मक्षय के द्वारा परिपूर्ण आत्मिक विकास की साधना के लिए मन, इन्द्रिय तथा शरीर को जिन सम्यक् विधियों से तपाया जाय वे सभी तप रूप ही हैं। उमास्वामी ने कहा है तप कर्मों के संवर का उपाय तो है ही निर्जरा का भी वह प्रमुख कारण है । मूलाचारकार ने तप को नगर की उपमा देते हुए कहा है : धैर्य, उत्साह और निश्चित-मति उस तपरूपी नगर के प्राकार (परकोटा) है, चारित्र उसके उत्तुंग गोपुर, क्षमा और सुकृत (धर्म) उसके फाटक तथा संयम रक्षक (कोतवाल) के समान हैं। तप रूप इस नगर को लूटने के लिए राग, द्वेष, मोह और इन्द्रिय रूपी चोर सदा उद्यत रहते हैं किन्तु सत्पुरुषों के द्वारा सुरक्षित इन नगर को ये लूटने या विनाश करने में समर्थ नहीं हो पाते ! तपश्चर्या में लीन श्रमण की मुद्रा का वर्णन करते हुए कहा है कि निरन्तर १. समस्तरागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः
-प्रवचनसार गाथा ७९ की तात्पर्यवृत्ति. २. धम्मो मंगल मुक्किट्टं अहिंसा संजमो तवो।
देवावि तं णमंसंति जस्स धम्मे सया मणो ।। दशवकालिक १६१. ३. मूलाचार ९।१११, ११२.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org