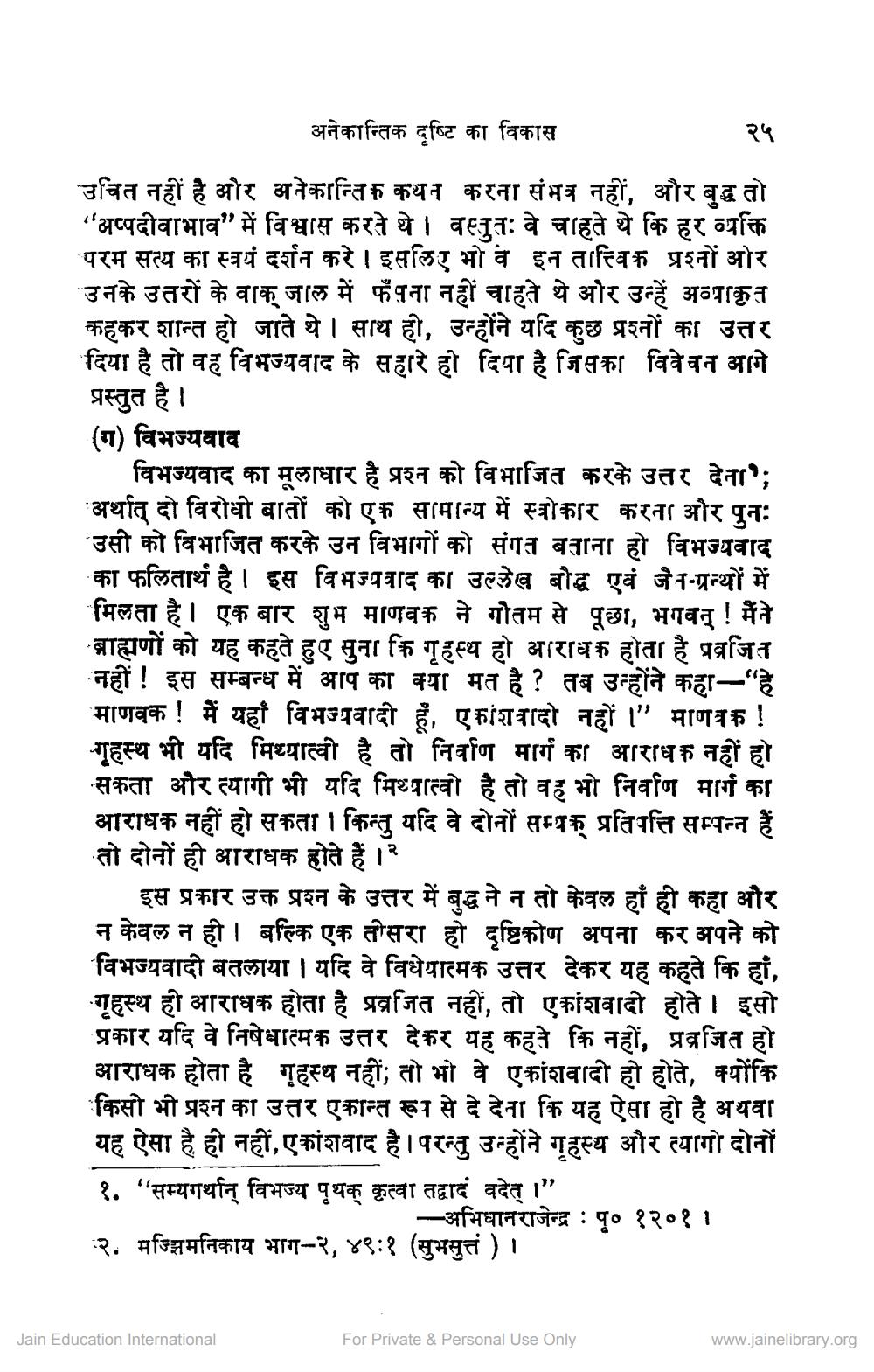________________
अनेकान्तिक दृष्टि का विकास
२५
उचित नहीं है और अनेकान्तिक कथन करना संभव नहीं, और बुद्ध तो "अप्पदीवाभाव" में विश्वास करते थे । वस्तुतः वे चाहते थे कि हर व्यक्ति परम सत्य का स्वयं दर्शन करे । इसलिए भी वे इन तात्त्विक प्रश्नों ओर 1 उनके उत्तरों के वाक् जाल में फँसना नहीं चाहते थे और उन्हें अव्याकृत कहकर शान्त हो जाते थे। साथ ही, उन्होंने यदि कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है तो वह विभज्यवाद के सहारे ही दिया है जिसका विवेचन आगे प्रस्तुत है ।
(ग) विभज्यवाद
विभज्यवाद का मूलाधार है प्रश्न को विभाजित करके उत्तर देना' ; अर्थात् दो विरोधी बातों को एक सामान्य में स्त्रोकार करना और पुनः उसी को विभाजित करके उन विभागों को संगत बनाना हो विभज्यवाद का फलितार्थ है । इस विभज्यवाद का उल्लेख बौद्ध एवं जैन-ग्रन्थों में मिलता है । एक बार शुभ माणवक ने गौतम से पूछा, भगवन् ! मैंने - ब्राह्मणों को यह कहते हुए सुना कि गृहस्थ हो आराधक होता है प्रव्रजित - नहीं ! इस सम्बन्ध में आप का क्या मत है ? तब उन्होंने कहा - "हे माणवक ! मैं यहां विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं ।" माणवक ! गृहस्थ भी यदि मिथ्यात्वी है तो निर्वाण मार्ग का आराधक नहीं हो सकता और त्यागी भी यदि मिथ्यात्वो है तो वह भो निर्वाण मार्ग का आराधक नहीं हो सकता । किन्तु यदि वे दोनों सम्यक् प्रतिपत्ति सम्पन्न हैं तो दोनों ही आराधक होते हैं ।
इस प्रकार उक्त प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने न तो केवल हाँ ही कहा और न केवल न ही । बल्कि एक तीसरा हो दृष्टिकोण अपना कर अपने को विभज्यवादी बतलाया । यदि वे विधेयात्मक उत्तर देकर यह कहते कि हाँ, -गृहस्थ ही आराधक होता है प्रव्रजित नहीं, तो एकांशवादी होते । इसी प्रकार यदि वे निषेधात्मक उत्तर देकर यह कहते कि नहीं, प्रव्रजित हो आराधक होता है गृहस्थ नहीं; तो भो वे एकांशवादी हो होते, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर एकान्त रूप से दे देना कि यह ऐसा हो है अथवा यह ऐसा है ही नहीं, एकांशवाद है । परन्तु उन्होंने गृहस्थ और त्यागो दोनों १. " सम्यगर्थान् विभज्य पृथक् कृत्वा तद्वादं वदेत् ।”
- अभिधान राजेन्द्र : पू० १२०१ ।
२. मज्झिमनिकाय भाग-२, ४९: १ ( सुभसुत्तं ) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org