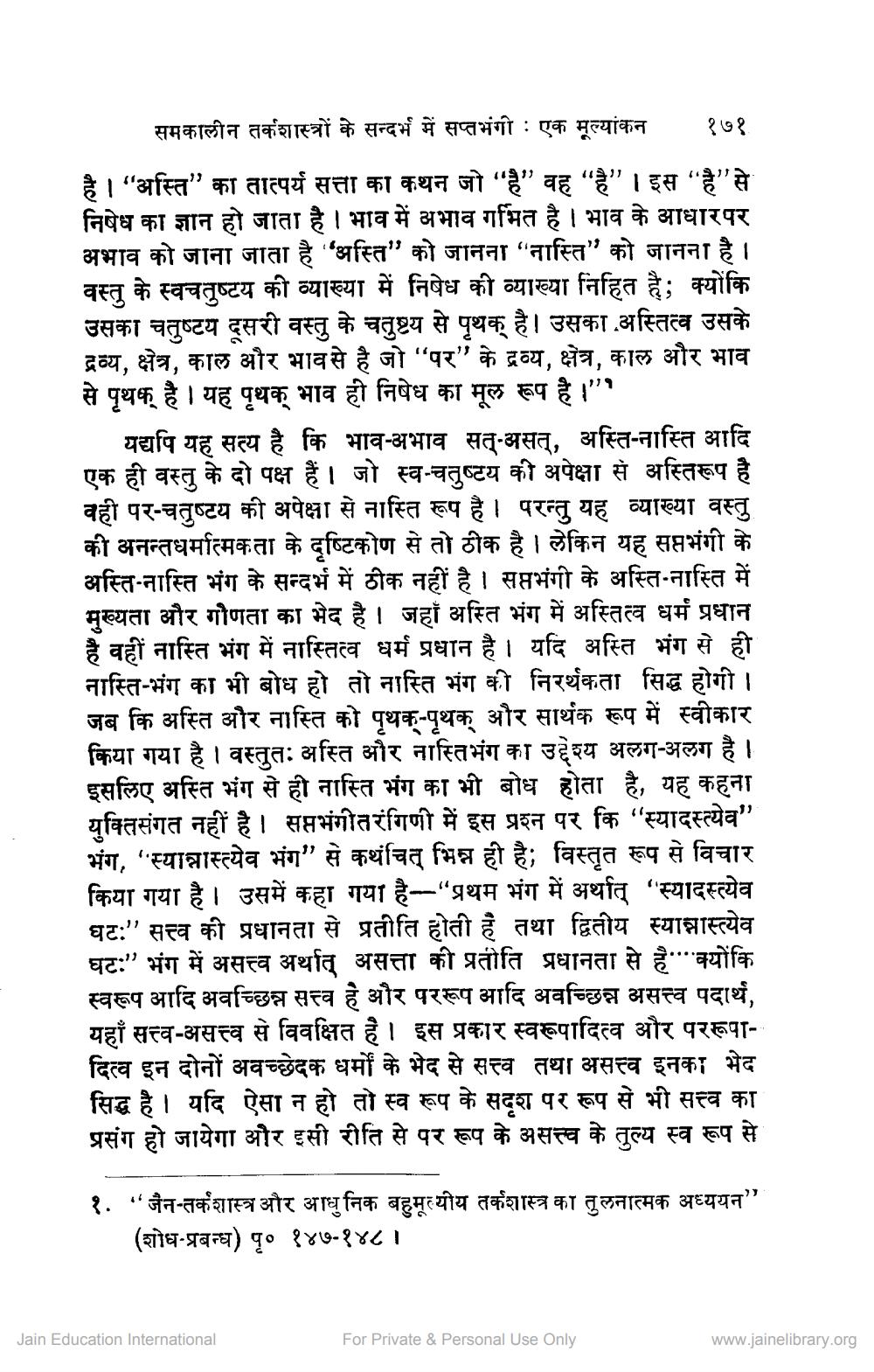________________
समकालीन तर्कशास्त्रों के सन्दर्भ में सप्तभंगी : एक मूल्यांकन
१७१
है । “अस्ति" का तात्पर्य सत्ता का कथन जो "है" वह “है" । इस "है" से निषेध का ज्ञान हो जाता है । भाव में अभाव गर्भित है । भाव के आधारपर अभाव को जाना जाता है "अस्ति" को जानना "नास्ति" को जानना है। वस्तु के स्वचतुष्टय की व्याख्या में निषेध की व्याख्या निहित है; क्योंकि उसका चतुष्टय दूसरी वस्तु के चतुष्टय से पृथक् है। उसका अस्तित्व उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे है जो "पर" के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से पृथक् है । यह पृथक् भाव ही निषेध का मूल रूप है।''
यद्यपि यह सत्य है कि भाव-अभाव सत्-असत्, अस्ति-नास्ति आदि एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। जो स्व-चतुष्टय की अपेक्षा से अस्तिरूप है वही पर-चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। परन्तु यह व्याख्या वस्तु की अनन्तधर्मात्मकता के दृष्टिकोण से तो ठीक है । लेकिन यह सप्तभंगी के अस्ति-नास्ति भंग के सन्दर्भ में ठीक नहीं है। सप्तभंगी के अस्ति-नास्ति में मुख्यता और गौणता का भेद है। जहाँ अस्ति भंग में अस्तित्व धर्म प्रधान है वहीं नास्ति भंग में नास्तित्व धर्म प्रधान है। यदि अस्ति भंग से ही नास्ति-भंग का भी बोध हो तो नास्ति भंग की निरर्थकता सिद्ध होगी। जब कि अस्ति और नास्ति को पृथक-पृथक् और सार्थक रूप में स्वीकार किया गया है । वस्तुतः अस्ति और नास्तिभंग का उद्देश्य अलग-अलग है । इसलिए अस्ति भंग से ही नास्ति भंग का भी बोध होता है, यह कहना युक्तिसंगत नहीं है। सप्तभंगीतरंगिणी में इस प्रश्न पर कि "स्यादस्त्येव" भंग, "स्यानास्त्येव भंग" से कथंचित् भिन्न ही है; विस्तृत रूप से विचार किया गया है। उसमें कहा गया है-"प्रथम भंग में अर्थात् "स्यादस्त्येव घट:' सत्त्व की प्रधानता से प्रतीति होती है तथा द्वितीय स्यान्नास्त्येव घटः" भंग में असत्त्व अर्थात् असत्ता की प्रतीति प्रधानता से है क्योंकि स्वरूप आदि अवच्छिन्न सत्त्व है और पररूप आदि अवच्छिन्न असत्त्व पदार्थ, यहाँ सत्त्व-असत्त्व से विवक्षित है। इस प्रकार स्वरूपादित्व और पररूपादित्व इन दोनों अवच्छेदक धर्मों के भेद से सत्त्व तथा असत्त्व इनका भेद सिद्ध है। यदि ऐसा न हो तो स्व रूप के सदृश पर रूप से भी सत्त्व का प्रसंग हो जायेगा और इसी रीति से पर रूप के असत्त्व के तुल्य स्व रूप से
१. 'जैन-तर्कशास्त्र और आधुनिक बहुमूल्यीय तर्कशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन"
(शोध-प्रबन्ध) पृ० १४७-१४८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org