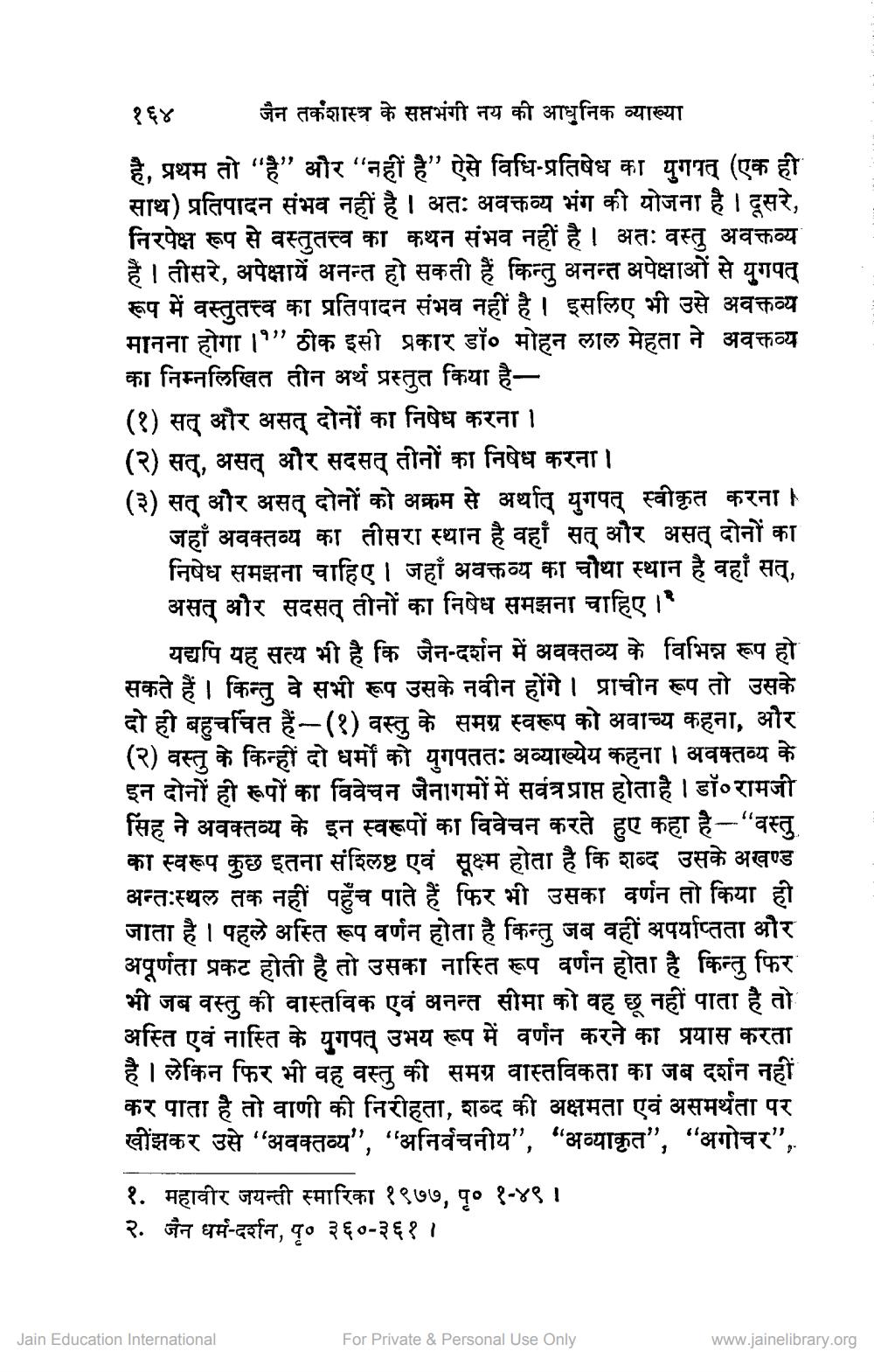________________
१६४
जैन तर्कशास्त्र के सप्तभंगी नय की आधुनिक व्याख्या
है, प्रथम तो " है" और "नहीं है" ऐसे विधि प्रतिषेध का युगपत् (एक ही साथ) प्रतिपादन संभव नहीं है । अतः अवक्तव्य भंग की योजना है । दूसरे, निरपेक्ष रूप से वस्तुतत्त्व का कथन संभव नहीं है । अतः वस्तु अवक्तव्य हैं । तीसरे, अपेक्षायें अनन्त हो सकती हैं किन्तु अनन्त अपेक्षाओं से युगपत् रूप में वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन संभव नहीं है । इसलिए भी उसे अवक्तव्य मानना होगा । " ठीक इसी प्रकार डॉ० मोहन लाल मेहता ने अवक्तव्य का निम्नलिखित तीन अर्थ प्रस्तुत किया है—
(१) सत् और असत् दोनों का निषेध करना ।
(२) सत्, असत् और सदसत् तीनों का निषेध करना ।
(३) सत् और असत् दोनों को अक्रम से अर्थात् युगपत् स्वीकृत करना । जहाँ अवक्तव्य का तीसरा स्थान है वहाँ सत् और असत् दोनों का निषेध समझना चाहिए । जहाँ अवक्तव्य का चौथा स्थान है वहाँ सत् असत् और सदसत् तीनों का निषेध समझना चाहिए ।
यद्यपि यह सत्य भी है कि जैन दर्शन में अवक्तव्य के विभिन्न रूप हो सकते हैं । किन्तु वे सभी रूप उसके नवीन होंगे। प्राचीन रूप तो उसके दो ही बहुचर्चित हैं - (१) वस्तु के समग्र स्वरूप को अवाच्य कहना, और (२) वस्तु के किन्हीं दो धर्मों को युगपततः अव्याख्येय कहना । अवक्तव्य के इन दोनों ही रूपों का विवेचन जैनागमों में सर्वत्र प्राप्त होता है । डॉ० रामजी सिंह ने अवक्तव्य के इन स्वरूपों का विवेचन करते हुए कहा है- “वस्तु का स्वरूप कुछ इतना संश्लिष्ट एवं सूक्ष्म होता है कि शब्द उसके अखण्ड अन्तःस्थल तक नहीं पहुँच पाते हैं फिर भी उसका वर्णन तो किया ही जाता है । पहले अस्ति रूप वर्णन होता है किन्तु जब वहीं अपर्याप्तता और अपूर्णता प्रकट होती है तो उसका नास्ति रूप वर्णन होता है किन्तु फिर भी जब वस्तु की वास्तविक एवं अनन्त सीमा को वह छू नहीं पाता है तो अस्ति एवं नास्ति के युगपत् उभय रूप में वर्णन करने का प्रयास करता है । लेकिन फिर भी वह वस्तु की समग्र वास्तविकता का जब दर्शन नहीं कर पाता है तो वाणी की निरीहता, शब्द की अक्षमता एवं असमर्थता पर खींझकर उसे "अवक्तव्य", "अनिर्वचनीय", "अव्याकृत", "अगोचर”,
१. महावीर जयन्ती स्मारिका १९७७, पृ० १-४९ ।
२. जैन धर्म - दर्शन, पृ० ३६० - ३६१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org