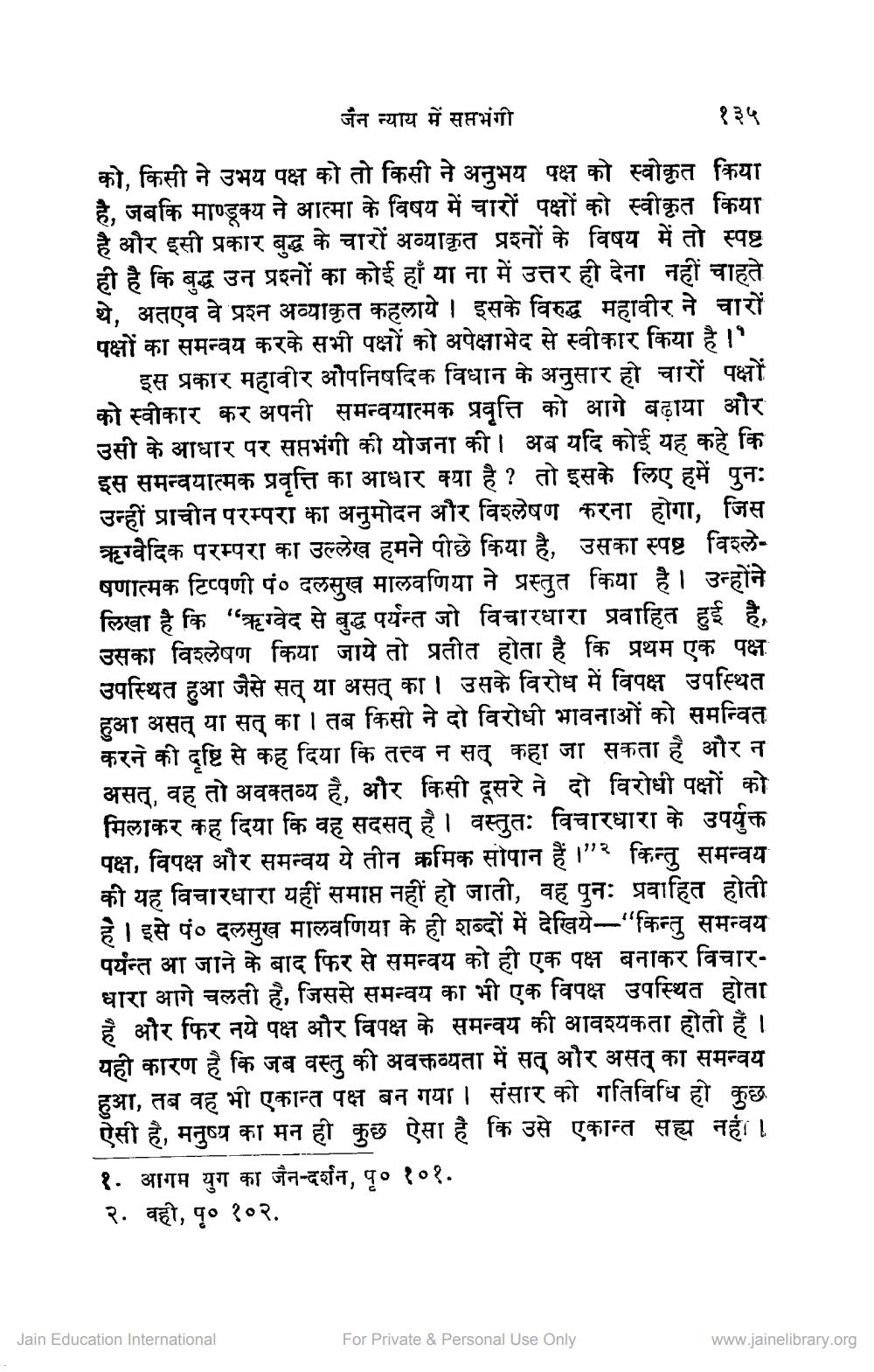________________
जैन न्याय में सप्तभंगी
को, किसी ने उभय पक्ष को तो किसी ने अनुभय पक्ष को स्वीकृत किया है, जबकि माण्डूक्य ने आत्मा के विषय में चारों पक्षों को स्वीकृत किया है और इसी प्रकार बुद्ध के चारों अव्याकृत प्रश्नों के विषय में तो स्पष्ट ही है कि बुद्ध उन प्रश्नों का कोई हाँ या ना में उत्तर ही देना नहीं चाहते थे, अतएव वे प्रश्न अव्याकृत कहलाये। इसके विरुद्ध महावीर ने चारों पक्षों का समन्वय करके सभी पक्षों को अपेक्षाभेद से स्वीकार किया है।'
इस प्रकार महावीर औपनिषदिक विधान के अनुसार हो चारों पक्षों को स्वीकार कर अपनी समन्वयात्मक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया और उसी के आधार पर सप्तभंगी की योजना की। अब यदि कोई यह कहे कि इस समन्वयात्मक प्रवृत्ति का आधार क्या है ? तो इसके लिए हमें पुनः उन्हीं प्राचीन परम्परा का अनुमोदन और विश्लेषण करना होगा, जिस ऋग्वैदिक परम्परा का उल्लेख हमने पीछे किया है, उसका स्पष्ट विश्लेषणात्मक टिप्पणी पं० दलसुख मालवणिया ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि "ऋग्वेद से बुद्ध पर्यन्त जो विचारधारा प्रवाहित हुई है, उसका विश्लेषण किया जाये तो प्रतीत होता है कि प्रथम एक पक्ष उपस्थित हुआ जैसे सत् या असत् का। उसके विरोध में विपक्ष उपस्थित हुआ असत् या सत् का । तब किसी ने दो विरोधी भावनाओं को समन्वित करने की दृष्टि से कह दिया कि तत्त्व न सत् कहा जा सकता है और न असत्, वह तो अवक्तव्य है, और किसी दूसरे ने दो विरोधी पक्षों को मिलाकर कह दिया कि वह सदसत् है। वस्तुतः विचारधारा के उपर्युक्त पक्ष, विपक्ष और समन्वय ये तीन क्रमिक सोपान हैं ।"२ किन्तु समन्वय की यह विचारधारा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, वह पुनः प्रवाहित होती है। इसे पं० दलसुख मालवणिया के ही शब्दों में देखिये-"किन्तु समन्वय पर्यन्त आ जाने के बाद फिर से समन्वय को ही एक पक्ष बनाकर विचारधारा आगे चलती है, जिससे समन्वय का भी एक विपक्ष उपस्थित होता है और फिर नये पक्ष और विपक्ष के समन्वय की आवश्यकता होती हैं। यही कारण है कि जब वस्तु की अवक्तव्यता में सत् और असत् का समन्वय हुआ, तब वह भी एकान्त पक्ष बन गया। संसार को गतिविधि हो कुछ ऐसी है, मनुष्य का मन ही कुछ ऐसा है कि उसे एकान्त सह्य नहः । १. आगम युग का जैन-दर्शन, पृ० १०१. २. वही, पृ० १०२.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org