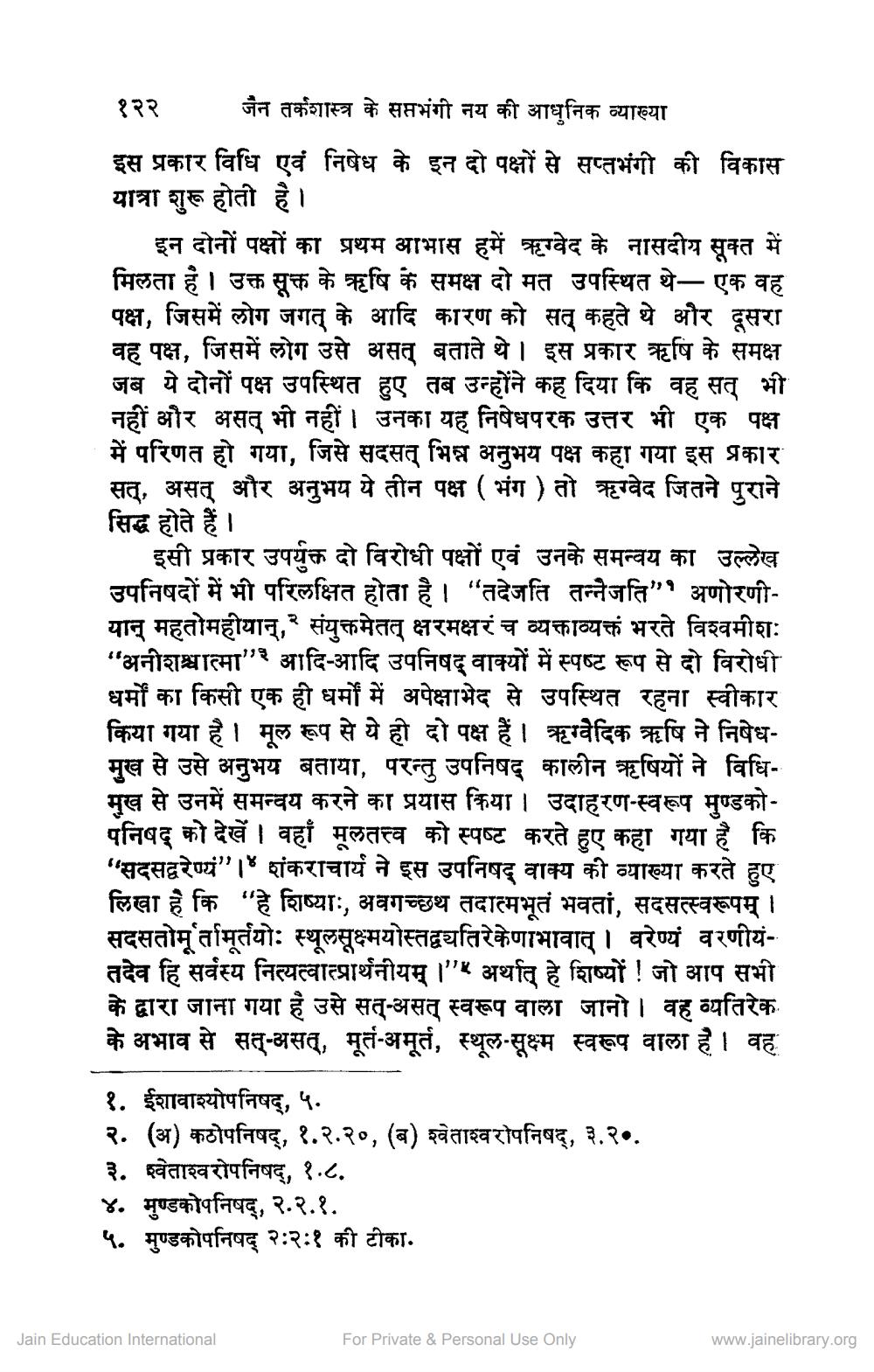________________
१२२
जैन तर्कशास्त्र के सप्तभंगी नय की आधुनिक व्याख्या
इस प्रकार विधि एवं निषेध के इन दो पक्षों से सप्तभंगी की विकास यात्रा शुरू होती है ।
इन दोनों पक्षों का प्रथम आभास हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है । उक्त सूक्त के ऋषि के समक्ष दो मत उपस्थित थे - एक वह पक्ष, जिसमें लोग जगत् के आदि कारण को सत् कहते थे और दूसरा वह पक्ष, जिसमें लोग उसे असत् बताते थे । इस प्रकार ऋषि के समक्ष जब ये दोनों पक्ष उपस्थित हुए तब उन्होंने कह दिया कि वह सत् भी नहीं और असत् भी नहीं । उनका यह निषेधपरक उत्तर भी एक पक्ष में परिणत हो गया, जिसे सदसत् भिन्न अनुभय पक्ष कहा गया इस प्रकार सत्, असत् और अनुभय ये तीन पक्ष (भंग) तो ऋग्वेद जितने पुराने सिद्ध होते हैं ।
२
।
इसी प्रकार उपर्युक्त दो विरोधी पक्षों एवं उनके समन्वय का उल्लेख उपनिषदों में भी परिलक्षित होता है । " तदेजति तन्नेजति " " अणोरणीयान् महतो महीयान् संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः "अनीशश्वात्मा आदि-आदि उपनिषद् वाक्यों में स्पष्ट रूप से दो विरोधी धर्मों का किसी एक ही धर्मों में अपेक्षाभेद से उपस्थित रहना स्वीकार किया गया है । मूल रूप से ये ही दो पक्ष हैं ऋग्वैदिक ऋषि ने निषेधमुख से उसे अनुभय बताया, परन्तु उपनिषद् कालीन ऋषियों ने विधिसे उनमें समन्वय करने का प्रयास किया । उदाहरण-स्वरूप मुण्डको - मुख पनिषद् को देखें । वहाँ मूलतत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि " सदसद्वरेण्यं" । शंकराचार्य ने इस उपनिषद् वाक्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि "हे शिष्याः, अवगच्छथ तदात्मभूतं भवतां सदसत्स्वरूपम् । सदसतोर्मू तमूर्तयोः स्थूलसूक्ष्मयोस्तद्व्यतिरेकेणाभावात् । वरेण्यं वरणीयंतदेव हि सर्वस्य नित्यत्वात्प्रार्थनीयम् ।"" अर्थात् हे शिष्यों ! जो आप सभी के द्वारा जाना गया है उसे सत्-असत् स्वरूप वाला जानो । वह व्यतिरेक के अभाव से सत्-असत् मूर्त-अमूर्त स्थूल सूक्ष्म स्वरूप वाला है । वह
,
१. ईशावास्योपनिषद्, ५.
२. (अ) कठोपनिषद्, १.२.२०, (ब) श्वेताश्व रोपनिषद्, ३.२०.
३. श्वेताश्वरोपनिषद्, १.८.
४. मुण्डकोपनिषद्, २.२.१.
५. मुण्डकोपनिषद् २:२:१ की टीका.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org