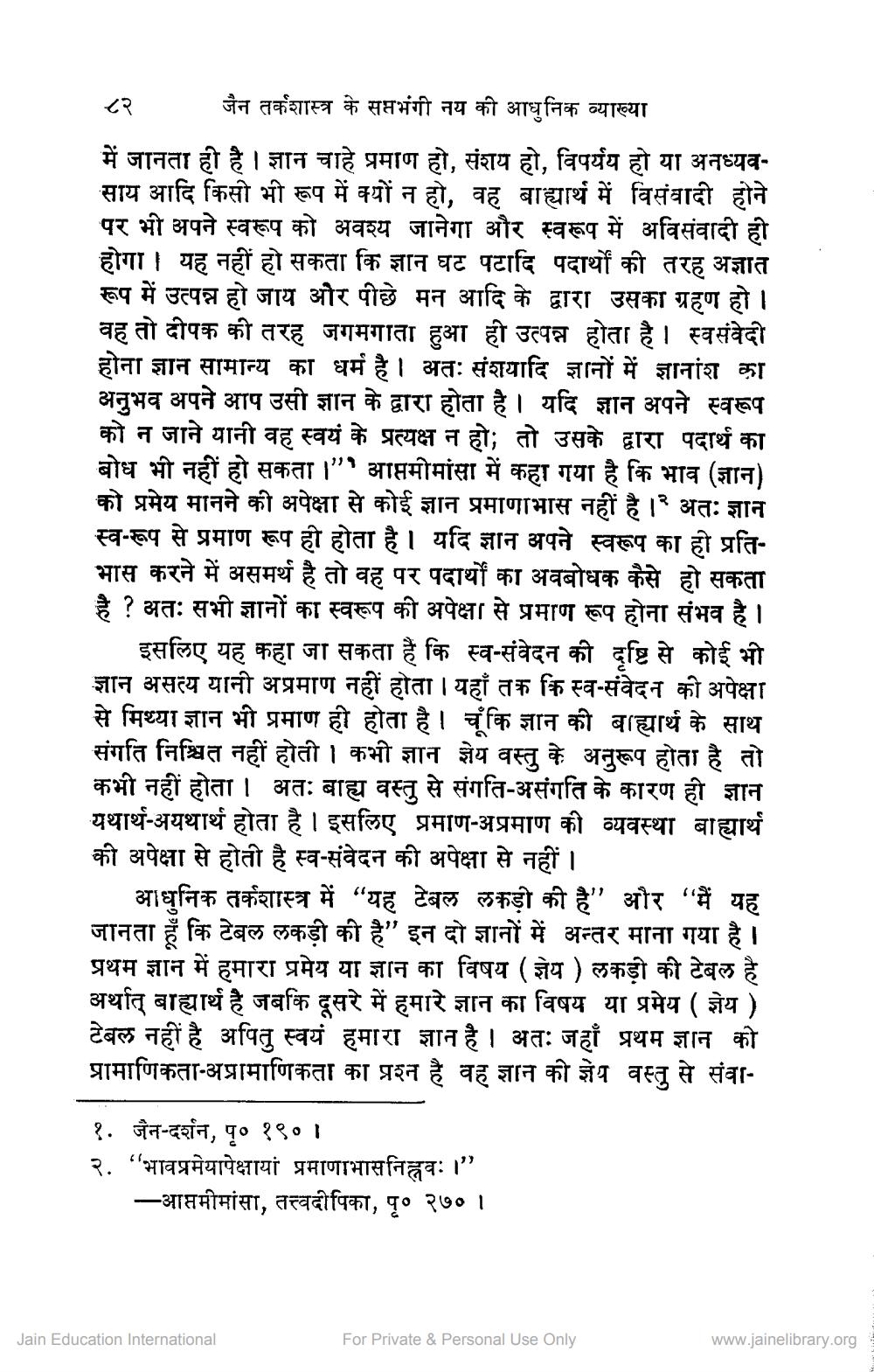________________
८२ जैन तर्कशास्त्र के सप्तभंगी नय की आधुनिक व्याख्या में जानता ही है । ज्ञान चाहे प्रमाण हो, संशय हो, विपर्यय हो या अनध्यवसाय आदि किसी भी रूप में क्यों न हो, वह बाह्यार्थ में विसंवादी होने पर भी अपने स्वरूप को अवश्य जानेगा और स्वरूप में अविसंवादी ही होगा। यह नहीं हो सकता कि ज्ञान घट पटादि पदार्थों की तरह अज्ञात रूप में उत्पन्न हो जाय और पीछे मन आदि के द्वारा उसका ग्रहण हो । वह तो दीपक की तरह जगमगाता हुआ ही उत्पन्न होता है। स्वसंवेदो होना ज्ञान सामान्य का धर्म है। अतः संशयादि ज्ञानों में ज्ञानांश का अनुभव अपने आप उसी ज्ञान के द्वारा होता है। यदि ज्ञान अपने स्वरूप को न जाने यानी वह स्वयं के प्रत्यक्ष न हो; तो उसके द्वारा पदार्थ का बोध भी नहीं हो सकता।"' आप्तमीमांसा में कहा गया है कि भाव (ज्ञान) को प्रमेय मानने की अपेक्षा से कोई ज्ञान प्रमाणाभास नहीं है । अतः ज्ञान स्व-रूप से प्रमाण रूप ही होता है। यदि ज्ञान अपने स्वरूप का ही प्रतिभास करने में असमर्थ है तो वह पर पदार्थों का अवबोधक कैसे हो सकता है ? अतः सभी ज्ञानों का स्वरूप की अपेक्षा से प्रमाण रूप होना संभव है।
इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्व-संवेदन की दृष्टि से कोई भी ज्ञान असत्य यानी अप्रमाण नहीं होता । यहाँ तक कि स्व-संवेदन की अपेक्षा से मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण ही होता है। चूंकि ज्ञान की बाह्यार्थ के साथ संगति निश्चित नहीं होती। कभी ज्ञान ज्ञेय वस्तु के अनुरूप होता है तो कभी नहीं होता। अतः बाह्य वस्तु से संगति-असंगति के कारण ही ज्ञान यथार्थ-अयथार्थ होता है । इसलिए प्रमाण-अप्रमाण की व्यवस्था बाह्यार्थ की अपेक्षा से होती है स्व-संवेदन की अपेक्षा से नहीं।
आधुनिक तर्कशास्त्र में “यह टेबल लकड़ी की है" और "मैं यह जानता हूँ कि टेबल लकड़ी की है" इन दो ज्ञानों में अन्तर माना गया है। प्रथम ज्ञान में हमारा प्रमेय या ज्ञान का विषय (ज्ञेय ) लकड़ी की टेबल है अर्थात् बाह्यार्थ है जबकि दूसरे में हमारे ज्ञान का विषय या प्रमेय ( ज्ञेय ) टेबल नहीं है अपितु स्वयं हमारा ज्ञान है । अतः जहाँ प्रथम ज्ञान को प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता का प्रश्न है वह ज्ञान को ज्ञेय वस्तु से संवा
१. जैन-दर्शन, पृ० १९० । २. "भावप्रमेयापेक्षायां प्रमाणाभासनिह्नवः।"
-आप्तमीमांसा, तत्त्वदीपिका, पृ० २७० ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org