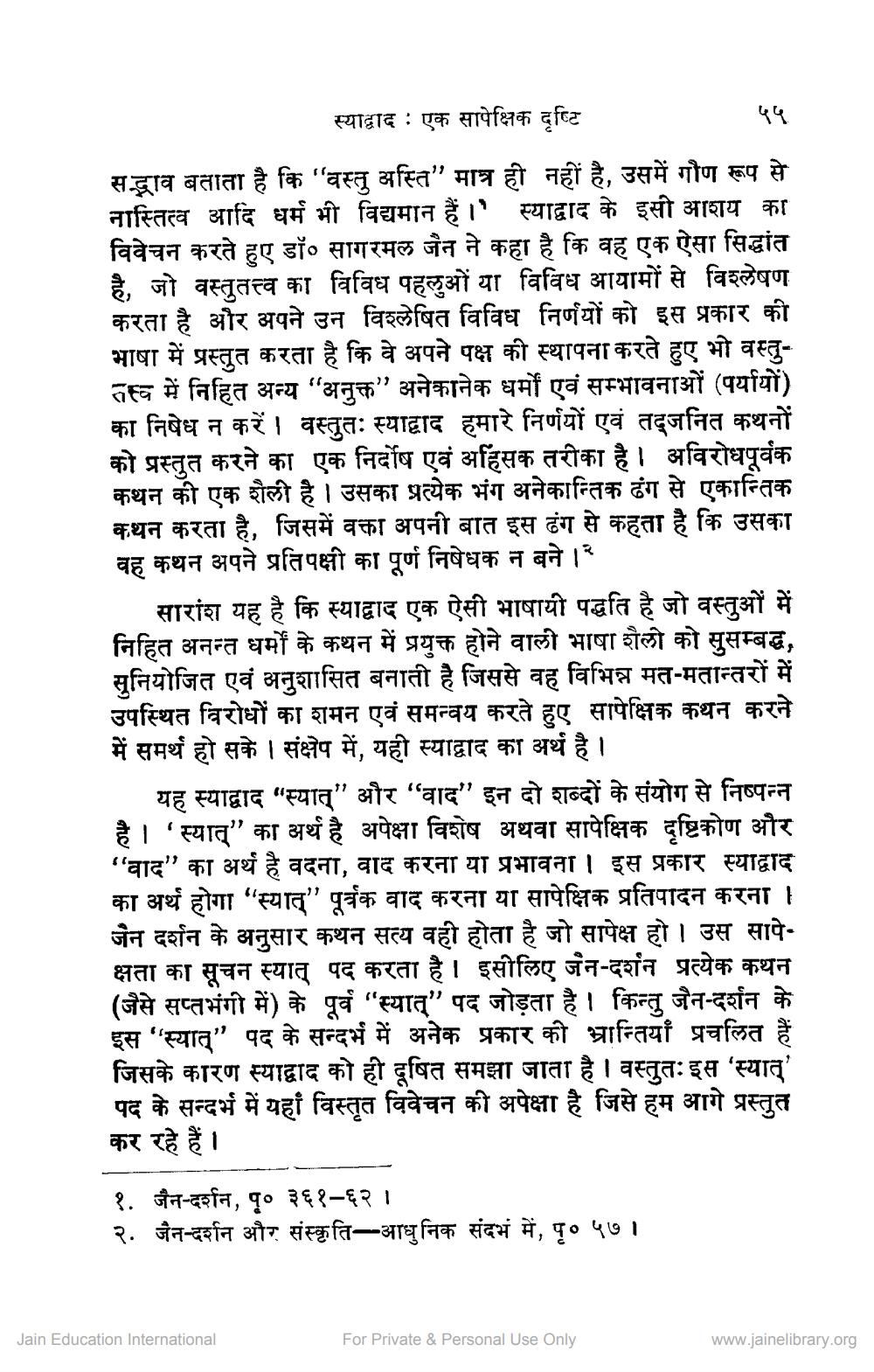________________
स्याद्वाद : एक सापेक्षिक दृष्टि
५५ सद्भाव बताता है कि "वस्तु अस्ति" मात्र ही नहीं है, उसमें गौण रूप से नास्तित्व आदि धर्म भी विद्यमान हैं।' स्याद्वाद के इसी आशय का विवेचन करते हुए डॉ० सागरमल जैन ने कहा है कि वह एक ऐसा सिद्धांत है, जो वस्तुतत्त्व का विविध पहलुओं या विविध आयामों से विश्लेषण करता है और अपने उन विश्लेषित विविध निर्णयों को इस प्रकार की भाषा में प्रस्तुत करता है कि वे अपने पक्ष की स्थापना करते हुए भी वस्तुतत्व में निहित अन्य "अनुक्त" अनेकानेक धर्मों एवं सम्भावनाओं (पर्यायों) का निषेध न करें। वस्तुतः स्याद्वाद हमारे निर्णयों एवं तदनित कथनों को प्रस्तुत करने का एक निर्दोष एवं अहिंसक तरीका है। अविरोधपूर्वक कथन की एक शैली है। उसका प्रत्येक भंग अनेकान्तिक ढंग से एकान्तिक कथन करता है, जिसमें वक्ता अपनी बात इस ढंग से कहता है कि उसका वह कथन अपने प्रतिपक्षी का पूर्ण निषेधक न बने । २
सारांश यह है कि स्याद्वाद एक ऐसी भाषायी पद्धति है जो वस्तुओं में निहित अनन्त धर्मों के कथन में प्रयुक्त होने वाली भाषा शैलो को सुसम्बद्ध, सुनियोजित एवं अनुशासित बनाती है जिससे वह विभिन्न मत-मतान्तरों में उपस्थित विरोधों का शमन एवं समन्वय करते हुए सापेक्षिक कथन करने में समर्थ हो सके । संक्षेप में, यही स्याद्वाद का अर्थ है ।
यह स्याद्वाद "स्यात्" और "वाद" इन दो शब्दों के संयोग से निष्पन्न है। 'स्यात्" का अर्थ है अपेक्षा विशेष अथवा सापेक्षिक दृष्टिकोण और "वाद" का अर्थ है वदना, वाद करना या प्रभावना। इस प्रकार स्याद्वाद का अर्थ होगा "स्यात्" पूर्वक वाद करना या सापेक्षिक प्रतिपादन करना । जैन दर्शन के अनुसार कथन सत्य वही होता है जो सापेक्ष हो । उस सापेक्षता का सूचन स्यात् पद करता है। इसीलिए जन-दर्शन प्रत्येक कथन (जैसे सप्तभंगी में) के पूर्व "स्यात्" पद जोड़ता है। किन्तु जैन-दर्शन के इस "स्यात्" पद के सन्दर्भ में अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ प्रचलित हैं जिसके कारण स्याद्वाद को ही दूषित समझा जाता है । वस्तुतः इस 'स्यात्' पद के सन्दर्भ में यहां विस्तृत विवेचन की अपेक्षा है जिसे हम आगे प्रस्तुत कर रहे हैं।
१. जैन-दर्शन, पृ० ३६१-६२ । २. जैन-दर्शन और संस्कृति-आधुनिक संदर्भ में, पृ० ५७ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org