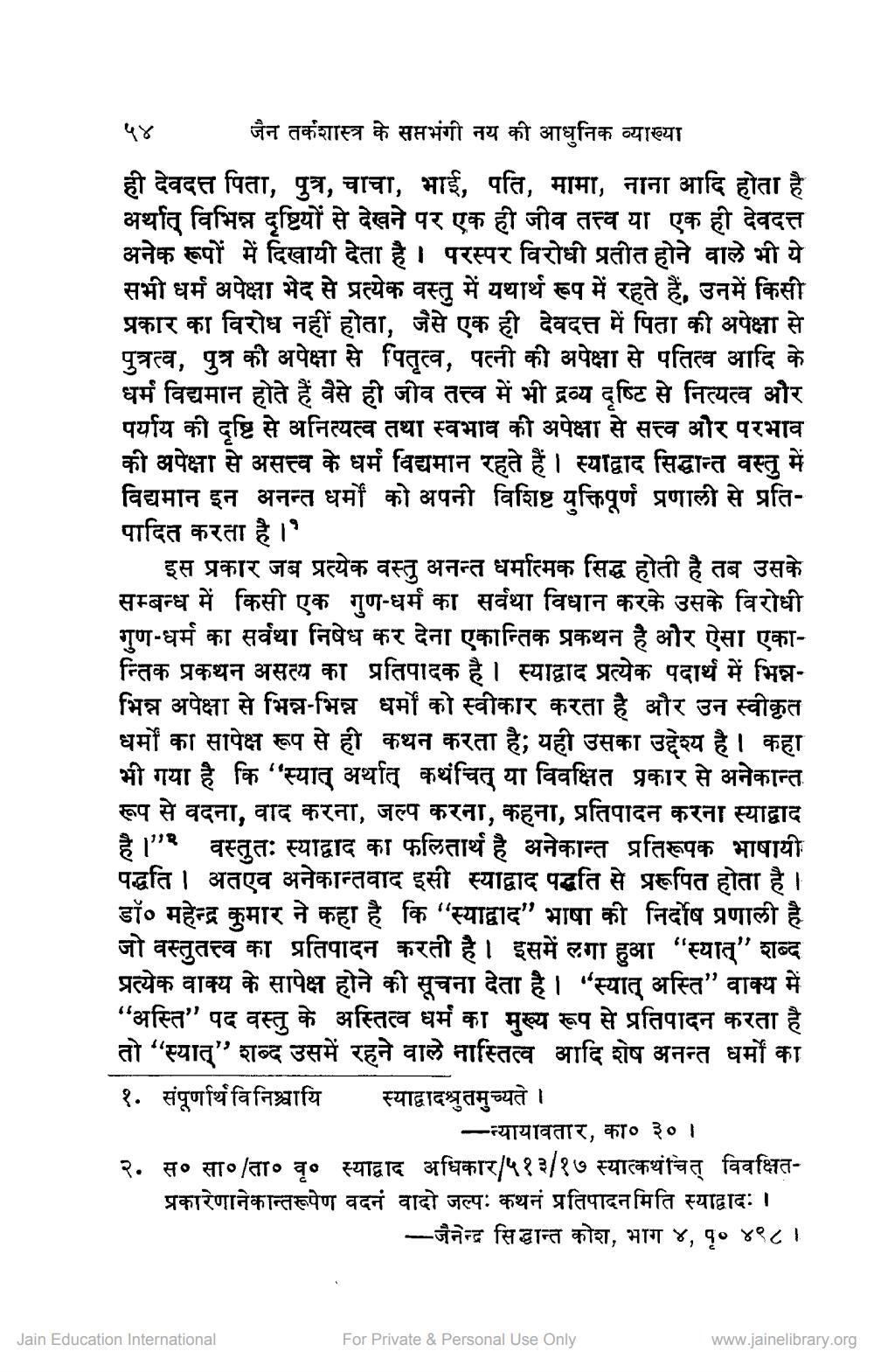________________
जैन तर्कशास्त्र के सप्तभंगी नय की आधुनिक व्याख्या ही देवदत्त पिता, पुत्र, चाचा, भाई, पति, मामा, नाना आदि होता है अर्थात् विभिन्न दृष्टियों से देखने पर एक ही जीव तत्त्व या एक ही देवदत्त अनेक रूपों में दिखायी देता है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भी ये सभी धर्म अपेक्षा भेद से प्रत्येक वस्तु में यथार्थ रूप में रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, जैसे एक ही देवदत्त में पिता की अपेक्षा से पुत्रत्व, पुत्र की अपेक्षा से पितत्व, पत्नी की अपेक्षा से पतित्व आदि के धर्म विद्यमान होते हैं वैसे ही जीव तत्त्व में भी द्रव्य दृष्टि से नित्यत्व और पर्याय की दृष्टि से अनित्यत्व तथा स्वभाव की अपेक्षा से सत्त्व और परभाव की अपेक्षा से असत्त्व के धर्म विद्यमान रहते हैं। स्याद्वाद सिद्धान्त वस्तु में विद्यमान इन अनन्त धर्मों को अपनी विशिष्ट युक्तिपूर्ण प्रणाली से प्रतिपादित करता है।' __ इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक सिद्ध होती है तब उसके सम्बन्ध में किसी एक गुण-धर्म का सर्वथा विधान करके उसके विरोधी गुण-धर्म का सर्वथा निषेध कर देना एकान्तिक प्रकथन है और ऐसा एकान्तिक प्रकथन असत्य का प्रतिपादक है। स्याद्वाद प्रत्येक पदार्थ में भिन्नभिन्न अपेक्षा से भिन्न-भिन्न धर्मों को स्वीकार करता है और उन स्वीकृत धर्मों का सापेक्ष रूप से ही कथन करता है; यही उसका उद्देश्य है। कहा भी गया है कि "स्यात् अर्थात् कथंचित् या विवक्षित प्रकार से अनेकान्त रूप से वदना, वाद करना, जल्प करना, कहना, प्रतिपादन करना स्याद्वाद है।" वस्तुतः स्याद्वाद का फलितार्थ है अनेकान्त प्रतिरूपक भाषायी पद्धति । अतएव अनेकान्तवाद इसी स्याद्वाद पद्धति से प्ररूपित होता है। डॉ० महेन्द्र कुमार ने कहा है कि "स्याद्वाद" भाषा की निर्दोष प्रणाली है जो वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन करती है। इसमें लगा हुआ "स्यात्" शब्द प्रत्येक वाक्य के सापेक्ष होने की सूचना देता है । "स्यात् अस्ति" वाक्य में "अस्ति" पद वस्तु के अस्तित्व धर्म का मुख्य रूप से प्रतिपादन करता है तो “स्यात्' शब्द उसमें रहने वाले नास्तित्व आदि शेष अनन्त धर्मों का १. संपूर्णार्थ विनिश्चायि स्याद्वादश्रुतमुच्यते ।
-न्यायावतार, का० ३० । २. स० सा०/ता० वृ० स्याद्वाद अधिकार/५१३/१७ स्यात्कथंचित विवक्षितप्रकारेणानेकान्तरूपेण वदनं वादो जल्पः कथनं प्रतिपादन मिति स्याद्वादः ।
-जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, पृ० ४९८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org