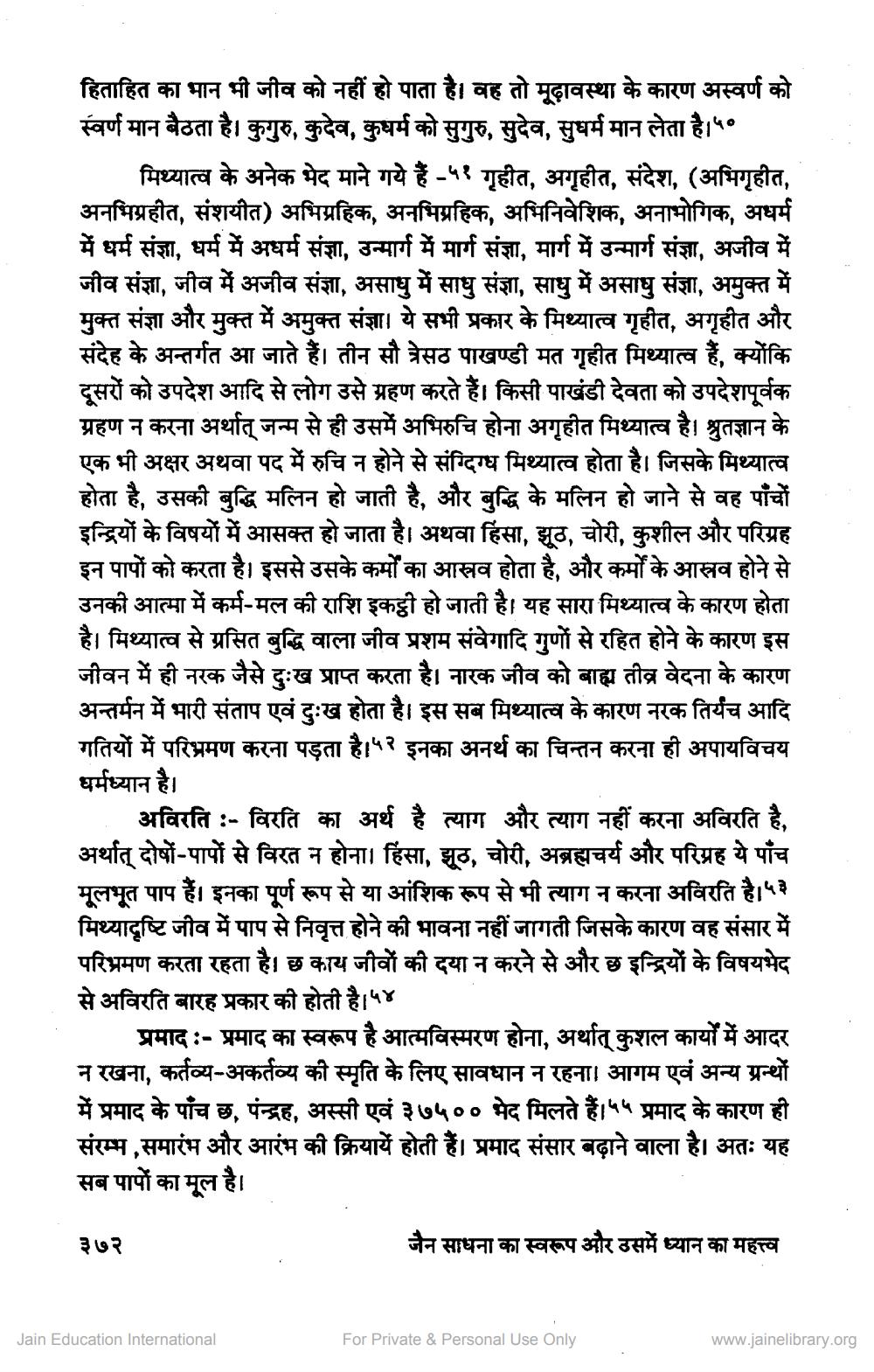________________
हिताहित का भान भी जीव को नहीं हो पाता है। वह तो मूढावस्था के कारण अस्वर्ण को स्वर्ण मान बैठता है। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को सुगुरु, सुदेव, सुधर्म मान लेता है।५०
मिथ्यात्व के अनेक भेद माने गये हैं -५१ गृहीत, अगृहीत, संदेश, (अभिगृहीत, अनभिग्रहीत, संशयीत) अभिग्रहिक, अनभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, अनाभोगिक, अधर्म में धर्म संज्ञा, धर्म में अधर्म संज्ञा, उन्मार्ग में मार्ग संज्ञा, मार्ग में उन्मार्ग संज्ञा, अजीव में जीव संज्ञा, जीव में अजीव संज्ञा, असाधु में साधु संज्ञा, साधु में असाधु संज्ञा, अमुक्त में मुक्त संज्ञा और मुक्त में अमुक्त संज्ञा। ये सभी प्रकार के मिथ्यात्व गृहीत, अगृहीत और संदेह के अन्तर्गत आ जाते हैं। तीन सौ त्रेसठ पाखण्डी मत गृहीत मिथ्यात्व हैं, क्योंकि दूसरों को उपदेश आदि से लोग उसे ग्रहण करते हैं। किसी पाखंडी देवता को उपदेशपूर्वक ग्रहण न करना अर्थात् जन्म से ही उसमें अभिरुचि होना अगृहीत मिथ्यात्व है। श्रुतज्ञान के एक भी अक्षर अथवा पद में रुचि न होने से संग्दिग्ध मिथ्यात्व होता है। जिसके मिथ्यात्व होता है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, और बुद्धि के मलिन हो जाने से वह पांचों इन्द्रियों के विषयों में आसक्त हो जाता है। अथवा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पापों को करता है। इससे उसके कर्मों का आस्रव होता है, और कर्मों के आस्रव होने से उनकी आत्मा में कर्म-मल की राशि इकट्ठी हो जाती है। यह सारा मिथ्यात्व के कारण होता है। मिथ्यात्व से ग्रसित बुद्धि वाला जीव प्रशम संवेगादि गुणों से रहित होने के कारण इस जीवन में ही नरक जैसे दुःख प्राप्त करता है। नारक जीव को बाह्य तीव्र वेदना के कारण अन्तर्मन में भारी संताप एवं दुःख होता है। इस सब मिथ्यात्व के कारण नरक तिर्यच आदि गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है।५२ इनका अनर्थ का चिन्तन करना ही अपायविचय धर्मध्यान है।
अविरति :- विरति का अर्थ है त्याग और त्याग नहीं करना अविरति है, अर्थात् दोषों-पापों से विरत न होना। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह ये पाँच मूलभूत पाप हैं। इनका पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भी त्याग न करना अविरति है।५३ मिथ्यादृष्टि जीव में पाप से निवृत्त होने की भावना नहीं जागती जिसके कारण वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। छ काय जीवों की दया न करने से और छ इन्द्रियों के विषयभेद से अविरति बारह प्रकार की होती है।५४
प्रमाद :- प्रमाद का स्वरूप है आत्मविस्मरण होना, अर्थात् कुशल कार्यों में आदर न रखना, कर्तव्य-अकर्तव्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना। आगम एवं अन्य ग्रन्थों में प्रमाद के पांच छ, पंन्द्रह, अस्सी एवं ३७५०० भेद मिलते हैं।५५ प्रमाद के कारण ही संरम्भ,समारंभ और आरंभ की क्रियायें होती हैं। प्रमाद संसार बढ़ाने वाला है। अतः यह सब पापों का मूल है।
३७२
जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org