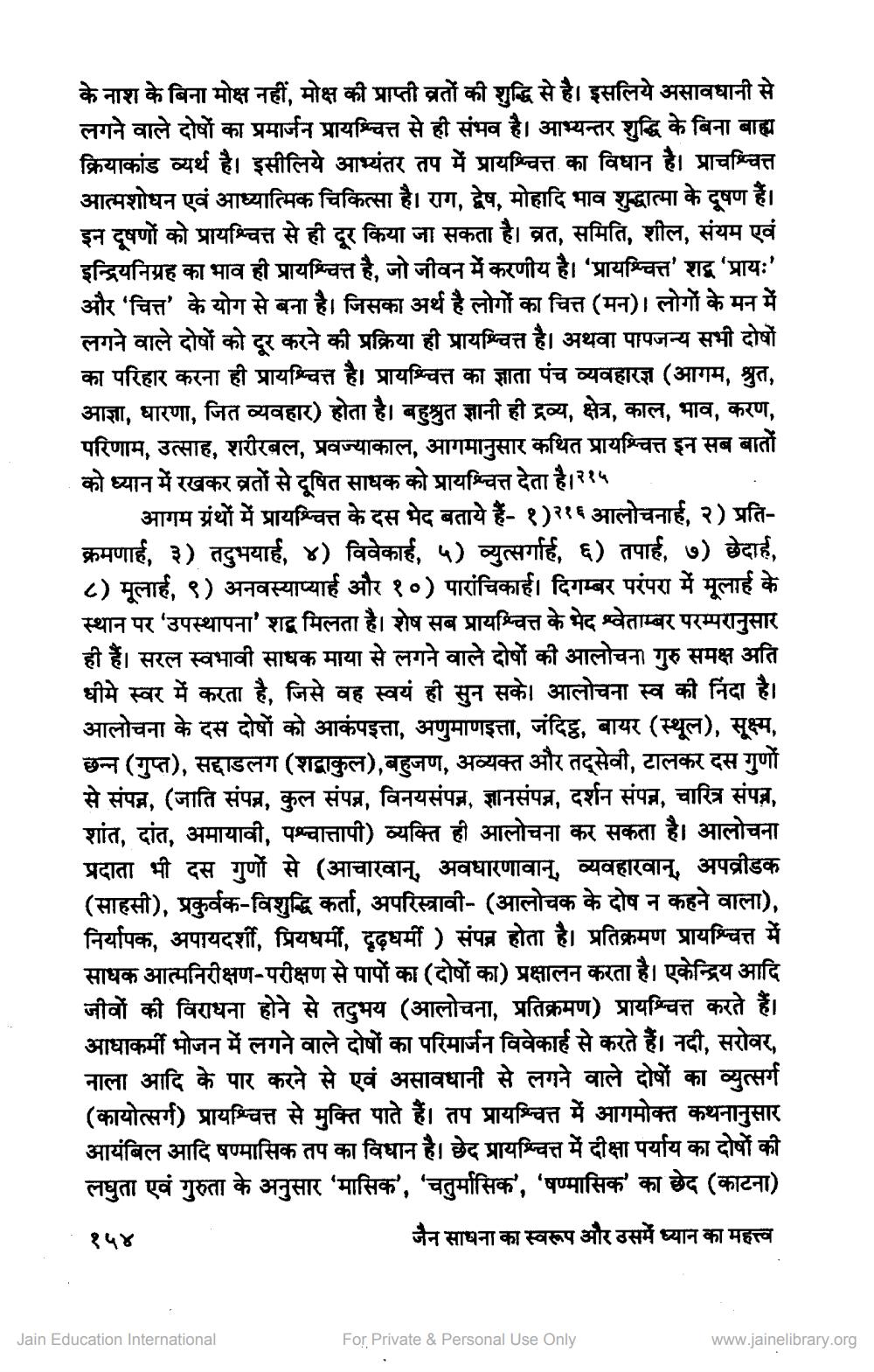________________
के नाश के बिना मोक्ष नहीं, मोक्ष की प्राप्ती व्रतों की शुद्धि से है। इसलिये असावधानी से लगने वाले दोषों का प्रमार्जन प्रायश्चित्त से ही संभव है। आभ्यन्तर शुद्धि के बिना बाह्य क्रियाकांड व्यर्थ है। इसीलिये आभ्यंतर तप में प्रायश्चित्त का विधान है। प्राचश्चित्त आत्मशोधन एवं आध्यात्मिक चिकित्सा है। राग, द्वेष, मोहादि भाव शुद्धात्मा के दूषण हैं। इन दूषणों को प्रायश्चित्त से ही दूर किया जा सकता है। व्रत, समिति, शील, संयम एवं इन्द्रियनिग्रह का भाव ही प्रायश्चित्त है, जो जीवन में करणीय है। 'प्रायश्चित्त' शब्द 'प्रायः ' और 'चित्त' के योग से बना है। जिसका अर्थ है लोगों का चित्त ( मन ) । लोगों के मन में लगने वाले दोषों को दूर करने की प्रक्रिया ही प्रायश्चित्त है। अथवा पापजन्य सभी दोषों का परिहार करना ही प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त का ज्ञाता पंच व्यवहारज्ञ (आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा, जित व्यवहार) होता है। बहुश्रुत ज्ञानी ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, करण, परिणाम, उत्साह, शरीरबल, प्रवज्याकाल, आगमानुसार कथित प्रायश्चित्त इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्रतों से दूषित साधक को प्रायश्चित्त देता है । २१५
आगम ग्रंथों में प्रायश्चित्त के दस भेद बताये हैं- १) २१६ आलोचनार्ह, २) प्रतिक्रमणार्ह, ३) तदुभयार्ह, ४) विवेकार्ह, ५) व्युत्सर्गार्ह, ६) तपार्ह, ७) छेदार्ह, ८) मूलाई, ९) अनवस्याप्यार्ह और १०) पारांचिकाई । दिगम्बर परंपरा में मूलाई के स्थान पर 'उपस्थापना' शद्ब मिलता है। शेष सब प्रायश्चित्त के भेद श्वेताम्बर परम्परानुसार ही हैं। सरल स्वभावी साधक माया से लगने वाले दोषों की आलोचना गुरु समक्ष अति धीमे स्वर में करता है, जिसे वह स्वयं ही सुन सके। आलोचना स्व की निंदा है। आलोचना के दस दोषों को आकंपइत्ता, अणुमाणइत्ता, जंदिट्ठ, बायर (स्थूल), सूक्ष्म, छन्न (गुप्त), सद्दाडलग (शद्वाकुल), बहुजण, अव्यक्त और तद्सेवी, टालकर दस गुणों से संपन्न, (जाति संपन्न, कुल संपन्न, विनयसंपन्न, ज्ञानसंपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, शांत, दांत, अमायावी, पश्चात्तापी) व्यक्ति ही आलोचना कर सकता है। आलोचना प्रदाता भी दस गुणों से ( आचारवान् अवधारणावान्, व्यवहारवान्, अपव्रीडक ( साहसी ), प्रकुर्वक - विशुद्धि कर्ता, अपरिस्त्रावी- (आलोचक के दोष न कहने वाला), निर्यापक, अपायदर्शी, प्रियधर्मी, दृढ़धर्मी ) संपन्न होता है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त में साधक आत्मनिरीक्षण-परीक्षण से पापों का (दोषों का ) प्रक्षालन करता है। एकेन्द्रिय आदि जीवों की विराधना होने से तदुभय (आलोचना, प्रतिक्रमण ) प्रायश्चित्त करते हैं। आधाकर्मी भोजन में लगने वाले दोषों का परिमार्जन विवेकार्ह से करते हैं। नदी, सरोवर, नाला आदि के पार करने से एवं असावधानी से लगने वाले दोषों का व्युत्सर्ग ( कायोत्सर्ग) प्रायश्चित्त से मुक्ति पाते हैं। तप प्रायश्चित्त में आगमोक्त कथनानुसार आयंबिल आदि षण्मासिक तप का विधान है। छेद प्रायश्चित्त में दीक्षा पर्याय का दोषों की लघुता एवं गुरुता के अनुसार 'मासिक', 'चतुर्मासिक', 'षण्मासिक' का छेद (काटना)
१५४
जैन साधना का स्वरूप और उसमें ध्यान का महत्त्व
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org