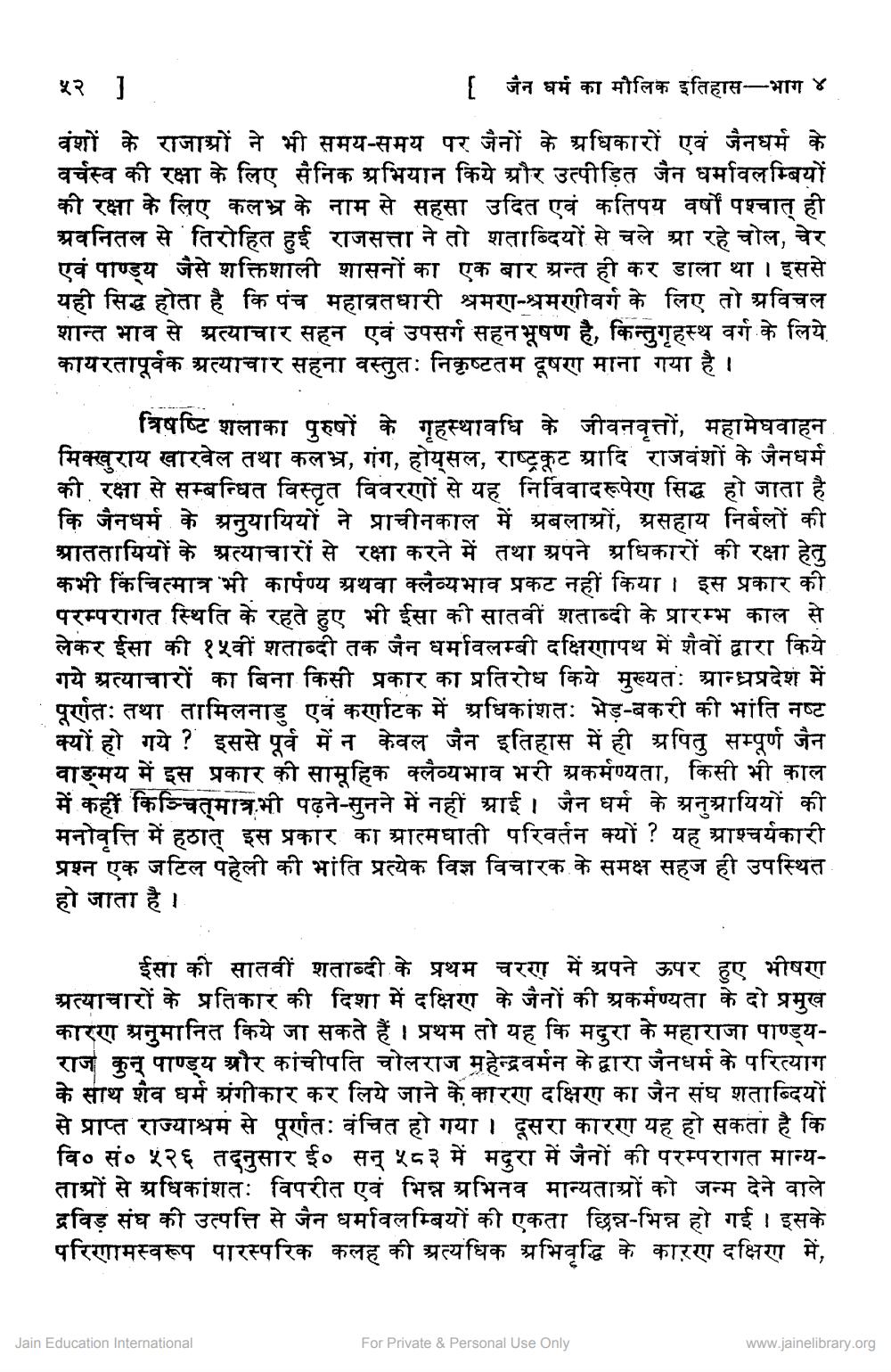________________
५२ J
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास - भाग ४
के
वंशों के राजाओं ने भी समय-समय पर जैनों के अधिकारों एवं जैनधर्म के वर्चस्व की रक्षा के लिए सैनिक अभियान किये और उत्पीड़ित जैन धर्मावलम्बियों की रक्षा के लिए कल नाम से सहसा उदित एवं कतिपय वर्षों पश्चात् ही अवनितल से तिरोहित हुई राजसत्ता ने तो शताब्दियों से चले आ रहे चोल, चेर एवं पाण्ड्य जैसे शक्तिशाली शासनों का एक बार अन्त ही कर डाला था । इससे यही सिद्ध होता है कि पंच महाव्रतधारी श्रमण श्रमरणीवर्ग के लिए तो अविचल शान्त भाव से अत्याचार सहन एवं उपसर्ग सहनभूषण है, किन्तुगृहस्थ वर्ग के लिये.. कायरतापूर्वक अत्याचार सहना वस्तुतः निकृष्टतम दूषरण माना गया है ।
त्रिषष्टि शलाका पुरुषों के गृहस्थावधि के जीवनवृत्तों, महामेघवाहन मिक्खुराय खारवेल तथा कलभ्र, गंग, होय्सल, राष्ट्रकूट आदि राजवंशों के जैनधर्म की रक्षा से सम्बन्धित विस्तृत विवरणों से यह निर्विवादरूपेण सिद्ध हो जाता है कि जैनधर्म के अनुयायियों ने प्राचीनकाल में अबलाओंों, असहाय निर्बलों की श्राततायियों के अत्याचारों से रक्षा करने में तथा अपने अधिकारों की रक्षा हेतु कभी किंचित्मात्र भी कार्पण्य अथवा क्लैव्यभाव प्रकट नहीं किया । इस प्रकार की परम्परागत स्थिति के रहते हुए भी ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल से लेकर ईसा की १५वीं शताब्दी तक जैन धर्मावलम्बी दक्षिणापथ में शैवों द्वारा किये गये अत्याचारों का बिना किसी प्रकार का प्रतिरोध किये मुख्यतः आन्ध्रप्रदेश में पूर्णतः तथा तामिलनाडु एवं करर्णाटक में अधिकांशतः भेड़-बकरी की भांति नष्ट क्यों हो गये ? इससे पूर्व में न केवल जैन इतिहास में ही अपितु सम्पूर्ण जैन वाङ्मय में इस प्रकार की सामूहिक क्लैव्यभाव भरी अकर्मण्यता, किसी भी काल में कहीं किञ्चित् मात्र भी पढ़ने-सुनने में नहीं आई। जैन धर्म के अनुनायियों की मनोवृत्ति में हठात् इस प्रकार का आत्मघाती परिवर्तन क्यों ? यह आश्चर्यकारी प्रश्न एक जटिल पहेली की भांति प्रत्येक विज्ञ विचारक के समक्ष सहज ही उपस्थित हो जाता है ।
ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रथम चरण में अपने ऊपर हुए भीषण अत्याचारों के प्रतिकार की दिशा में दक्षिण के जैनों की अकर्मण्यता के दो प्रमुख कारण अनुमानित किये जा सकते हैं । प्रथम तो यह कि मदुरा के महाराजा पाण्ड्यराज कुन् पाण्ड्य और कांचीपति चोलराज महेन्द्रवर्मन के द्वारा जैनधर्म के परित्याग के साथ शैव धर्म अंगीकार कर लिये जाने के कारण दक्षिण का जैन संघ शताब्दियों से प्राप्त राज्याश्रमं से पूर्णतः वंचित हो गया । दूसरा कारण यह हो सकता है कि वि० सं० ५२६ तद्नुसार ई० सन् ५८३ में मदुरा में जैनों की परम्परागत मान्यताओं से अधिकांशतः विपरीत एवं भिन्न अभिनव मान्यताओं को जन्म देने वाले द्रविड़ संघ की उत्पत्ति से जैन धर्मावलम्बियों की एकता छिन्न-भिन्न हो गई । इसके परिणामस्वरूप पारस्परिक कलह की अत्यधिक अभिवृद्धि के कारण दक्षिण में,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org