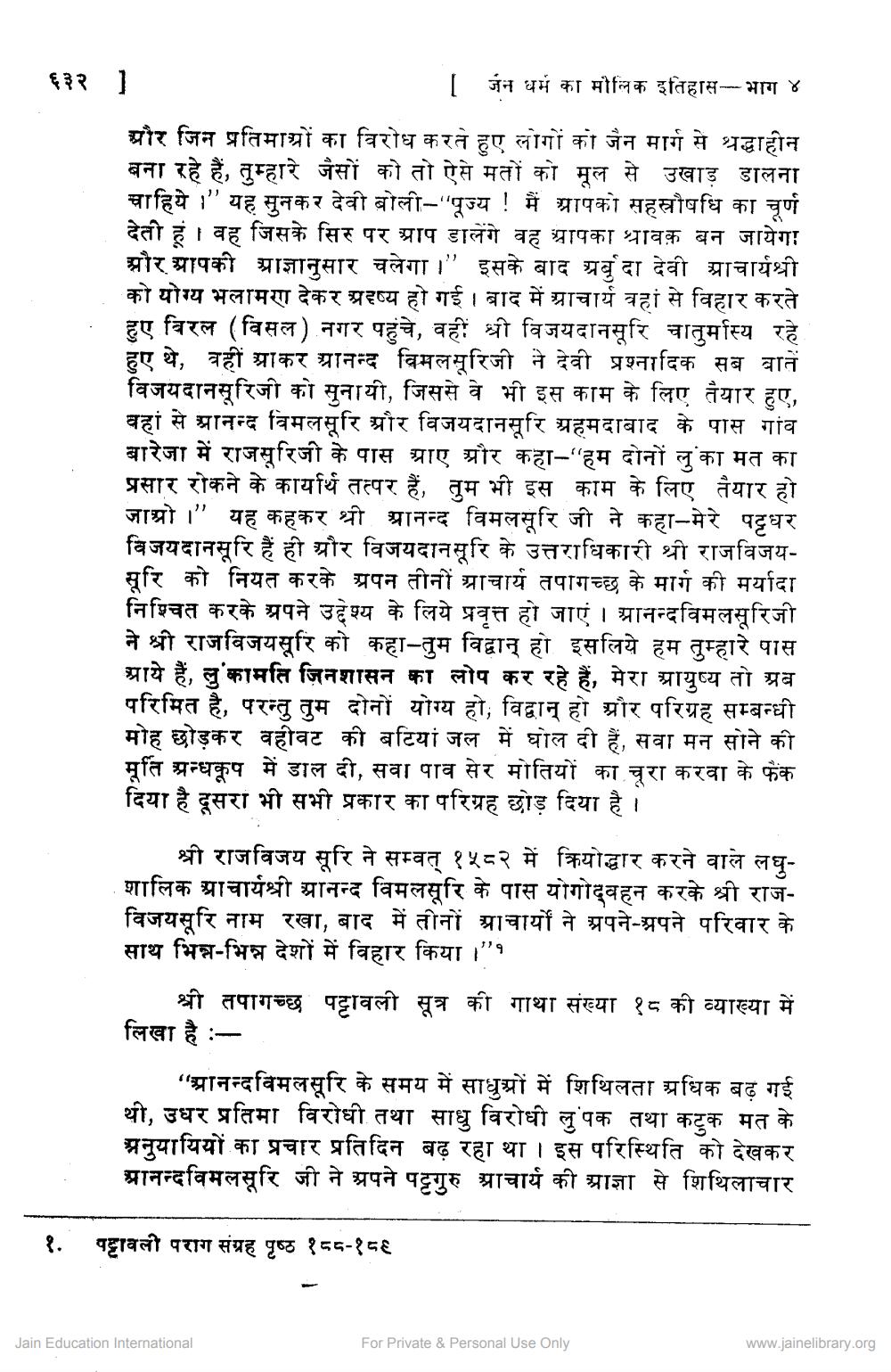________________
६३२ ]
[ जन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ४
और जिन प्रतिमाओं का विरोध करते हुए लोगों को जैन मार्ग से श्रद्धाहीन बना रहे हैं, तुम्हारे जैसों को तो ऐसे मतों को मूल से उखाड़ डालना चाहिये।' यह सुनकर देवी बोली-"पूज्य ! मैं आपको सहस्रौषधि का चूर्ण देती हैं। वह जिसके सिर पर आप डालेंगे वह अापका श्रावक बन जायेगा और आपकी प्राज्ञानुसार चलेगा।' इसके बाद अर्बुदा देवी प्राचार्यश्री को योग्य भलामण देकर अदृष्य हो गई। बाद में प्राचार्य वहां से विहार करते हुए विरल (विसल) नगर पहुंचे, वहीं श्री विजयदानसूरि चातुर्मास्य रहे हुए थे, वहीं पाकर ग्रानन्द विमलमूरिजी ने देवी प्रश्नादिक सब बातें विजयदानसूरिजी को सुनायी, जिससे वे भी इस काम के लिए तैयार हुए, वहां से आनन्द विमलसूरि और विजयदानसूरि अहमदाबाद के पास गांव बारेजा में राजसूरिजी के पास आए और कहा-"हम दोनों लुका मत का प्रसार रोकने के कार्यार्थ तत्पर हैं, तुम भी इस काम के लिए तैयार हो जाओ।" यह कहकर श्री आनन्द विमलसूरि जी ने कहा-मेरे पट्टधर विजयदानसूरि हैं ही और विजयदानसूरि के उत्तराधिकारी श्री राजविजयसूरि को नियत करके अपन तीनों प्राचार्य तपागच्छ के मार्ग की मर्यादा निश्चित करके अपने उद्देश्य के लिये प्रवृत्त हो जाएं । आनन्द विमलसूरिजी ने श्री राजविजयसूरि को कहा-तुम विद्वान् हो इसलिये हम तुम्हारे पास आये हैं, लुकामति जिनशासन का लोप कर रहे हैं, मेरा आयुष्य तो अब परिमित है, परन्तु तुम दोनों योग्य हो, विद्वान् हो और परिग्रह सम्बन्धी मोह छोड़कर वहीवट की बटियां जल में घोल दी हैं, सवा मन सोने की मूर्ति अन्धकूप में डाल दी, सवा पाव सेर मोतियों का चूरा करवा के फैक दिया है दूसरा भी सभी प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है।
श्री राजविजय सूरि ने सम्वत् १५८२ में क्रियोद्धार करने वाले लघुशालिक प्राचार्यश्री आनन्द विमलसूरि के पास योगोद्वहन करके श्री राजविजयसूरि नाम रखा, बाद में तीनों प्राचार्यों ने अपने-अपने परिवार के साथ भिन्न-भिन्न देशों में विहार किया।''
श्री तपागच्छ पट्टावली सूत्र की गाथा संख्या १८ की व्याख्या में लिखा है :
"अानन्दविमलसूरि के समय में साधुनों में शिथिलता अधिक बढ़ गई थी, उधर प्रतिमा विरोधी तथा साधु विरोधी लुपक तथा कटुक मत के अनुयायियों का प्रचार प्रतिदिन बढ़ रहा था। इस परिस्थिति को देखकर प्रानन्दविमलसूरि जी ने अपने पट्टगुरु प्राचार्य की आज्ञा से शिथिलाचार
१. पट्टावली पराग संग्रह पृष्ठ १८८-१८६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org