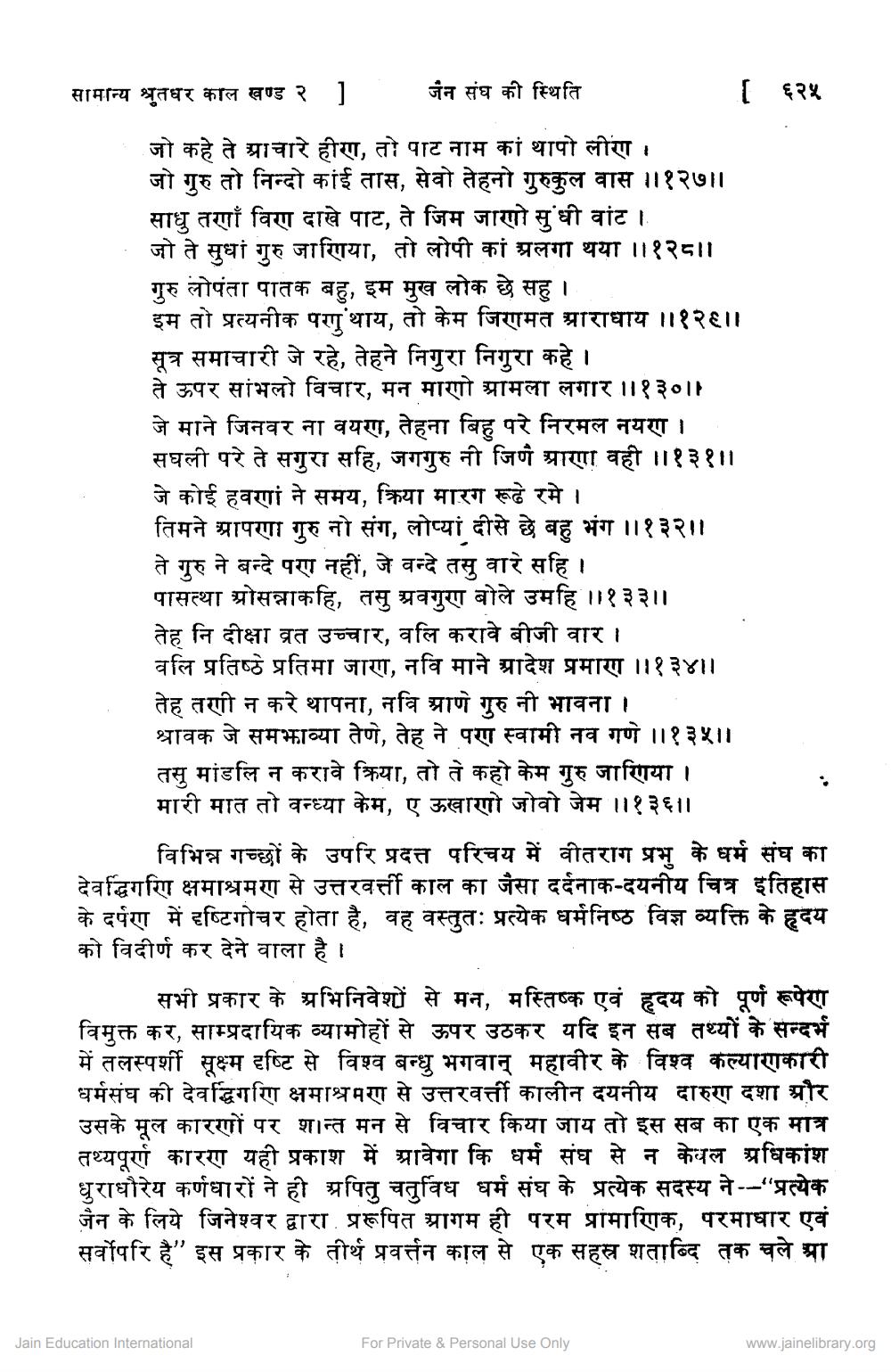________________
सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ]
जैन संघ की स्थिति
६२५
जो कहे ते प्राचारे हीण, तो पाट नाम कां थापो लीण । जो गुरु तो निन्दो कांई तास, सेवो तेहनो गुरुकुल वास ॥१२७।। साधु तणां विण दाखे पाट, ते जिम जाणो सुधी वांट । जो ते सुधां गुरु जाणिया, तो लोपी कां अलगा थया ।।१२८।। गुरु लोपंता पातक बहु, इम मुख लोक छे सहु। इम तो प्रत्यनीक पणु थाय, तो केम जिरणमत प्राराधाय ।।१२६।। सूत्र समाचारी जे रहे, तेहने निगुरा निगुरा कहे। ते ऊपर सांभलो विचार, मन मारणो आमला लगार ।।१३०।। जे माने जिनवर ना वयण, तेहना बिहु परे निरमल नयण । सघली परे ते सगुरा सहि, जगगुरु नी जिणे पारणा वही ।।१३१।। जे कोई हवणां ने समय, क्रिया मारग रूढे रमे । तिमने आपणा गुरु नो संग, लोप्यां दीसे छे बहु भंग ।।१३२।। ते गुरु ने बन्दे पण नहीं, जे वन्दे तसु वारे सहि । पासत्था अोसन्नाकहि, तसु अवगुण बोले उमहि ।।१३३।। तेह नि दीक्षा व्रत उच्चार, वलि करावे बीजी वार । वलि प्रतिष्ठे प्रतिमा जारण, नवि माने आदेश प्रमाण ॥१३४।। तेह तणी न करे थापना, नवि आणे गुरु नी भावना। श्रावक जे समझाव्या तेणे, तेह ने पण स्वामी नव गणे ।।१३५।। तसू मांडलि न करावे क्रिया, तो ते कहो केम गुरु जाणिया । मारी मात तो वन्ध्या केम, ए ऊखाणो जोवो जेम ।।१३६।।
विभिन्न गच्छों के उपरि प्रदत्त परिचय में वीतराग प्रभु के धर्म संघ का देवद्धिगणि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल का जैसा दर्दनाक-दयनीय चित्र इतिहास के दर्पण में दृष्टिगोचर होता है, वह वस्तुतः प्रत्येक धर्मनिष्ठ विज्ञ व्यक्ति के हृदय को विदीर्ण कर देने वाला है ।
सभी प्रकार के अभिनिवेशों से मन, मस्तिष्क एवं हृदय को पूर्ण रूपेण विमुक्त कर, साम्प्रदायिक व्यामोहों से ऊपर उठकर यदि इन सब तथ्यों के सन्दर्भ में तलस्पर्शी सूक्ष्म दृष्टि से विश्व बन्धु भगवान् महावीर के विश्व कल्याणकारी धर्मसंघ की देवद्धिगरिण क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती कालीन दयनीय दारुण दशा और उसके मूल कारणों पर शान्त मन से विचार किया जाय तो इस सब का एक मात्र तथ्यपूर्ण कारण यही प्रकाश में आवेगा कि धर्म संघ से न केवल अधिकांश धुराधौरेय कर्णधारों ने ही अपितु चतुर्विध धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य ने--"प्रत्येक जैन के लिये जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित आगम ही परम प्रामाणिक, परमाधार एवं सर्वोपरि है" इस प्रकार के तीर्थ प्रवर्तन काल से एक सहस्र शताब्दि तक चले पा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org