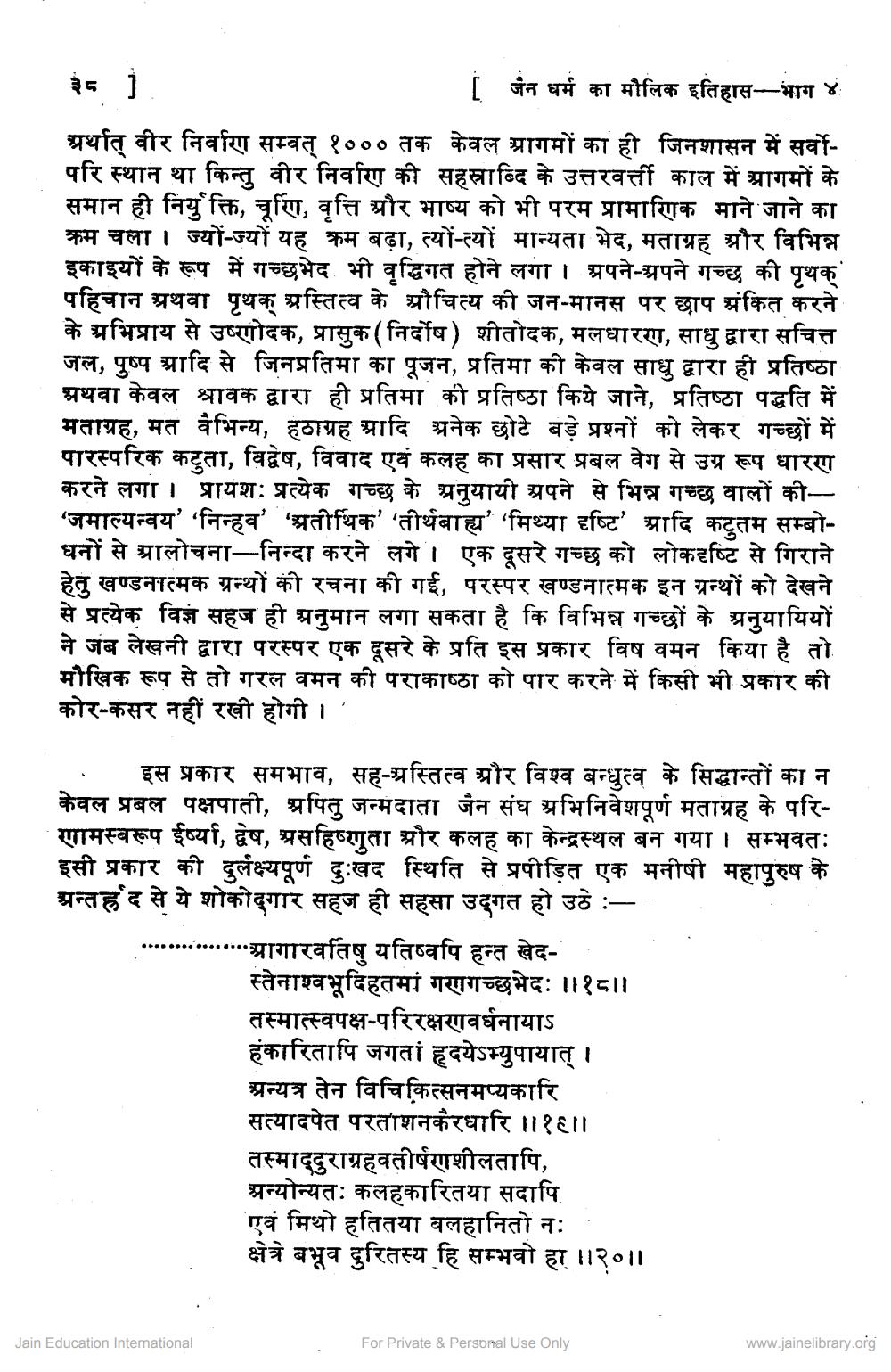________________
३८ ]
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ४
अर्थात् वीर निर्वाण सम्वत् १००० तक केवल आगमों का ही जिनशासन में सर्वोपरि स्थान था किन्तु वीर निर्वाण की सहस्राब्दि के उत्तरवर्ती काल में आगमों के समान ही नियुक्ति, चूणि, वृत्ति और भाष्य को भी परम प्रामाणिक माने जाने का क्रम चला। ज्यों-ज्यों यह क्रम बढ़ा, त्यों-त्यों मान्यता भेद, मताग्रह और विभिन्न इकाइयों के रूप में गच्छभेद भी वृद्धिगत होने लगा। अपने-अपने गच्छ की पृथक् पहिचान अथवा पृथक् अस्तित्व के औचित्य की जन-मानस पर छाप अंकित करने के अभिप्राय से उष्णोदक, प्रासुक (निर्दोष) शीतोदक, मलधारण, साधु द्वारा सचित्त जल, पुष्प आदि से जिनप्रतिमा का पूजन, प्रतिमा की केवल साधु द्वारा ही प्रतिष्ठा अथवा केवल श्रावक द्वारा ही प्रतिमा की प्रतिष्ठा किये जाने, प्रतिष्ठा पद्धति में मताग्रह, मत वैभिन्य, हठाग्रह आदि अनेक छोटे बड़े प्रश्नों को लेकर गच्छों में पारस्परिक कटुता, विद्वेष, विवाद एवं कलह का प्रसार प्रबल वेग से उग्र रूप धारण करने लगा। प्रायशः प्रत्येक गच्छ के अनुयायी अपने से भिन्न गच्छ वालों की'जमाल्यन्वय' 'निन्हव' 'अतीथिक' 'तीर्थबाह्य' 'मिथ्या दृष्टि' आदि कटुतम सम्बोधनों से आलोचना-निन्दा करने लगे। एक दूसरे गच्छ को लोकदृष्टि से गिराने हेतु खण्डनात्मक ग्रन्थों की रचना की गई, परस्पर खण्डनात्मक इन ग्रन्थों को देखने से प्रत्येक विज्ञ सहज ही अनुमान लगा सकता है कि विभिन्न गच्छों के अनुयायियों ने जब लेखनी द्वारा परस्पर एक दूसरे के प्रति इस प्रकार विष वमन किया है तो मौखिक रूप से तो गरल वमन की पराकाष्ठा को पार करने में किसी भी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी होगी।'
. इस प्रकार समभाव, सह-अस्तित्व और विश्व बन्धुत्व के सिद्धान्तों का न केवल प्रबल पक्षपाती, अपितु जन्मदाता जैन संघ अभिनिवेशपूर्ण मताग्रह के परिरणामस्वरूप ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता और कलह का केन्द्रस्थल बन गया। सम्भवतः इसी प्रकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण दुःखद स्थिति से प्रपीड़ित एक मनीषी महापुरुष के अन्तर्हद से ये शोकोद्गार सहज ही सहसा उद्गत हो उठे :
"आगारवर्तिषु यतिष्वपि हन्त खेदस्तेनाश्वभूदिहतमां गणगच्छभेदः ॥१८॥ तस्मात्स्वपक्ष-परिरक्षणवर्धनायाऽ हंकारितापि जगतां हृदयेऽभ्युपायात् । अन्यत्र तेन विचिकित्सनमप्यकारि सत्यादपेत परताशनकैरधारि ॥१६॥ तस्मादुराग्रहवतीर्षणशीलतापि, अन्योन्यतः कलहकारितया सदापि एवं मिथो हतितया बलहा नितो नः क्षेत्रे बभूव दुरितस्य हि सम्भवो हा ।।२०।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.