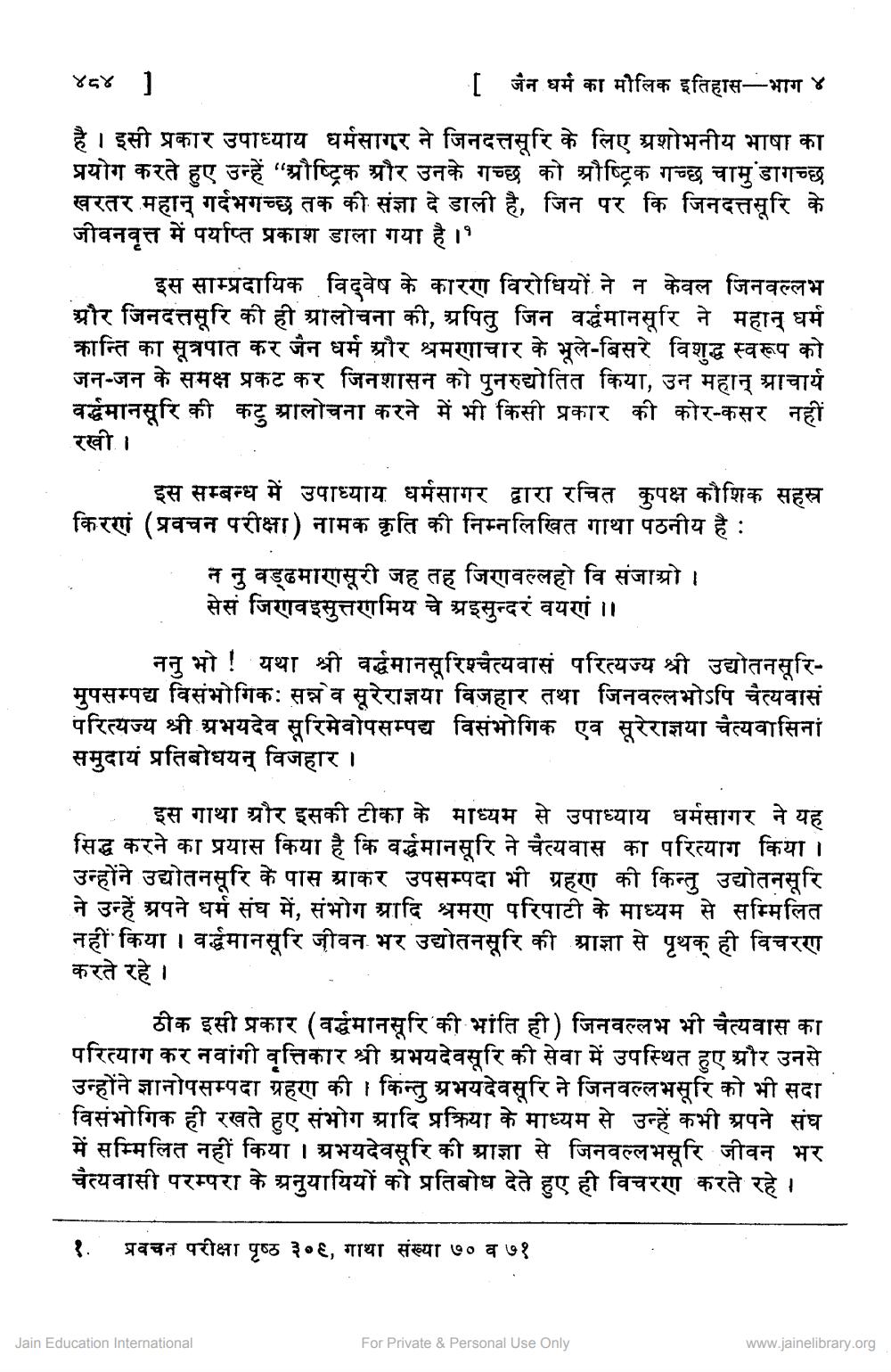________________
४८४ ]
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ४
है। इसी प्रकार उपाध्याय धर्मसागर ने जिनदत्तसूरि के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें "ौष्ट्रिक और उनके गच्छ को औष्ट्रिक गच्छ चामुंडागच्छ खरतर महान् गर्दभगच्छ तक की संज्ञा दे डाली है, जिन पर कि जिनदत्तसूरि के जीवनवृत्त में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।'
इस साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण विरोधियों ने न केवल जिनवल्लभ और जिनदत्तसूरि की ही आलोचना की, अपितु जिन वर्द्धमानसूरि ने महान् धर्म क्रान्ति का सूत्रपात कर जैन धर्म और श्रमणाचार के भूले-बिसरे विशुद्ध स्वरूप को जन-जन के समक्ष प्रकट कर जिनशासन को पुनरुद्योतित किया, उन महान् प्राचार्य वर्द्धमानसूरि की कटु आलोचना करने में भी किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी।
इस सम्बन्ध में उपाध्याय धर्मसागर द्वारा रचित कुपक्ष कौशिक सहस्र किरणं (प्रवचन परीक्षा) नामक कृति की निम्नलिखित गाथा पठनीय है :
न नु वड्ढमाणसूरी जह तह जिणवल्लहो वि संजाओ।
सेसं जिणवइसुत्तणमिय चे अइसुन्दरं वयणं ।।
ननु भो ! यथा श्री वर्द्धमानसूरिश्चैत्यवासं परित्यज्य श्री उद्योतनसूरिमुपसम्पद्य विसंभोगिकः सन्न व सूरेराज्ञया विजहार तथा जिनवल्लभोऽपि चैत्यवासं परित्यज्य श्री अभयदेव सूरिमेवोपसम्पद्य विसंभोगिक एव सूरेराज्ञया चैत्यवासिनां समुदायं प्रतिबोधयन् विजहार ।
__ इस गाथा और इसकी टीका के माध्यम से उपाध्याय धर्मसागर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वर्द्धमानसूरि ने चैत्यवास का परित्याग किया। उन्होंने उद्योतनसूरि के पास आकर उपसम्पदा भी ग्रहण की किन्तु उद्योतनसूरि ने उन्हें अपने धर्म संघ में, संभोग आदि श्रमण परिपाटी के माध्यम से सम्मिलित नहीं किया। वर्द्धमानसूरि जीवन भर उद्योतनसूरि की आज्ञा से पृथक् ही विचरण करते रहे।
ठीक इसी प्रकार (वर्द्धमानसूरि की भांति ही) जिनवल्लभ भी चैत्यवास का परित्याग कर नवांगी वृत्तिकार श्री अभयदेवसूरि की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे उन्होंने ज्ञानोपसम्पदा ग्रहण की। किन्तु अभयदेवसूरि ने जिनवल्लभसूरि को भी सदा विसंभोगिक ही रखते हुए संभोग आदि प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें कभी अपने संघ में सम्मिलित नहीं किया । अभयदेवसूरि की आज्ञा से जिनवल्लभसूरि जीवन भर चैत्यवासी परम्परा के अनुयायियों को प्रतिबोध देते हुए ही विचरण करते रहे ।
१. प्रवचन परीक्षा पृष्ठ ३०६, गाथा संख्या ७० व ७१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org |