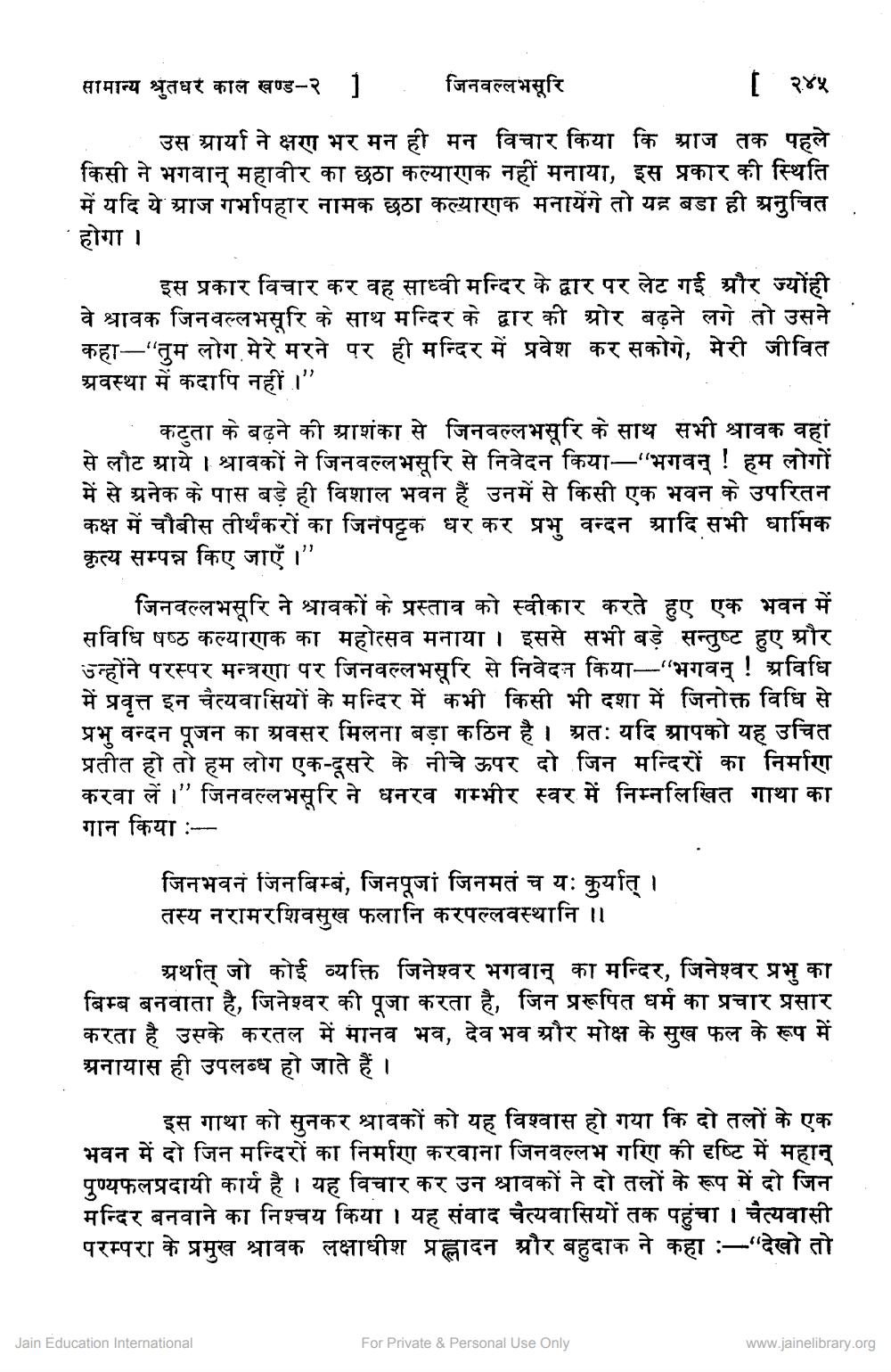________________
सामान्य श्रुतधर काल खण्ड-२ ] जिनवल्लभसूरि
[ २४५ . उस आर्या ने क्षण भर मन ही मन विचार किया कि आज तक पहले किसी ने भगवान् महावीर का छठा कल्याणक नहीं मनाया, इस प्रकार की स्थिति में यदि ये आज गर्भापहार नामक छठा कल्याणक मनायेंगे तो यह बडा ही अनुचित होगा।
इस प्रकार विचार कर वह साध्वी मन्दिर के द्वार पर लेट गई और ज्योंही वे श्रावक जिनवल्लभसूरि के साथ मन्दिर के द्वार की ओर बढ़ने लगे तो उसने कहा-"तुम लोग मेरे मरने पर ही मन्दिर में प्रवेश कर सकोगे, मेरी जीवित अवस्था में कदापि नहीं।"
कटुता के बढ़ने की आशंका से जिनवल्लभसूरि के साथ सभी श्रावक वहां से लौट आये । श्रावकों ने जिनवल्लभसूरि से निवेदन किया-"भगवन् ! हम लोगों में से अनेक के पास बड़े ही विशाल भवन हैं उनमें से किसी एक भवन के उपरितन कक्ष में चौबीस तीर्थंकरों का जिनेपट्टक धर कर प्रभु वन्दन आदि सभी धार्मिक कृत्य सम्पन्न किए जाएँ।"
जिनवल्लभसूरि ने श्रावकों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक भवन में सविधि षष्ठ कल्याणक का महोत्सव मनाया। इससे सभी बड़े सन्तुष्ट हुए और उन्होंने परस्पर मन्त्रणा पर जिनवल्लभसूरि से निवेदन किया-"भगवन् ! अविधि में प्रवृत्त इन चैत्यवासियों के मन्दिर में कभी किसी भी दशा में जिनोक्त विधि से प्रभु वन्दन पूजन का अवसर मिलना बड़ा कठिन है। अत: यदि आपको यह उचित प्रतीत हो तो हम लोग एक-दूसरे के नीचे ऊपर दो जिन मन्दिरों का निर्माण करवा लें।" जिनवल्लभसूरि ने धनरव गम्भीर स्वर में निम्नलिखित गाथा का गान किया :
जिनभवनं जिनबिम्बं, जिनपूजां जिनमतं च यः कुर्यात् । तस्य नरामरशिवसुख फलानि करपल्लवस्थानि ॥
अर्थात् जो कोई व्यक्ति जिनेश्वर भगवान् का मन्दिर, जिनेश्वर प्रभु का बिम्ब बनवाता है, जिनेश्वर की पूजा करता है, जिन प्ररूपित धर्म का प्रचार प्रसार करता है उसके करतल में मानव भव, देव भव और मोक्ष के सुख फल के रूप में अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं ।
इस गाथा को सुनकर श्रावकों को यह विश्वास हो गया कि दो तलों के एक भवन में दो जिन मन्दिरों का निर्माण करवाना जिनवल्लभ गणि की दृष्टि में महान् पुण्यफलप्रदायी कार्य है । यह विचार कर उन श्रावकों ने दो तलों के रूप में दो जिन मन्दिर बनवाने का निश्चय किया। यह संवाद चैत्यवासियों तक पहुंचा । चैत्यवासी परम्परा के प्रमुख श्रावक लक्षाधीश प्रह्लादन और बहुदाक ने कहा :-"देखो तो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org