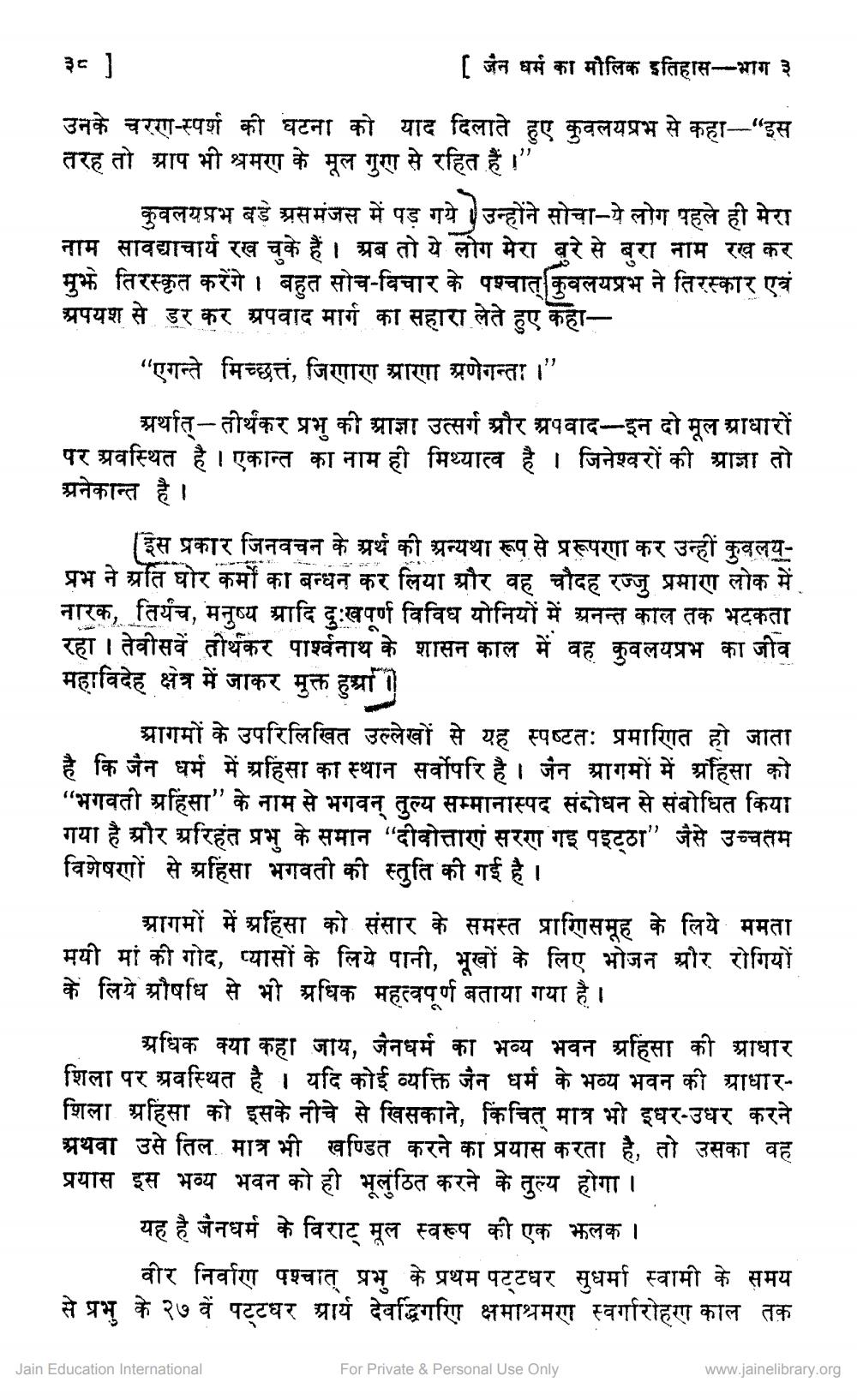________________
३८ ]
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ३ उनके चरण-स्पर्श की घटना को याद दिलाते हुए कुवलयप्रभ से कहा- "इस तरह तो आप भी श्रमण के मूल गुण से रहित हैं !"
कुवलयप्रभ बडे असमंजस में पड़ गये। उन्होंने सोचा-ये लोग पहले ही मेरा नाम सावधाचार्य रख चुके हैं। अब तो ये लोग मेरा बुरे से बुरा नाम रख कर मुझे तिरस्कृत करेंगे। बहुत सोच-विचार के पश्चात् कुवलयप्रभ ने तिरस्कार एवं अपयश से डर कर अपवाद मार्ग का सहारा लेते हुए कहा
“एगन्ते मिच्छत्तं, जिणाण आणा अणेगन्ता।"
अर्थात्-तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा उत्सर्ग और अपवाद-इन दो मूल आधारों पर अवस्थित है। एकान्त का नाम ही मिथ्यात्व है । जिनेश्वरों की आज्ञा तो अनेकान्त है।
(इस प्रकार जिनवचन के अर्थ की अन्यथा रूप से प्ररूपणा कर उन्हीं कुवलयप्रभ ने अति घोर कर्मों का बन्धन कर लिया और वह चौदह रज्जु प्रमाण लोक में नारक, तिर्यंच, मनुष्य आदि दुःखपूर्ण विविध योनियों में अनन्त काल तक भटकता रहा । तेवीसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ के शासन काल में वह कुवलयप्रभ का जीव महाविदेह क्षेत्र में जाकर मुक्त हुआ।
आगमों के उपरिलिखित उल्लेखों से यह स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है कि जैन धर्म में अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है। जैन आगमों में अहिंसा को "भगवती अहिंसा" के नाम से भगवन् तुल्य सम्मानास्पद संबोधन से संबोधित किया गया है और अरिहंत प्रभु के समान “दीवोत्तारणं सरण गइ पइट्ठा" जैसे उच्चतम विशेषणों से अहिंसा भगवती की स्तुति की गई है ।
आगमों में अहिंसा को संसार के समस्त प्राणिसमूह के लिये ममता मयी मां की गोद, प्यासों के लिये पानी, भूखों के लिए भोजन और रोगियों के लिये औषधि से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है।
अधिक क्या कहा जाय, जैनधर्म का भव्य भवन अहिंसा की आधार शिला पर अवस्थित है । यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म के भव्य भवन की अाधारशिला अहिंसा को इसके नीचे से खिसकाने, किंचित् मात्र भो इधर-उधर करने अथवा उसे तिल. मात्र भी खण्डित करने का प्रयास करता है, तो उसका वह प्रयास इस भव्य भवन को ही भूलुंठित करने के तुल्य होगा ।
यह है जैनधर्म के विराट् मूल स्वरूप की एक झलक ।
वीर निर्वाण पश्चात् प्रभु के प्रथम पट्टधर सुधर्मा स्वामी के समय से प्रभु के २७ वें पट्टधर आर्य देवद्भिगणि क्षमाश्रमण स्वर्गारोहण काल तक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org