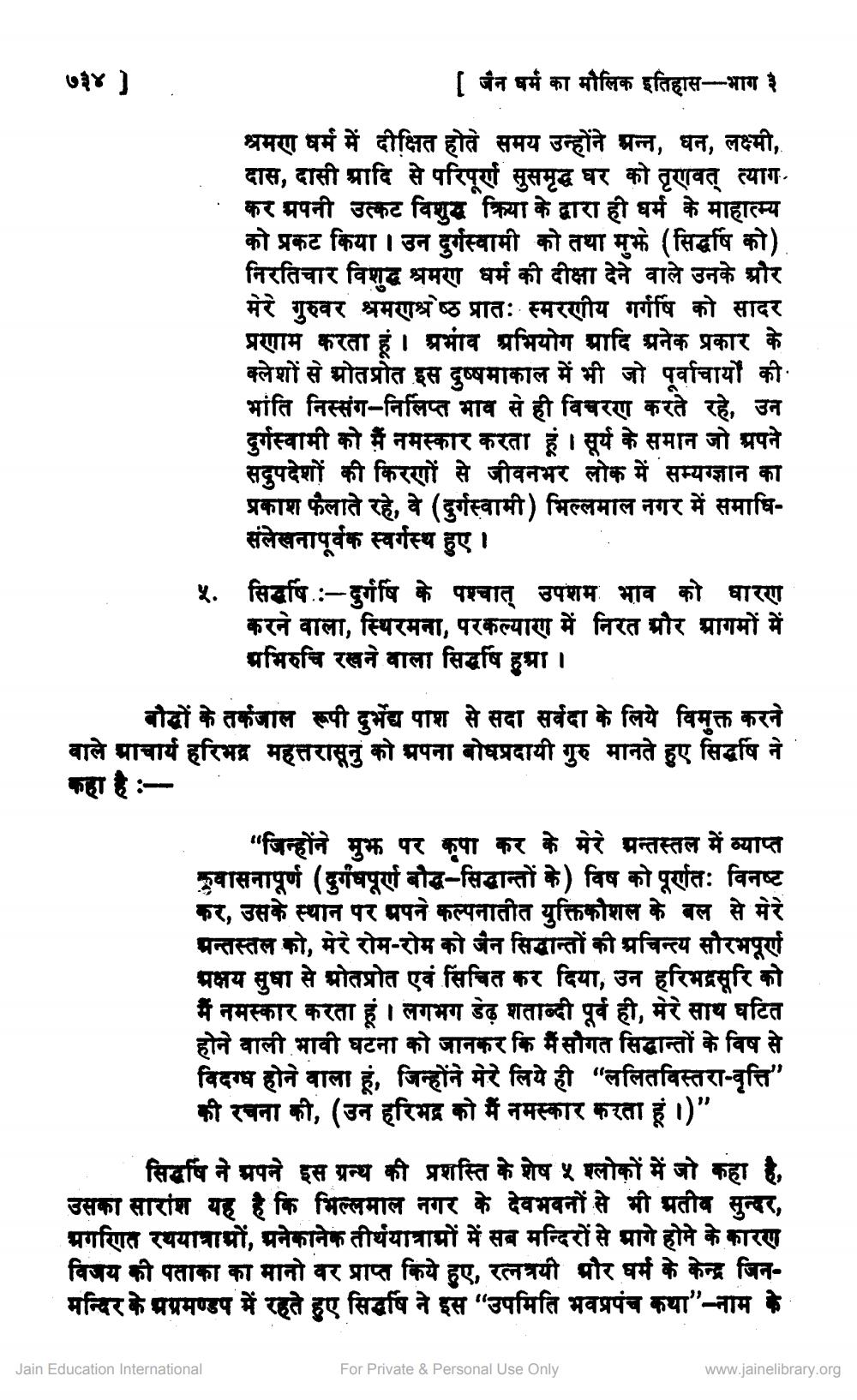________________
७३४)
.
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ३ श्रमण धर्म में दीक्षित होते समय उन्होंने अन्न, धन, लक्ष्मी, दास, दासी प्रादि से परिपूर्ण सुसमृद्ध घर को तृणवत् त्यागकर अपनी उत्कट विशुद्ध क्रिया के द्वारा ही धर्म के माहात्म्य को प्रकट किया। उन दुर्गस्वामी को तथा मुझे (सिद्धर्षि को) निरतिचार विशुद्ध श्रमण धर्म की दीक्षा देने वाले उनके और मेरे गुरुवर श्रमणश्रेष्ठ प्रातः स्मरणीय गर्गर्षि को सादर प्रणाम करता हूं। प्रभाव अभियोग प्रादि अनेक प्रकार के क्लेशों से मोतप्रोत इस दुष्षमाकाल में भी जो पूर्वाचार्यों की भांति निस्संग-निर्लिप्त भाव से ही विचरण करते रहे, उन दुर्गस्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। सूर्य के समान जो अपने सदुपदेशों की किरणों से जीवनभर लोक में सम्यग्ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे, वे (दुर्गस्वामी) भिल्लमाल नगर में समाधि
संलेखनापूर्वक स्वर्गस्थ हुए। ५. सिद्धर्षि:-दुर्गर्षि के पश्चात् उपशम भाव को धारण
करने वाला, स्थिरमना, परकल्याण में निरत और पागमों में अभिरुचि रखने वाला सिद्धर्ष हुमा।
बौदों के तर्कजाल रूपी दुर्भद्य पाश से सदा सर्वदा के लिये विमुक्त करने वाले प्राचार्य हरिभद्र महत्तरासूनु को अपना बोषप्रदायी गुरु मानते हुए सिद्धर्षि ने
"जिन्होंने मुझ पर कृपा कर के मेरे अन्तस्तल में व्याप्त कुवासनापूर्ण (दुर्गंधपूर्ण बौद्ध-सिद्धान्तों के) विष को पूर्णतः विनष्ट कर, उसके स्थान पर अपने कल्पनातीत युक्तिकौशल के बल से मेरे अन्तस्तल को, मेरे रोम-रोम को जैन सिद्धान्तों की अचिन्त्य सौरभपूर्ण प्रक्षय सुधा से प्रोतप्रोत एवं सिंचित कर दिया, उन हरिभद्रसरि को मैं नमस्कार करता हूं। लगभग डेढ़ शताब्दी पूर्व ही, मेरे साथ घटित होने वाली भावी घटना को जानकर कि मैं सौगत सिद्धान्तों के विष से विदग्ध होने वाला हूं, जिन्होंने मेरे लिये ही "ललितविस्तरा-वृत्ति"
की रचना की, (उन हरिभद्र को मैं नमस्कार करता हूं।)" सिद्धपि ने अपने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति के शेष ५ श्लोकों में जो कहा है, उसका सारांश यह है कि भिल्लमाल नगर के देवभवनों से भी प्रतीव सुन्दर, अगणित रथयात्रामों, अनेकानेक तीर्थयात्रामों में सब मन्दिरों से मागे होने के कारण विजय की पताका का मानो वर प्राप्त किये हुए, रत्नत्रयी पौर धर्म के केन्द्र जिनमन्दिर के प्रामण्डप में रहते हुए सिद्धर्षि ने इस "उपमिति भवप्रपंच कथा"-नाम के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org