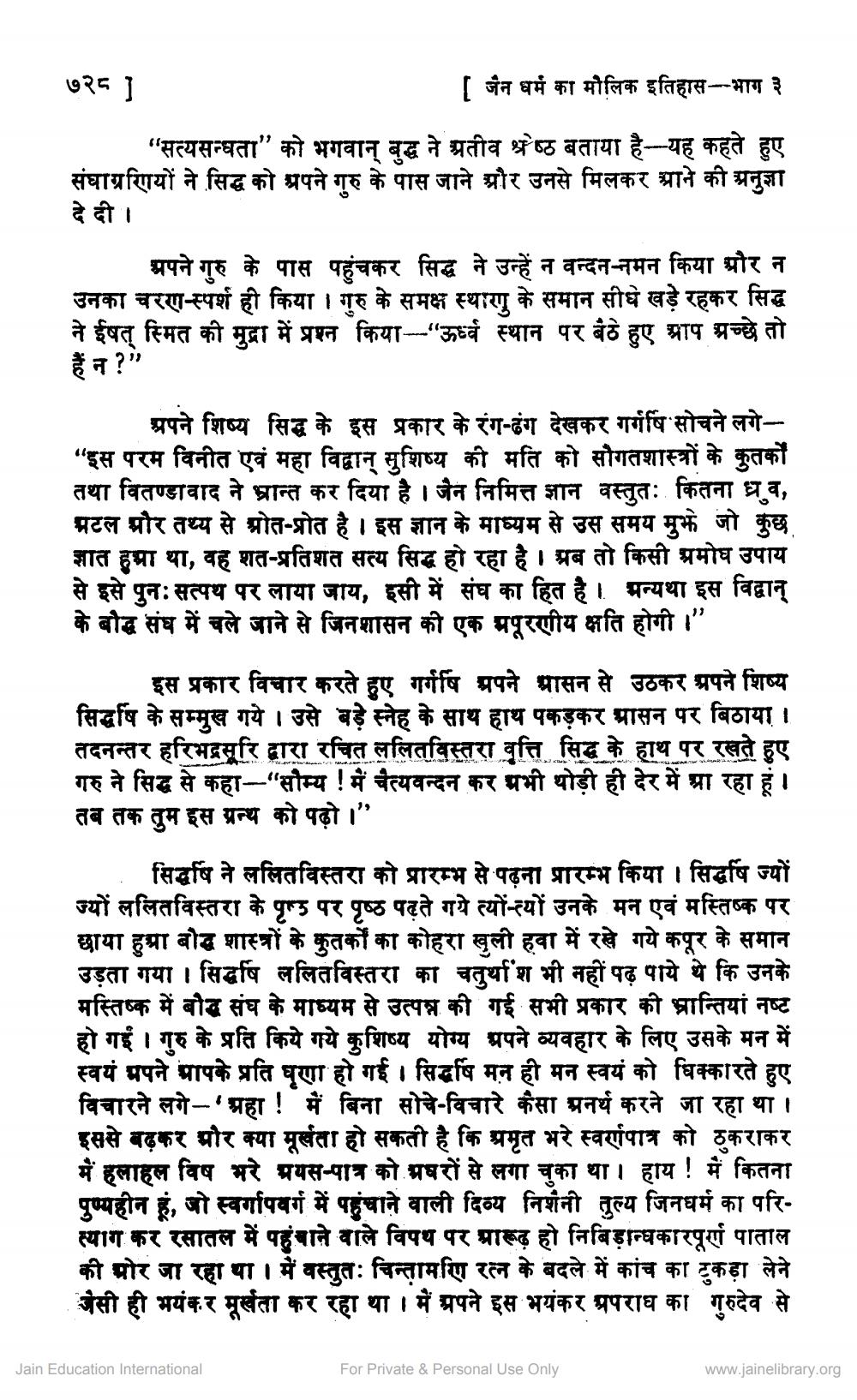________________
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास - भाग ३
"सत्यसन्धता” को भगवान् बुद्ध ने प्रतीव श्रेष्ठ बताया है - यह कहते हुए संघारियों ने सिद्ध को अपने गुरु के पास जाने और उनसे मिलकर आने की अनुज्ञा दे दी ।
७२८]
अपने गुरु के पास पहुंचकर सिद्ध ने उन्हें न उनका चरण-स्पर्श ही किया । गुरु के समक्ष स्थारणु के ने ईषत् स्मित की मुद्रा में प्रश्न किया- "ऊर्ध्व स्थान हैं न ?
वन्दन - नमन किया और न समान सीधे खड़े रहकर सिद्ध पर बैठे हुए आप अच्छे तो
अपने शिष्य सिद्ध के इस प्रकार के रंग-ढंग देखकर गर्गर्षि सोचने लगे"इस परम विनीत एवं महा विद्वान् सुशिष्य की मति को सौगतशास्त्रों के कुतक तथा वितण्डावाद ने भ्रान्त कर दिया है। जैन निमित्त ज्ञान वस्तुतः कितना ध्रुव, अटल और तथ्य से श्रोत-प्रोत है । इस ज्ञान के माध्यम से उस समय मुझे जो कुछ ज्ञात हुआ था, वह शत-प्रतिशत सत्य सिद्ध हो रहा है। अब तो किसी प्रमोघ उपाय से इसे पुनः सत्पथ पर लाया जाय, इसी में संघ का हित है । अन्यथा इस विद्वान् के बौद्ध संघ में चले जाने से जिनशासन की एक प्रपूरणीय क्षति होगी ।"
I
इस प्रकार विचार करते हुए गर्गषि अपने श्रासन से उठकर अपने शिष्य सिद्धषि के सम्मुख गये । उसे बड़े स्नेह के साथ हाथ पकड़कर प्रासन पर बिठाया । तदनन्तर हरिभद्रसूरि द्वारा रचित ललितविस्तरा वृत्ति सिद्ध के हाथ पर रखते हुए गरु ने सिद्ध से कहा - "सौम्य ! मैं चेत्यवन्दन कर अभी थोड़ी ही देर में श्रा रहा हूं । तब तक तुम इस ग्रन्थ को पढ़ो ।”
सिद्धर्षि ने ललितविस्तरा को प्रारम्भ से पढ़ना प्रारम्भ किया । सिद्धर्षि ज्यों ज्यों ललितविस्तरा के पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते गये त्यों-त्यों उनके मन एवं मस्तिष्क पर छाया हुआ बौद्ध शास्त्रों के कुतर्कों का कोहरा खुली हवा में रखे गये कपूर के समान उड़ता गया । सिद्धर्षि ललितविस्तरा का चतुर्थांश भी नहीं पढ़ पाये थे कि उनके मस्तिष्क में बौद्ध संघ के माध्यम से उत्पन्न की गई सभी प्रकार की भ्रान्तियां नष्ट हो गईं। गुरु के प्रति किये गये कुशिष्य योग्य अपने व्यवहार के लिए उसके मन में स्वयं अपने प्रापके प्रति घृणा हो गई । सिद्धर्षि मन ही मन स्वयं को धिक्कारते हुए विचारने लगे - ' अहा ! मैं बिना सोचे-विचारे कैसा अनर्थ करने जा रहा था । इससे बढ़कर और क्या मूर्खता हो सकती है कि अमृत भरे स्वर्णपात्र को ठुकराकर मैं हलाहल विष भरे प्रयस पात्र को अघरों से लगा चुका था । हाय ! मैं कितना पुष्यहीन हूं, जो स्वर्गापवर्ग में पहुंचाने वाली दिव्य निर्शनी तुल्य जिनधर्म का परित्याग कर रसातल में पहुंचाने वाले विपथ पर प्रारूढ़ हो निबिहान्धकारपूर्ण पाताल की प्रोर जा रहा था। मैं वस्तुतः चिन्तामणि रत्न के बदले में कांच का टुकड़ा लेने जैसी ही भयंकर मूर्खता कर रहा था । मैं अपने इस भयंकर अपराध का गुरुदेव से
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org