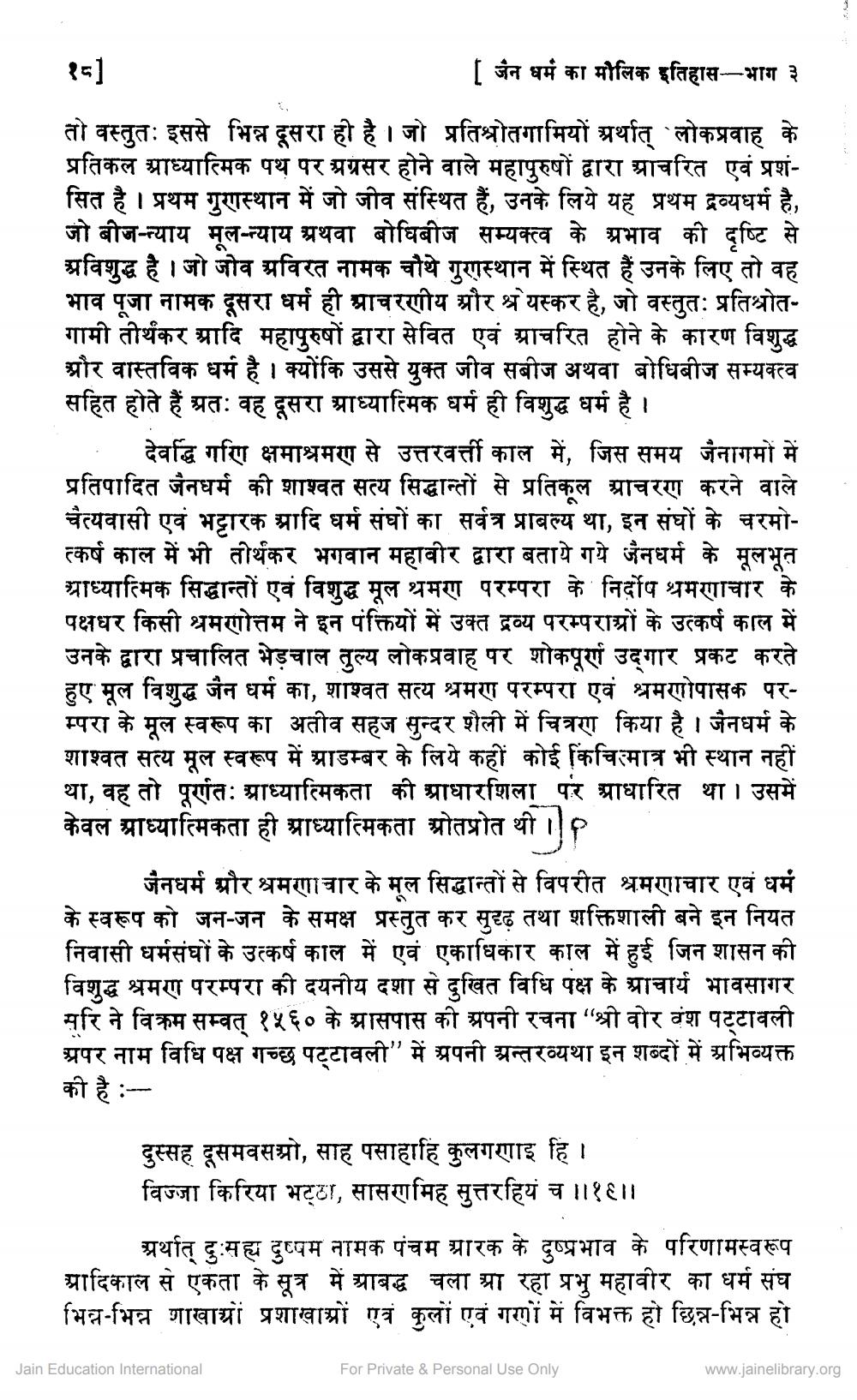________________
१८]
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ३ तो वस्तुतः इससे भिन्न दूसरा ही है । जो प्रतिश्रोतगामियों अर्थात् लोकप्रवाह के प्रतिकल आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाले महापुरुषों द्वारा आचरित एवं प्रशंसित है । प्रथम गुणस्थान में जो जीव संस्थित हैं, उनके लिये यह प्रथम द्रव्यधर्म है, जो बीज-न्याय मूल-न्याय अथवा बोधिबीज सम्यक्त्व के अभाव की दृष्टि से अविशुद्ध है । जो जोव अविरत नामक चौथे गुरणस्थान में स्थित हैं उनके लिए तो वह भाव पूजा नामक दूसरा धर्म ही आचरणीय और श्रेयस्कर है, जो वस्तुतः प्रतिश्रोतगामी तीर्थंकर आदि महापुरुषों द्वारा सेवित एवं आचरित होने के कारण विशुद्ध और वास्तविक धर्म है। क्योंकि उससे युक्त जीव सबीज अथवा बोधिबीज सम्यक्त्व सहित होते हैं अतः वह दूसरा आध्यात्मिक धर्म ही विशुद्ध धर्म है।
. देवद्धि गणि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती काल में, जिस समय जैनागमों में प्रतिपादित जैनधर्म की शाश्वत सत्य सिद्धान्तों से प्रतिकुल आचरण करने वाले चैत्यवासी एवं भट्टारक आदि धर्म संघों का सर्वत्र प्राबल्य था, इन संघों के चरमोत्कर्ष काल में भी तीर्थकर भगवान महावीर द्वारा बताये गये जैनधर्म के मूलभूत याध्यात्मिक सिद्धान्तों एवं विशुद्ध मूल श्रमरण परम्परा के निर्दोष श्रमरणाचार के पक्षधर किसी श्रमरणोत्तम ने इन पंक्तियों में उक्त द्रव्य परम्पराओं के उत्कर्ष काल में उनके द्वारा प्रचालित भेड़चाल तुल्य लोकप्रवाह पर शोकपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए मूल विशुद्ध जैन धर्म का, शाश्वत सत्य श्रमण परम्परा एवं श्रमणोपासक परम्परा के मूल स्वरूप का अतीव सहज सून्दर शैली में चित्रण किया है। जैनधर्म के शाश्वत सत्य मूल स्वरूप में आडम्बर के लिये कहीं कोई किचित्मात्र भी स्थान नहीं था, वह तो पूर्णतः आध्यात्मिकता की आधारशिला पर आधारित था। उसमें केवल आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिकता ओतप्रोत थी।
जैनधर्म और श्रमणाचार के मूल सिद्धान्तों से विपरीत श्रमणाचार एवं धर्म के स्वरूप को जन-जन के समक्ष प्रस्तुत कर सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बने इन नियत निवासी धर्मसंघों के उत्कर्ष काल में एवं एकाधिकार काल में हुई जिन शासन की विशुद्ध श्रमण परम्परा की दयनीय दशा से दुखित विधि पक्ष के प्राचार्य भावसागर सरि ने विक्रम सम्वत् १५६० के आसपास की अपनी रचना "श्री वोर वंश पट्टावली अपर नाम विधि पक्ष गच्छ पट्टावली'' में अपनी अन्तरव्यथा इन शब्दों में अभिव्यक्त की है :
दुस्सह दूसमवसनो, साह पसाहाहि कुलगणाइ हिं। विज्जा किरिया भट्टा, सासरणमिह सुत्तरहियं च ।।१६।।
अर्थात् दुःसह्य दुष्पम नामक पंचम प्रारक के दुष्प्रभाव के परिणामस्वरूप आदिकाल से एकता के सूत्र में आबद्ध चला आ रहा प्रभु महावीर का धर्म संघ भिन्न-भिन्न शाखायों प्रशाखाओं एवं कुलों एवं गणों में विभक्त हो छिन्न-भिन्न हो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org