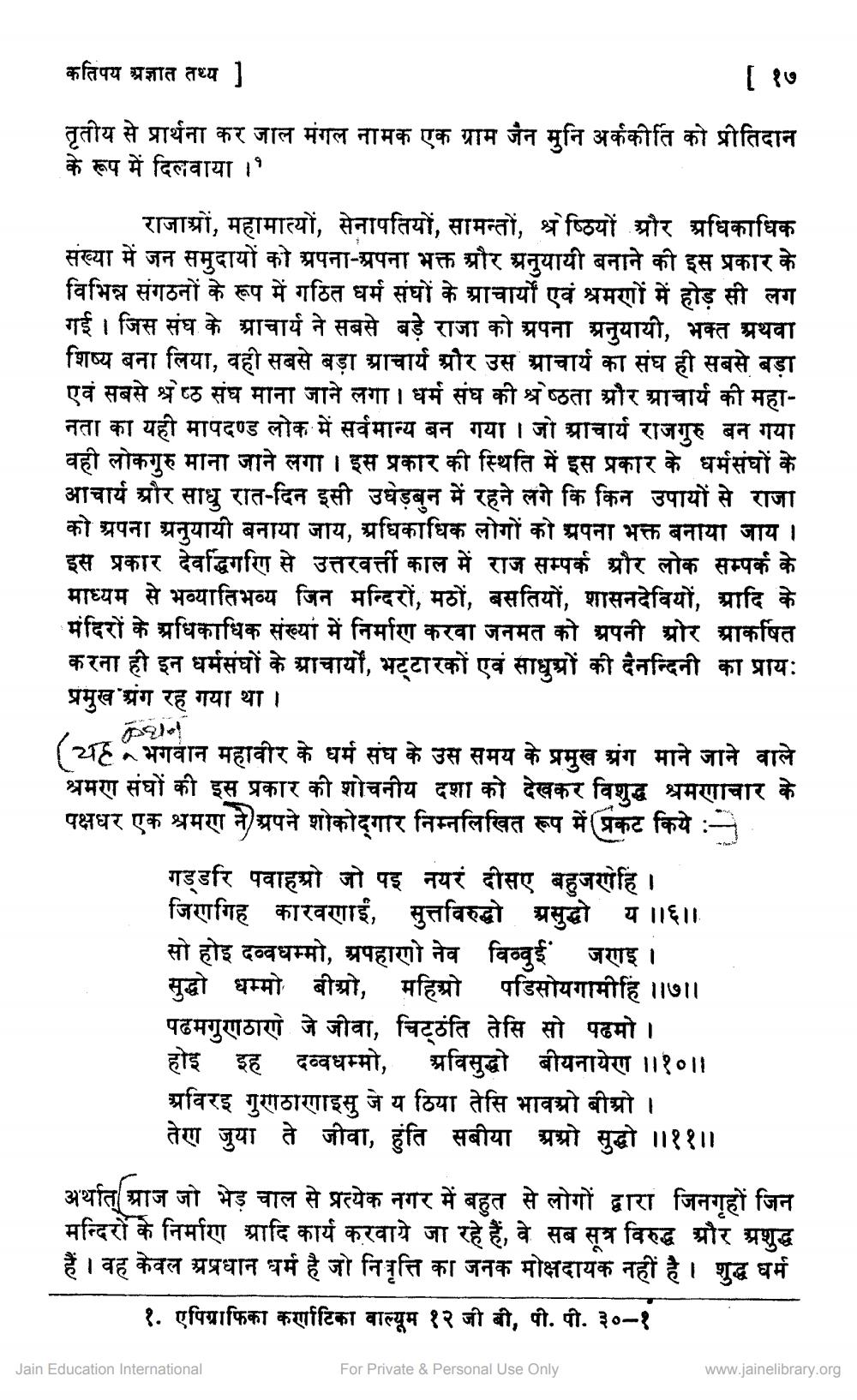________________
कतिपय अज्ञात तथ्य ]
[ १७
तृतीय से प्रार्थना कर जाल मंगल नामक एक ग्राम जैन मुनि अर्ककीर्ति को प्रीतिदान के रूप में दिलवाया । '
राजाओं, महामात्यों, सेनापतियों, सामन्तों, श्रेष्ठियों और अधिकाधिक संख्या में जन समुदायों को अपना-अपना भक्त और अनुयायी बनाने की इस प्रकार के विभिन्न संगठनों के रूप में गठित धर्म संघों के प्राचार्यों एवं श्रमरणों में होड़ सी लग गई । जिस संघ के आचार्य ने सबसे बड़े राजा को अपना अनुयायी, भक्त अथवा शिष्य बना लिया, वही सबसे बड़ा प्राचार्य और उस प्राचार्य का संघ ही सबसे बड़ा एवं सबसे श्रेष्ठ संघ माना जाने लगा। धर्म संघ की श्रेष्ठता और आचार्य की महानता का यही मापदण्ड लोक में सर्वमान्य बन गया । जो आचार्य राजगुरु बन गया
ही लोकगुरु माना जाने लगा। इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार के धर्मसंघों के आचार्य और साधु रात-दिन इसी उधेड़बुन में रहने लगे कि किन उपायों से राजा को अपना अनुयायी बनाया जाय, अधिकाधिक लोगों को अपना भक्त बनाया जाय । इस प्रकार देवगिरिण से उत्तरवर्ती काल में राज सम्पर्क और लोक सम्पर्क के माध्यम से भव्यातिभव्य जिन मन्दिरों, मठों, बसतियों, शासनदेवियों, आदि के मंदिरों के अधिकाधिक संख्या में निर्माण करवा जनमत को अपनी ओर आकर्षित करना ही इन धर्मसंघों के आचार्यो, भट्टारकों एवं साधुत्रों की दैनन्दिनी का प्रायः प्रमुख अंग रह गया था ।
कथन
A
( यह भगवान महावीर के धर्म संघ के उस समय के प्रमुख अंग माने जाने वाले श्रमण संघों की इस प्रकार की शोचनीय दशा को देखकर विशुद्ध श्रमणाचार के पक्षधर एक श्रमरण ने/अपने शोकोद्गार निम्नलिखित रूप में प्रकट किये : -
गड्डरि पवाहम्रो जो पइ नयरं दीसए बहुजणेहिं । जिगहि कारवरगाईं, सुत्तविरुद्धो प्रसुद्धो य ॥ ६ ॥ सो होइ दव्वधम्मो, अपहारगो नेव विव्वुई जगइ । सुद्धो धम्मो बीग्रो, महिश्रो पडिसोयगामीहि ||७|| पढमगुणठाणे जे जीवा, चिट्ठति तेसि सो पढमो । होइ इह दव्वधम्मो, अविसुद्ध बीयनायेण || १० || अविर गुरगठारगासु जे य ठिया तेसि भावप्रो बीओो । तेरण जुया ते जीवा, हुंति सबीया अनो सुद्धो ॥११॥
अर्थात् आज जो भेड़ चाल से प्रत्येक नगर में बहुत से लोगों द्वारा जिनगृहों जिन मन्दिरों के निर्माण आदि कार्य करवाये जा रहे हैं, वे सब सूत्र विरुद्ध और अशुद्ध हैं। वह केवल अप्रधान धर्म है जो निवृत्ति का जनक मोक्षदायक नहीं है । शुद्ध धर्म
१. एपिग्राफिका कर्णाटिका वाल्यूम १२ जीबी, पी. पी. ३०-१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org