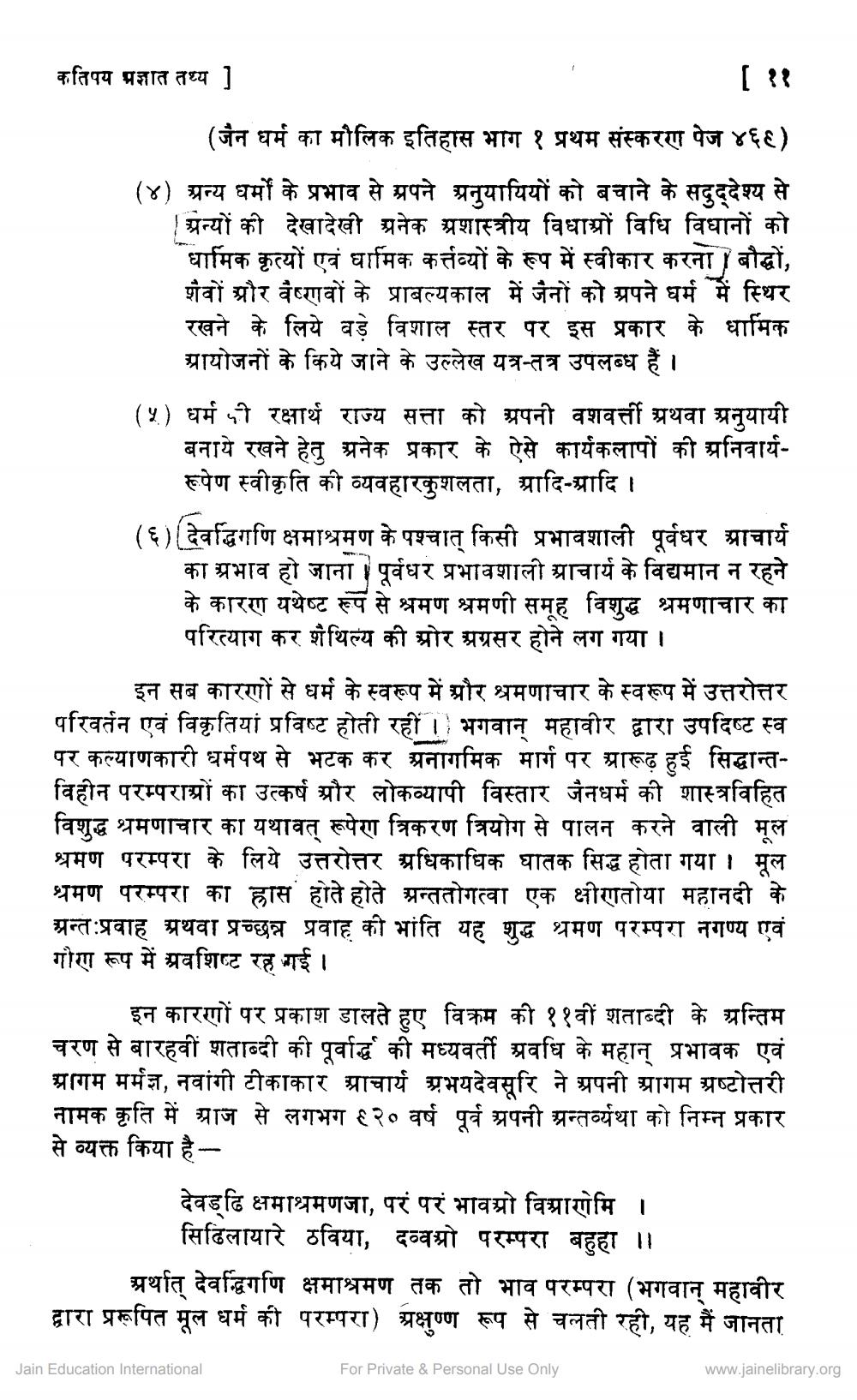________________
कतिपय प्रज्ञात तथ्य ]
[ ११ (जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग १ प्रथम संस्करण पेज ४६६) (४) अन्य धर्मों के प्रभाव से अपने अनुयायियों को बचाने के सदुद्देश्य से
अन्यों की देखादेखी अनेक अशास्त्रीय विधाओं विधि विधानों को धार्मिक कृत्यों एवं धार्मिक कर्तव्यों के रूप में स्वीकार करना। बौद्धों, शैवों और वैष्णवों के प्राबल्यकाल में जैनों को अपने धर्म में स्थिर रखने के लिये बड़े विशाल स्तर पर इस प्रकार के धार्मिक
प्रायोजनों के किये जाने के उल्लेख यत्र-तत्र उपलब्ध हैं। (५) धर्म की रक्षार्थ राज्य सत्ता को अपनी वशवर्ती अथवा अनुयायी
बनाये रखने हेतु अनेक प्रकार के ऐसे कार्यकलापों की अनिवार्य
रूपेण स्वीकृति की व्यवहारकुशलता, आदि-आदि। (६) (देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के पश्चात् किसी प्रभावशाली पूर्वधर आचार्य
का अभाव हो जाना। पूर्वधर प्रभावशाली प्राचार्य के विद्यमान न रहने के कारण यथेष्ट रूप से श्रमण श्रमणी समूह विशुद्ध श्रमणाचार का
परित्याग कर शैथिल्य की ओर अग्रसर होने लग गया। इन सब कारणों से धर्म के स्वरूप में और श्रमणाचार के स्वरूप में उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं विकृतियां प्रविष्ट होती रहीं। भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट स्व पर कल्याणकारी धर्मपथ से भटक कर अनागमिक मार्ग पर आरूढ़ हुई सिद्धान्तविहीन परम्पराओं का उत्कर्ष और लोकव्यापी विस्तार जैनधर्म की शास्त्रविहित विशुद्ध श्रमणाचार का यथावत् रूपेण त्रिकरण त्रियोग से पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा के लिये उत्तरोत्तर अधिकाधिक घातक सिद्ध होता गया। मूल श्रमण परम्परा का ह्रास होते होते अन्ततोगत्वा एक क्षीणतोया महानदी के अन्तःप्रवाह अथवा प्रच्छन्न प्रवाह की भांति यह शुद्ध श्रमण परम्परा नगण्य एवं गौरण रूप में अवशिष्ट रह गई।
इन कारणों पर प्रकाश डालते हुए विक्रम की ११वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से बारहवीं शताब्दी की पूर्वार्द्ध की मध्यवर्ती अवधि के महान प्रभावक एवं प्रागम मर्मज्ञ, नवांगी टीकाकार आचार्य अभयदेवसूरि ने अपनी आगम अष्टोत्तरी नामक कृति में आज से लगभग ६२० वर्ष पूर्व अपनी अन्तर्व्यथा को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है
देवढि क्षमाश्रमणजा, परं परं भावो विप्राणेमि ।
सिढिलायारे ठविया, दव्वो परम्परा बहुहा ।। अर्थात् देवद्धिगणि क्षमाश्रमण तक तो भाव परम्परा (भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित मूल धर्म की परम्परा) अक्षुण्ण रूप से चलती रही, यह मैं जानता
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org