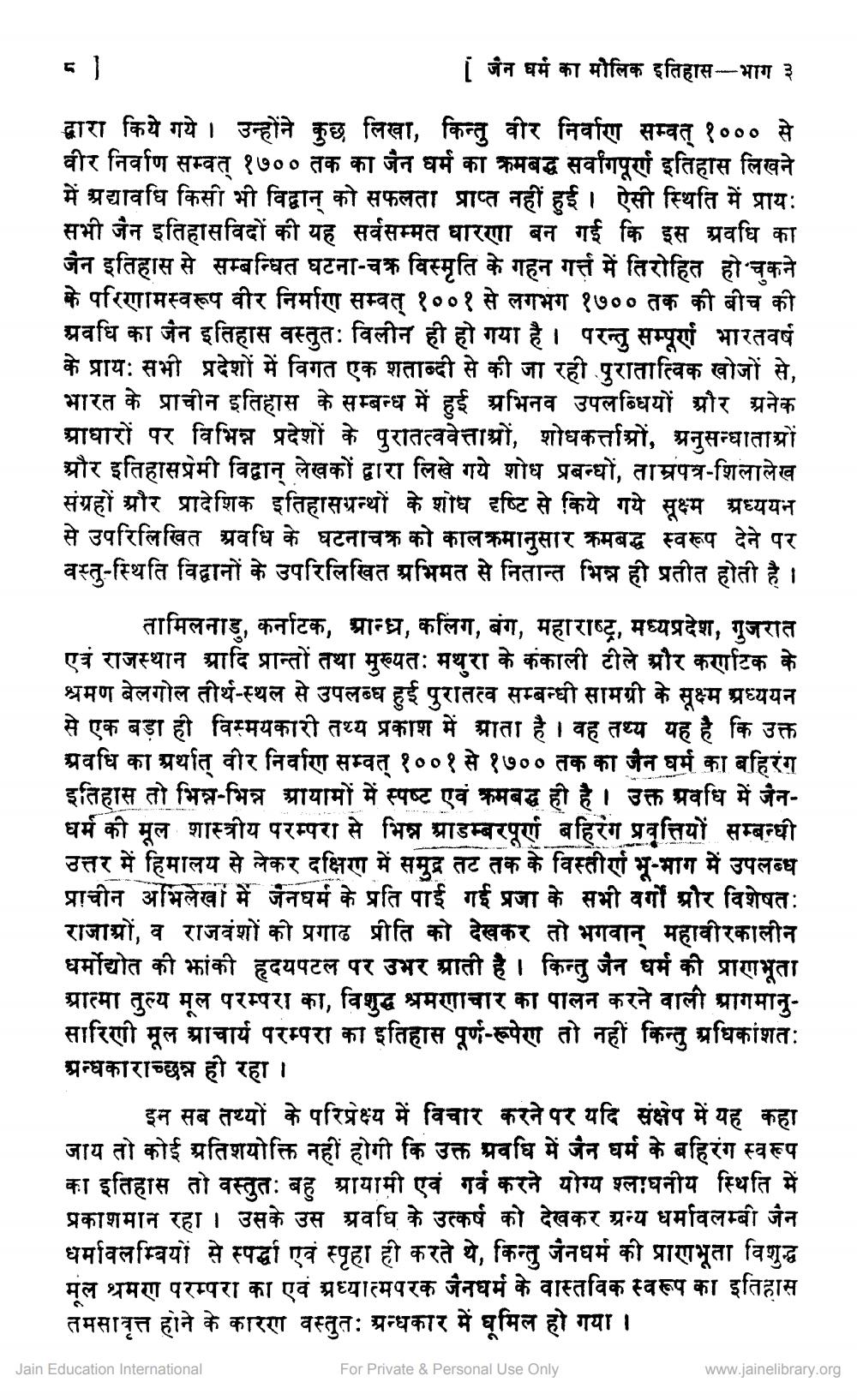________________
८]
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास - भाग ३
द्वारा किये गये । उन्होंने कुछ लिखा, किन्तु वीर निर्वारण सम्वत् १००० से वीर निर्वाण सम्वत् १७०० तक का जैन धर्म का क्रमबद्ध सर्वांगपूर्ण इतिहास लिखने में अद्यावधि किसी भी विद्वान् को सफलता प्राप्त नहीं हुई । ऐसी स्थिति में प्राय: सभी जैन इतिहासविदों की यह सर्वसम्मत धारणा बन गई कि इस अवधि का जैन इतिहास से सम्बन्धित घटना चक्र विस्मृति के गहन गर्त में तिरोहित हो चुकने के परिणामस्वरूप वीर निर्माण सम्वत् १००१ से लगभग १७०० तक की बीच की अवधि का जैन इतिहास वस्तुतः विलीन ही हो गया है । परन्तु सम्पूर्ण भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रदेशों में विगत एक शताब्दी से की जा रही पुरातात्विक खोजों से, भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में हुई अभिनव उपलब्धियों और अनेक आधारों पर विभिन्न प्रदेशों के पुरातत्ववेत्ताओं, शोधकर्त्तानों, अनुसन्धाताओं और इतिहासप्रेमी विद्वान् लेखकों द्वारा लिखे गये शोध प्रबन्धों, ताम्रपत्र - शिलालेख संग्रहों और प्रादेशिक इतिहास ग्रन्थों के शोध दृष्टि से किये गये सूक्ष्म अध्ययन से उपरिलिखित अवधि के घटनाचक्र को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध स्वरूप देने पर वस्तुस्थिति विद्वानों के उपरिलिखित प्रभिमत से नितान्त भिन्न ही प्रतीत होती है ।
तामिलनाडु, कर्नाटक, प्रान्ध्र, कलिंग, बंग, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान आदि प्रान्तों तथा मुख्यतः मथुरा के कंकाली टीले और करर्णाटक के श्रमण बेलगोल तीर्थ-स्थल से उपलब्ध हुई पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री के सूक्ष्म अध्ययन से एक बड़ा ही विस्मयकारी तथ्य प्रकाश में आता है । वह तथ्य यह है कि उक्त अवधि का अर्थात् वीर निर्वारण सम्वत् १००१ से १७०० तक का जैन धर्म का बहिरंग इतिहास तो भिन्न-भिन्न आयामों में स्पष्ट एवं क्रमबद्ध ही है । उक्त अवधि में जैनधर्म की मूल शास्त्रीय परम्परा से भिन्न प्राडम्बरपूर्ण बहिरंग प्रवृत्तियों सम्बन्धी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक के विस्तीर्ण भू-भाग में उपलब्ध प्राचीन अभिलेखों में जैनधर्म के प्रति पाई गई प्रजा के सभी वर्गों और विशेषत: राजानों, व राजवंशों की प्रगाढ प्रीति को देखकर तो भगवान् महावीरकालीन धर्मोद्योत की झांकी हृदयपटल पर उभर आती है। किन्तु जैन धर्म की प्राणभूता आत्मा तुल्य मूल परम्परा का, विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली श्रागमानुसारिणी मूल प्राचार्य परम्परा का इतिहास पूर्ण रूपेण तो नहीं किन्तु अधिकांशतः अन्धकाराच्छन्न ही रहा ।
इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यदि संक्षेप में यह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उक्त अवधि में जैन धर्म के बहिरंग स्वरूप का इतिहास तो वस्तुतः बहु आयामी एवं गर्व करने योग्य श्लाघनीय स्थिति में प्रकाशमान रहा। उसके उस अवधि के उत्कर्ष को देखकर अन्य धर्मावलम्बी जैन धर्मावलम्बियों से स्पर्द्धा एवं स्पृहा ही करते थे, किन्तु जैनधर्म की प्रारणभूता विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा का एवं अध्यात्मपरक जैनधर्म के वास्तविक स्वरूप का इतिहास तमसावृत्त होने के कारण वस्तुतः अन्धकार में घूमिल हो गया ।
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org