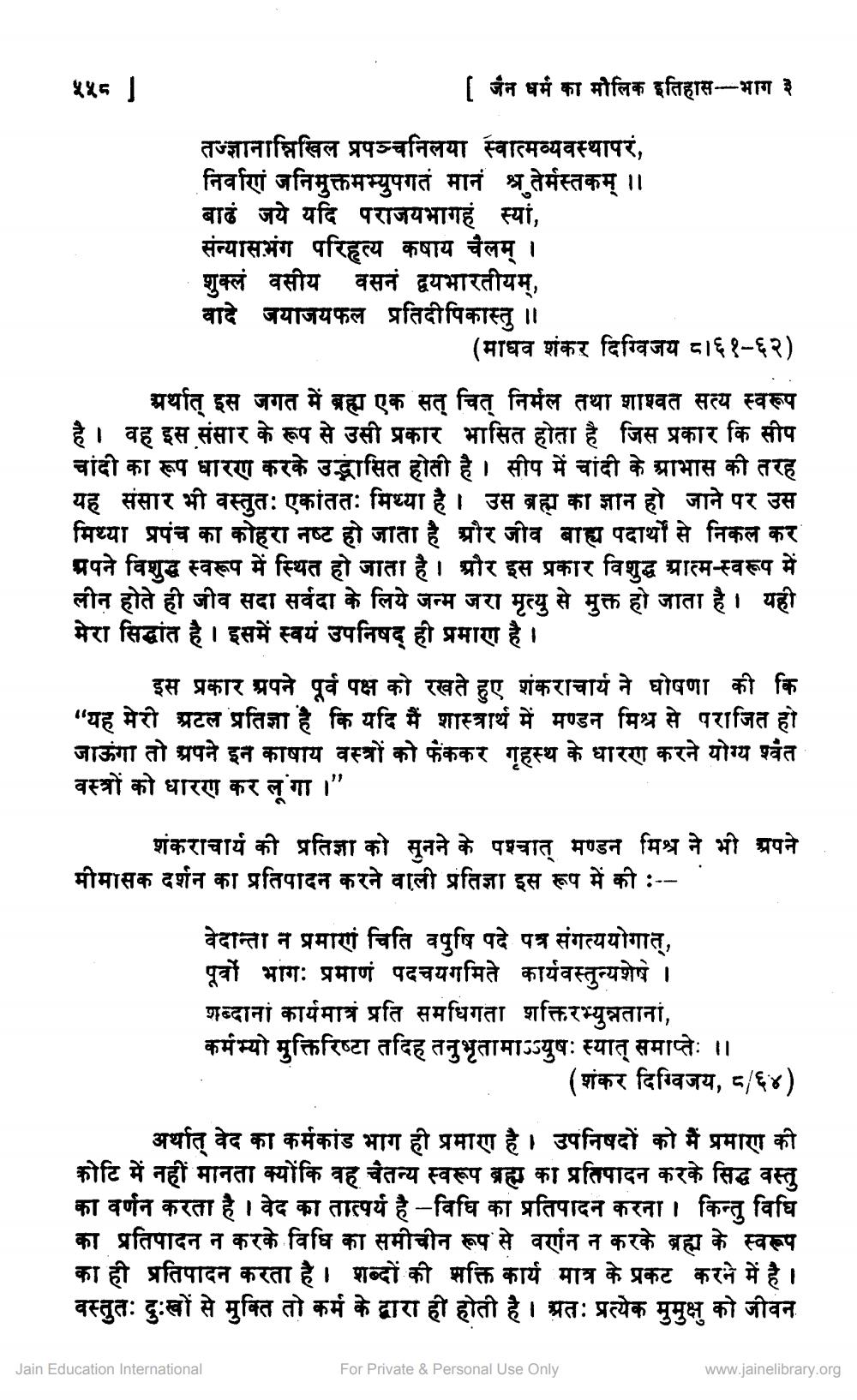________________
५५८ ।
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ३
तज्ज्ञानानिखिल प्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्थापरं, निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्र तेर्मस्तकम् ।। बाढं जये यदि पराजयभागहं स्यां, संन्यासभंग परिहृत्य कषाय चैलम् । शुक्लं वसीय वसनं द्वयभारतीयम्, वादे जयाजयफल प्रतिदीपिकास्तु ॥
(माधव शंकर दिग्विजय ८।६१-६२) अर्थात् इस जगत में ब्रह्म एक सत् चित निर्मल तथा शाश्वत सत्य स्वरूप है। वह इस संसार के रूप से उसी प्रकार भासित होता है जिस प्रकार कि सीप चांदी का रूप धारण करके उद्भासित होती है। सीप में चांदी के आभास की तरह यह संसार भी वस्तुत: एकांततः मिथ्या है। उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर उस मिथ्या प्रपंच का कोहरा नष्ट हो जाता है और जीव बाह्य पदार्थों से निकल कर अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। और इस प्रकार विशुद्ध प्रात्म-स्वरूप में लीन होते ही जीव सदा सर्वदा के लिये जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यही मेरा सिद्धांत है । इसमें स्वयं उपनिषद् ही प्रमाण है।
इस प्रकार अपने पूर्व पक्ष को रखते हुए शंकराचार्य ने घोषणा की कि "यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है कि यदि मैं शास्त्रार्थ में मण्डन मिश्र से पराजित हो जाऊंगा तो अपने इन काषाय वस्त्रों को फेंककर गृहस्थ के धारण करने योग्य श्वत वस्त्रों को धारण कर लूगा।"
शंकराचार्य की प्रतिज्ञा को सुनने के पश्चात् मण्डन मिश्र ने भी अपने मीमासक दर्शन का प्रतिपादन करने वाली प्रतिज्ञा इस रूप में की :--
वेदान्ता न प्रमाणं चिति वपुषि पदे पत्र संगत्ययोगात्, पूर्वो भागः प्रमाणं पदचयगमिते कार्यवस्तुन्यशेषे । शब्दानां कार्यमा प्रति समधिगता शक्तिरभ्युन्नतानां, कर्मभ्यो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृतामाऽयुषः स्यात् समाप्तेः ।।
(शंकर दिग्विजय, ८/६४) अर्थात वेद का कर्मकांड भाग ही प्रमाण है। उपनिषदों को मैं प्रमाण की कोटि में नहीं मानता क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन करके सिद्ध वस्तु का वर्णन करता है । वेद का तात्पर्य है --विधि का प्रतिपादन करना। किन्तु विधि का प्रतिपादन न करके विधि का समीचीन रूप से वर्णन न करके ब्रह्म के स्वरूप का ही प्रतिपादन करता है। शब्दों की भक्ति कार्य मात्र के प्रकट करने में है। वस्तुतः दुःखों से मुक्ति तो कर्म के द्वारा ही होती है । अतः प्रत्येक मुमुक्षु को जीवन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org