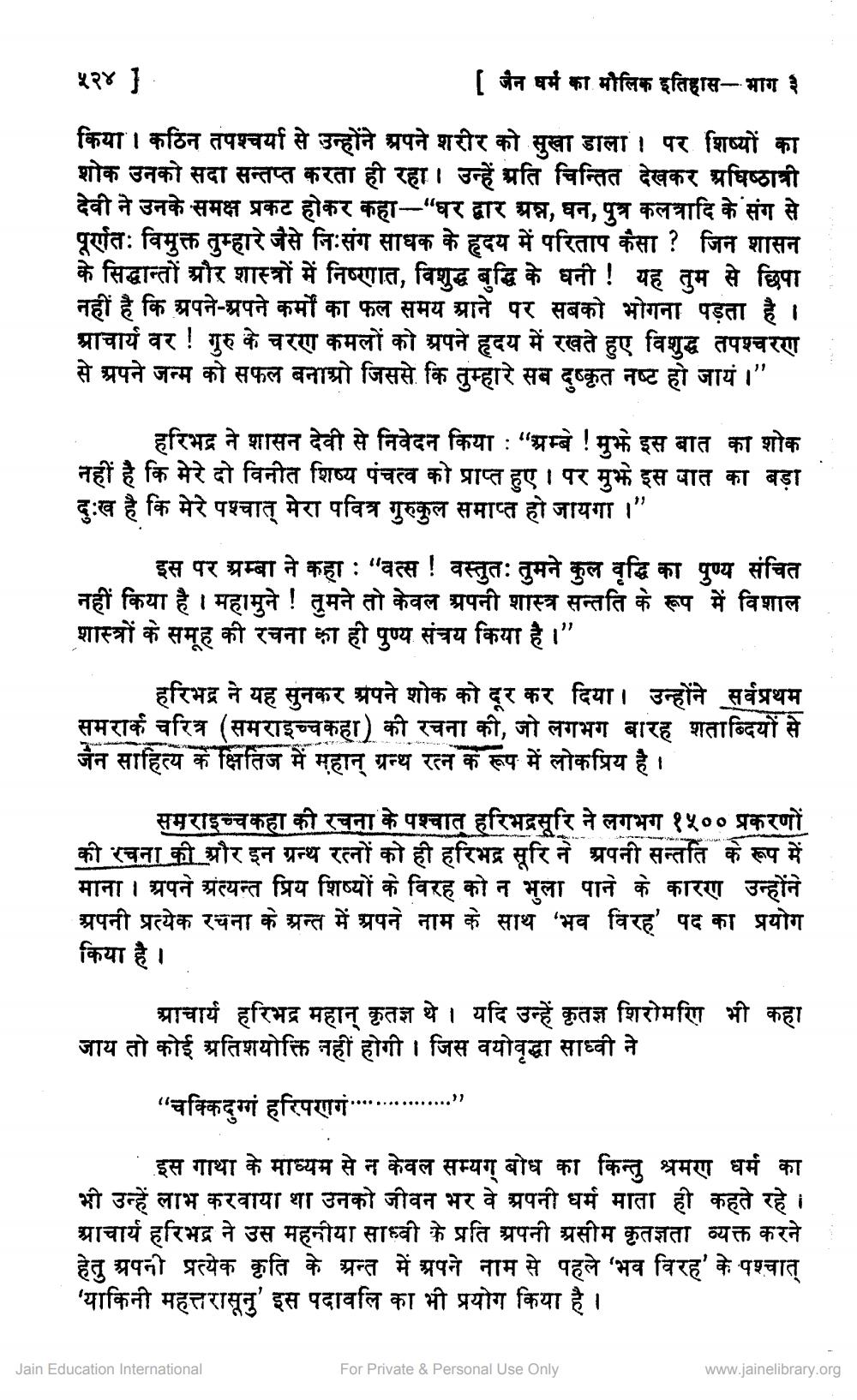________________
५२४ 1.
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ३
किया। कठिन तपश्चर्या से उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। पर शिष्यों का शोक उनको सदा सन्तप्त करता ही रहा। उन्हें प्रति चिन्तित देखकर अधिष्ठात्री देवी ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा-"घर द्वार अन्न, धन, पुत्र कलत्रादि के संग से पूर्णतः विमुक्त तुम्हारे जैसे निःसंग साधक के हृदय में परिताप कैसा? जिन शासन के सिद्धान्तों और शास्त्रों में निष्णात, विशुद्ध बुद्धि के धनी ! यह तुम से छिपा नहीं है कि अपने-अपने कर्मों का फल समय आने पर सबको भोगना पड़ता है । प्राचार्य वर ! गुरु के चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हुए विशुद्ध तपश्चरण से अपने जन्म को सफल बनाओ जिससे कि तुम्हारे सब दुष्कृत नष्ट हो जायं।"
हरिभद्र ने शासन देवी से निवेदन किया : "अम्बे ! मुझे इस बात का शोक नहीं है कि मेरे दो विनीत शिष्य पंचत्व को प्राप्त हुए। पर मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि मेरे पश्चात् मेरा पवित्र गुरुकुल समाप्त हो जायगा।"
इस पर अम्बा ने कहा : "वत्स ! वस्तुतः तुमने कुल वृद्धि का पुण्य संचित नहीं किया है । महामुने ! तुमने तो केवल अपनी शास्त्र सन्तति के रूप में विशाल शास्त्रों के समूह की रचना का ही पुण्य संचय किया है।"
हरिभद्र ने यह सुनकर अपने शोक को दूर कर दिया। उन्होंने सर्वप्रथम समरार्क चरित्र (समराइच्चकहा) की रचना की, जो लगभग बारह शताब्दियों से जैन साहित्य के क्षितिज में महान् ग्रन्थ रत्न के रूप में लोकप्रिय है।
समराइच्चकहा की रचना के पश्चात् हरिभद्रसूरि ने लगभग १५०० प्रकरणों की रचना की और इन ग्रन्थ रत्नों को ही हरिभद्र सूरि ने अपनी सन्तति के रूप में माना। अपने अंत्यन्त प्रिय शिष्यों के विरह को न भुला पाने के कारण उन्होंने अपनी प्रत्येक रचना के अन्त में अपने नाम के साथ 'भव विरह' पद का प्रयोग किया है।
........
"
प्राचार्य हरिभद्र महान् कृतज्ञ थे। यदि उन्हें कृतज्ञ शिरोमरिण भी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस वयोवृद्धा साध्वी ने
"चक्किदुग्गं हरिपणगं........ ___ इस गाथा के माध्यम से न केवल सम्यग् बोध का किन्तु श्रमण धर्म का भी उन्हें लाभ करवाया था उनको जीवन भर वे अपनी धर्म माता ही कहते रहे। आचार्य हरिभद्र ने उस महनीया साध्वी के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु अपनी प्रत्येक कृति के अन्त में अपने नाम से पहले 'भव विरह' के पश्चात् 'याकिनी महत्तरासूनु' इस पदावलि का भी प्रयोग किया है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org