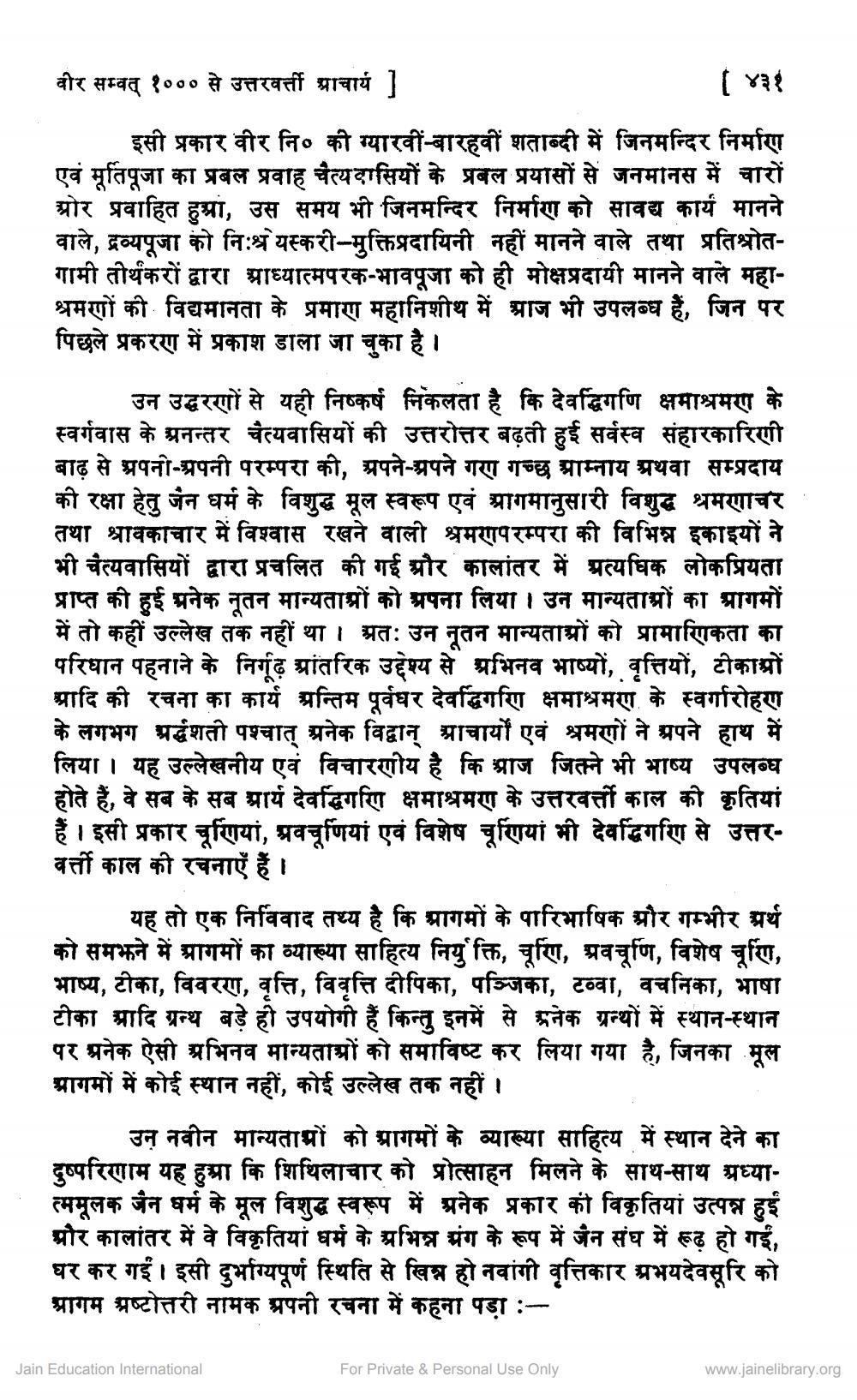________________
वीर सम्वत् १००० से उत्तरवर्ती प्राचार्य ]
[ ४३१
इसी प्रकार वीर नि० की ग्यारवीं-बारहवीं शताब्दी में जिनमन्दिर निर्माण एवं मूर्तिपूजा का प्रबल प्रवाह चैत्यदासियों के प्रबल प्रयासों से जनमानस में चारों ओर प्रवाहित हुआ, उस समय भी जिनमन्दिर निर्माण को सावध कार्य मानने वाले, द्रव्यपूजा को निःश्रेयस्करी-मुक्तिप्रदायिनी नहीं मानने वाले तथा प्रतिश्रोतगामी तीर्थंकरों द्वारा प्राध्यात्मपरक-भावपूजा को ही मोक्षप्रदायी मानने वाले महाश्रमणों की विद्यमानता के प्रमाण महानिशीथ में आज भी उपलब्ध हैं, जिन पर पिछले प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है।
उन उद्धरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गवास के अनन्तर चैत्यवासियों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सर्वस्व संहारकारिणी बाढ़ से अपनी-अपनी परम्परा की, अपने-अपने गरण गच्छ प्राम्नाय अथवा सम्प्रदाय की रक्षा हेतु जैन धर्म के विशुद्ध मूल स्वरूप एवं प्रागमानुसारी विशुद्ध श्रमरणाचर तथा श्रावकाचार में विश्वास रखने वाली श्रमरणपरम्परा की विभिन्न इकाइयों ने भी चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित की गई और कालांतर में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की हुई अनेक नूतन मान्यताओं को अपना लिया। उन मान्यताओं का आगमों में तो कहीं उल्लेख तक नहीं था। अतः उन नूतन मान्यताओं को प्रामाणिकता का परिधान पहनाने के निर्गढ़ प्रांतरिक उद्देश्य से अभिनव भाष्यों, वृत्तियों, टीकाओं आदि की रचना का कार्य अन्तिम पूर्वधर देवद्धिगणि क्षमाश्रमरण के स्वर्गारोहण के लगभग अर्द्धशती पश्चात् अनेक विद्वान् आचार्यों एवं श्रमणों ने अपने हाथ में लिया। यह उल्लेखनीय एवं विचारणीय है कि आज जितने भी भाष्य उपलब्ध होते हैं, वे सब के सब प्रार्य देवद्धिगरिण क्षमाश्रमण के उत्तरवर्ती काल की कृतियां हैं । इसी प्रकार चूणियां, अवचूर्णियां एवं विशेष चूणियां भी देवद्धिगणि से उत्तरवर्ती काल की रचनाएँ हैं।
यह तो एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रागमों के पारिभाषिक और गम्भीर अर्थ को समझने में प्रागमों का व्याख्या साहित्य नियुक्ति, चूरिण, प्रवचूणि, विशेष चरिण, भाष्य, टीका, विवरण, वत्ति, विवृत्ति दीपिका, पञ्जिका, टव्वा, वनिका, भाषा टीका आदि ग्रन्थ बड़े ही उपयोगी हैं किन्तु इनमें से अनेक ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर अनेक ऐसी अभिनव मान्यताओं को समाविष्ट कर लिया गया है, जिनका मूल आगमों में कोई स्थान नहीं, कोई उल्लेख तक नहीं।
उन नवीन मान्यतामों को प्रागमों के व्याख्या साहित्य में स्थान देने का दुष्परिणाम यह हुआ कि शिथिलाचार को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ अध्यात्ममूलक जैन धर्म के मूल विशुद्ध स्वरूप में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हुई और कालांतर में वे विकृतियां धर्म के अभिन्न अंग के रूप में जैन संघ में रूढ़ हो गईं, घर कर गई। इसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से खिन्न हो नवांगी वृत्तिकार अभयदेवसूरि को पागम अष्टोत्तरी नामक अपनी रचना में कहना पड़ा :
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org