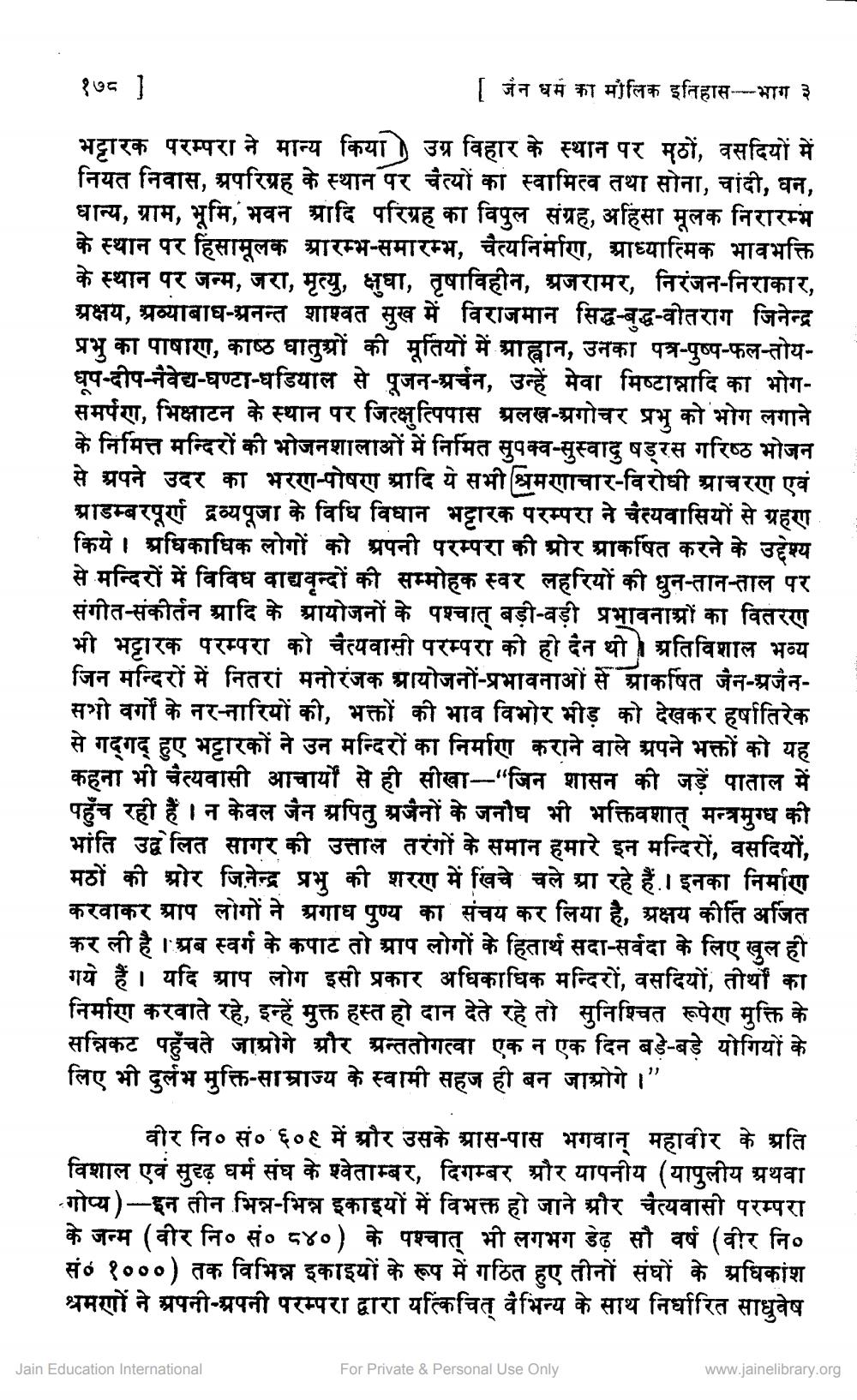________________
१७८ ]
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास - भाग ३
भट्टारक परम्परा ने मान्य किया उग्र विहार के स्थान पर मठों, वसदियों में नियत निवास, अपरिग्रह के स्थान पर चैत्यों का स्वामित्व तथा सोना, चांदी, धन, धान्य, ग्राम, भूमि, भवन आदि परिग्रह का विपुल संग्रह, अहिंसा मूलक निरारम्भ के स्थान पर हिंसामूलक आरम्भ समारम्भ, चैत्यनिर्माण, आध्यात्मिक भावभक्ति के स्थान पर जन्म, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृषाविहीन, अजरामर, निरंजन- निराकार, अक्षय, अव्याबाघ - अनन्त शाश्वत सुख में विराजमान सिद्ध-बुद्ध- वीतराग जिनेन्द्र प्रभु का पाषाण, काष्ठ घातुत्रों की मूर्तियों में आह्वान, उनका पत्र- पुष्प-फल-तोयधूप दीप नैवेद्य - घण्टा घडियाल से पूजन-अर्चन, उन्हें मेवा मिष्टान्नादि का भोगसमर्पण, भिक्षाटन के स्थान पर जित्क्षुत्पिपास अलख - अगोचर प्रभु को भोग लगाने के निमित्त मन्दिरों की भोजनशालाओं में निर्मित सुपक्व - सुस्वादु षड्स गरिष्ठ भोजन से अपने उदर का भरण-पोषण आदि ये सभी श्रमणाचार - विरोधी श्राचरण एवं प्राडम्बरपूर्ण द्रव्य पूजा के विधि विधान भट्टारक परम्परा ने चैत्यवासियों से ग्रहण किये। अधिकाधिक लोगों को अपनी परम्परा की ओर प्राकर्षित करने के उद्देश्य से मन्दिरों में विविध वाद्यवृन्दों की सम्मोहक स्वर लहरियों की धुन-तान-ताल पर संगीत-संकीर्तन आदि के प्रयोजनों के पश्चात् बड़ी-बड़ी प्रभावनाओं का वितरण भी भट्टारक परम्परा को चैत्यवासी परम्परा की हो दैन थी । प्रतिविशाल भव्य जिन मन्दिरों में नितरां मनोरंजक प्रयोजनों-प्रभावनाओं से आकर्षित जैन प्रजैनसभी वर्गों के नर-नारियों की, भक्तों की भाव विभोर भीड़ को देखकर हर्षातिरेक से गद्गद् हुए भट्टारकों ने उन मन्दिरों का निर्माण कराने वाले अपने भक्तों को यह कहना भी चैत्यवासी आचार्यों से ही सीखा - " जिन शासन की जड़ें पाताल में पहुँच रही हैं । न केवल जैन अपितु जैनों के जनौघ भी भक्तिवशात् मन्त्रमुग्ध की भांति उद्व ेलित सागर की उत्ताल तरंगों के समान हमारे इन मन्दिरों, वसदियों, मठों की ओर जिनेन्द्र प्रभु की शरण में खिंचे चले आ रहे हैं। इनका निर्माण करवाकर आप लोगों ने प्रगाध पुण्य का संचय कर लिया है, अक्षय कीर्ति अर्जित कर ली है । अब स्वर्ग के कपाट तो आप लोगों के हितार्थ सदा-सर्वदा के लिए खुल ही गये हैं। यदि आप लोग इसी प्रकार अधिकाधिक मन्दिरों, वसदियों, तीर्थों का निर्माण करवाते रहे, इन्हें मुक्त हस्त हो दान देते रहे तो सुनिश्चित रूपेण मुक्ति के सन्निकट पहुँचते जानोगे और अन्ततोगत्वा एक न एक दिन बड़े-बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति-साम्राज्य के स्वामी सहज ही बन जाओगे ।"
वीर नि० सं० ६०६ में और उसके आस-पास भगवान् महावीर के प्रति विशाल एवं सुदृढ़ धर्म संघ के श्वेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय ( यापुलीय अथवा - गोप्य ) - इन तीन भिन्न-भिन्न इकाइयों में विभक्त हो जाने और चैत्यवासी परम्परा के जन्म ( वीर नि० सं० ८४० ) के पश्चात् भी लगभग डेढ़ सौ वर्ष ( वीर नि० सं० १०००) तक विभिन्न इकाइयों के रूप में गठित हुए तीनों संघों के अधिकांश श्रमणों ने अपनी-अपनी परम्परा द्वारा यत्किंचित् वैभिन्य के साथ निर्धारित साधुवेष
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org