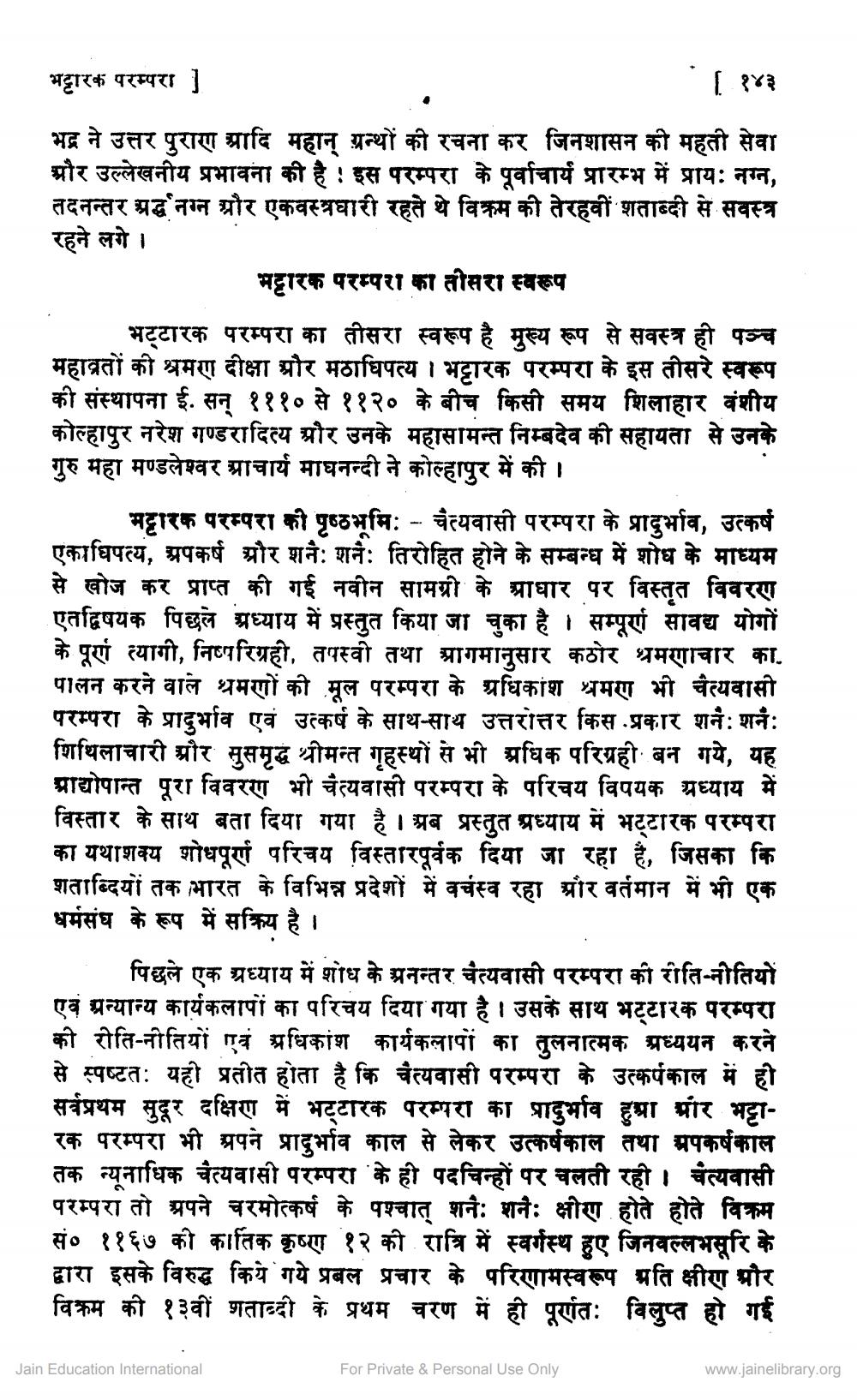________________
भट्टारक परम्परा ]
[ १४३ भद्र ने उत्तर पुराण आदि महान ग्रन्थों की रचना कर जिनशासन की महती सेवा और उल्लेखनीय प्रभावना की है । इस परम्परा के पूर्वाचार्य प्रारम्भ में प्रायः नग्न, तदनन्तर अर्द्धनग्न और एकवस्त्रधारी रहते थे विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से सवस्त्र रहने लगे।
भट्टारक परम्परा का तीसरा स्वरूप भट्टारक परम्परा का तीसरा स्वरूप है मुख्य रूप से सवस्त्र ही पञ्च महाव्रतों की श्रमण दीक्षा और मठाधिपत्य । भट्टारक परम्परा के इस तीसरे स्वरूप की संस्थापना ई. सन १११० से ११२० के बीच किसी समय शिलाहार वंशीय कोल्हापुर नरेश गण्डरादित्य और उनके महासामन्त निम्बदेव की सहायता से उनके गुरु महा मण्डलेश्वर प्राचार्य माघनन्दी ने कोल्हापुर में की।
___ मट्टारक परम्परा की पृष्ठभूमिः - चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव, उत्कर्ष एकाधिपत्य, अपकर्ष और शनैः शनैः तिरोहित होने के सम्बन्ध में शोध के माध्यम से खोज कर प्राप्त की गई नवीन सामग्री के आधार पर विस्तृत विवरण एतद्विषयक पिछले अध्याय में प्रस्तुत किया जा चुका है । सम्पूर्ण सावध योगों के पूर्ण त्यागी, निष्परिग्रही, तपस्वी तथा आगमानुसार कठोर श्रमरणाचार का. पालन करने वाले श्रमरणों की मूल परम्परा के अधिकांश श्रमण भी चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव एवं उत्कर्ष के साथ-साथ उत्तरोत्तर किस प्रकार शनैः शन: शिथिलाचारी और सुसमृद्ध श्रीमन्त गृहस्थों से भी अधिक परिग्रही बन गये, यह प्राद्योपान्त पूरा विवरण भी चैत्यवासी परम्परा के परिचय विषयक अध्याय में विस्तार के साथ बता दिया गया है। अब प्रस्तुत अध्याय में भट्टारक परम्परा का यथाशक्य शोधपूर्ण परिचय विस्तारपूर्वक दिया जा रहा है, जिसका कि शताब्दियों तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में वर्चस्व रहा और वर्तमान में भी एक धर्मसंघ के रूप में सक्रिय है।।
पिछले एक अध्याय में शोध के अनन्तर चैत्यवासी परम्परा की रीति-नीतियों एवं अन्यान्य कार्यकलापों का परिचय दिया गया है। उसके साथ भट्टारक परम्परा की रीति-नीतियों एवं अधिकांश कार्यकलापों का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्टत: यही प्रतीत होता है कि चैत्यवासी परम्परा के उत्कर्पकाल में ही सर्वप्रथम सुदूर दक्षिण में भट्टारक परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ और भट्टारक परम्परा भी अपने प्रादुर्भाव काल से लेकर उत्कर्षकाल तथा अपकर्षकाल तक न्यूनाधिक चैत्यवासी परम्परा के ही पदचिन्हों पर चलती रही। चैत्यवासी परम्परा तो अपने चरमोत्कर्ष के पश्चात् शनैः शनैः क्षीण होते होते विक्रम सं० ११६७ की कार्तिक कृष्ण १२ की रात्रि में स्वर्गस्थ हुए जिनवल्लभसूरि के द्वारा इसके विरुद्ध किये गये प्रबल प्रचार के परिणामस्वरूप प्रति क्षीण और विक्रम की १३वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही पूर्णतः विलुप्त हो गई
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org