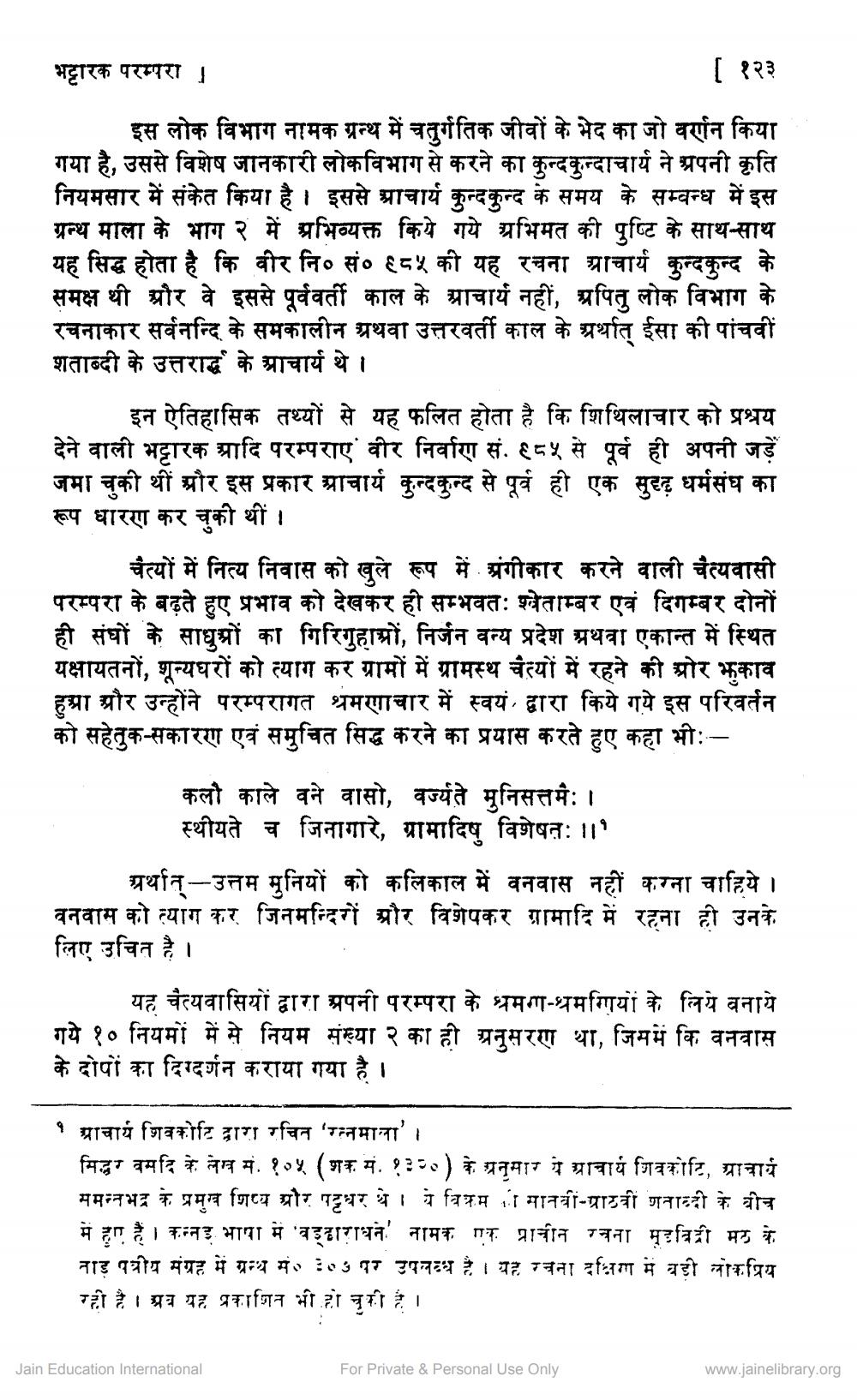________________
भट्टारक परम्परा ।
[ १२३
इस लोक विभाग नामक ग्रन्थ में चतुर्गतिक जीवों के भेद का जो वर्णन किया गया है, उससे विशेष जानकारी लोकविभाग से करने का कुन्दकुन्दाचार्य ने अपनी कृति नियमसार में संकेत किया है। इससे प्राचार्य कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ माला के भाग २ में अभिव्यक्त किये गये अभिमत की पुष्टि के साथ-साथ यह सिद्ध होता है कि वीर नि० सं० ६८५ की यह रचना प्राचार्य कुन्दकुन्द के समक्ष थी और वे इससे पूर्ववर्ती काल के प्राचार्य नहीं, अपितु लोक विभाग के रचनाकार सर्वनन्दि के समकालीन अथवा उत्तरवर्ती काल के अर्थात् ईसा की पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के आचार्य थे ।
इन ऐतिहासिक तथ्यों से यह फलित होता है कि शिथिलाचार को प्रश्रय देने वाली भट्टारक आदि परम्पराए वीर निर्वाण सं. ९८५ से पूर्व ही अपनी जड़ें जमा चुकी थीं और इस प्रकार प्राचार्य कुन्दकुन्द से पूर्व ही एक सुदृढ़ धर्मसंघ का रूप धारण कर चुकी थीं।
चैत्यों में नित्य निवास को खुले रूप में अंगीकार करने वाली चैत्यवासी परम्परा के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर ही सम्भवतः श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही संघों के साधुनों का गिरिगुहारों, निर्जन वन्य प्रदेश अथवा एकान्त में स्थित यक्षायतनों, शून्यघरों को त्याग कर ग्रामों में ग्रामस्थ चैत्यों में रहने की ओर झकाव हया और उन्होंने परम्परागत श्रमणाचार में स्वयं द्वारा किये गये इस परिवर्तन को सहेतुक-सकारण एवं समुचित सिद्ध करने का प्रयास करते हुए कहा भी:
कलो काले वने वासो, वय॑ते मुनिसत्तमः ।
स्थीयते च जिनागारे, ग्रामादिषु विशेषतः ।। अर्थात-उत्तम मनियों को कलिकाल में वनवास नहीं करना चाहिये। वनवाम को त्याग कर जिनमन्दिरों और विशेपकर ग्रामादि में रहना ही उनके लिए उचित है।
यह चैत्यवासियों द्वारा अपनी परम्परा के श्रमग-श्रमगिगयों के लिये बनाये गये १० नियमों में से नियम संख्या २ का ही अनुसरण था, जिसमें कि वनवास के दोपों का दिग्दर्शन कराया गया है।
१ प्राचार्य शिवकोटि द्वारा रचित 'रत्नमाला'। मिद्धर वमदि के लेख म. १०५ (शक मं. १३२०) के अनुमार ये प्राचार्य गिवकोटि, प्राचार्य ममन्तभद्र के प्रमुख शिप्य और पट्टधर थे। ये विक्रम । मातवीं-पाठवीं शताब्दी के बीच में हुए हैं । कन्नड़ भाषा में 'वहाराधने' नामक एक प्राचीन रचना मुद्दविद्री मठ के ताड़ पत्रीय संग्रह में ग्रन्थ म०:०७ पर उपलब्ध है । यह रचना दक्षिा में बड़ी लोकप्रिय रही है। अब यह प्रकाशित भी हो चुकी है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org