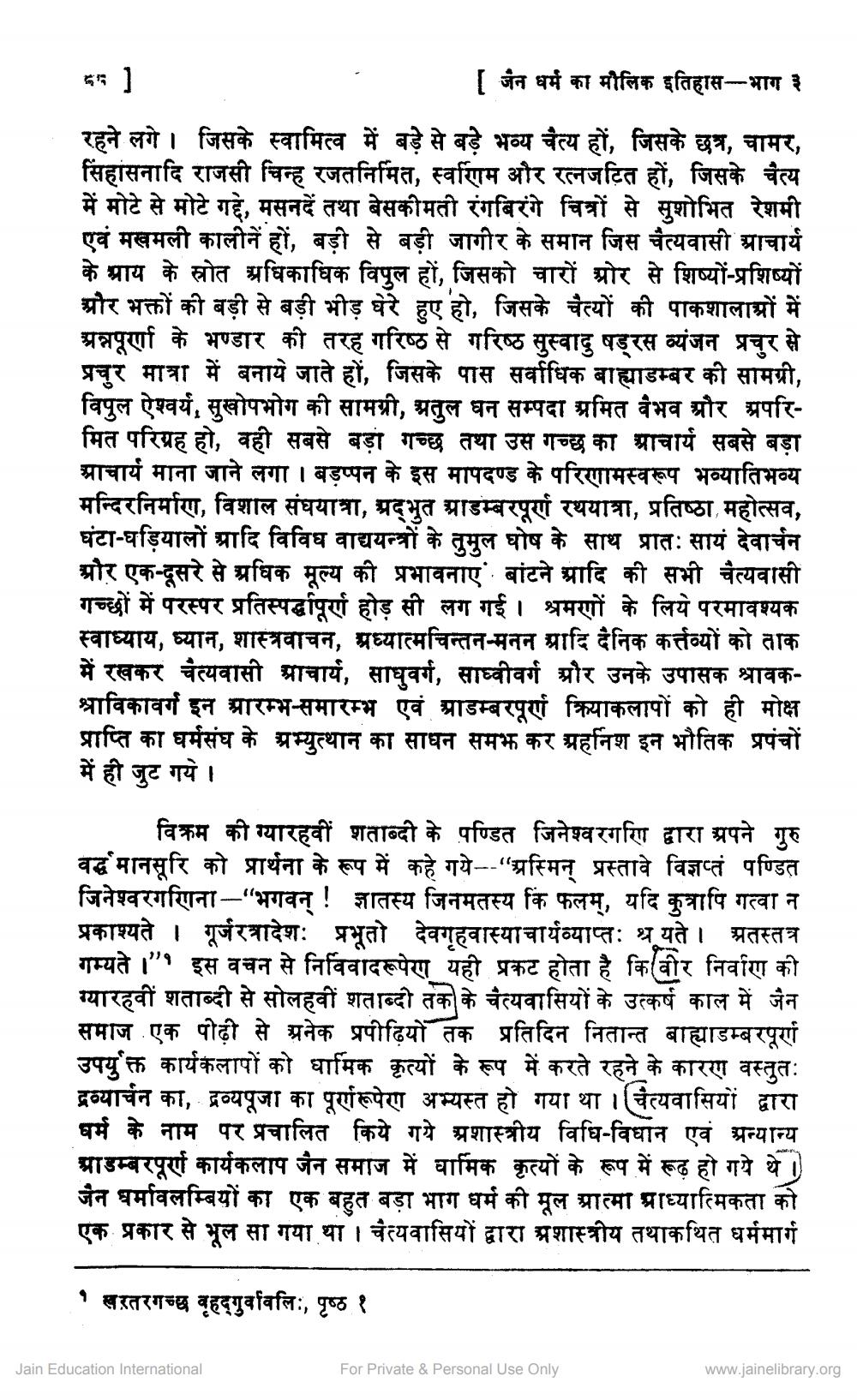________________
८८ ]
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ३
रहने लगे। जिसके स्वामित्व में बड़े से बड़े भव्य चैत्य हों, जिसके छत्र, चामर, सिंहासनादि राजसी चिन्ह रजतनिर्मित, स्वर्णिम और रत्नजटित हों, जिसके चैत्य में मोटे से मोटे गद्दे, मसनदें तथा बेसकीमती रंगबिरंगे चित्रों से सुशोभित रेशमी एवं मखमली कालीनें हों, बड़ी से बड़ी जागीर के समान जिस चैत्यवासी आचार्य के प्राय के स्रोत अधिकाधिक विपुल हों, जिसको चारों ओर से शिष्यों-प्रशिष्यों और भक्तों की बड़ी से बड़ी भीड़ घेरे हुए हो, जिसके चैत्यों की पाकशालाओं में अन्नपूर्णा के भण्डार की तरह गरिष्ठ से गरिष्ठ सुस्वादु षड्रस व्यंजन प्रचुर से प्रचुर मात्रा में बनाये जाते हों, जिसके पास सर्वाधिक बाह्याडम्बर की सामग्री, विपुल ऐश्वर्य, सुखोपभोग की सामग्री, अतुल धन सम्पदा अमित वैभव और अपरिमित परिग्रह हो, वही सबसे बड़ा गच्छ तथा उस गच्छ का प्राचार्य सबसे बड़ा प्राचार्य माना जाने लगा । बड़प्पन के इस मापदण्ड के परिणामस्वरूप भव्यातिभव्य मन्दिरनिर्माण, विशाल संघयात्रा, अद्भुत प्राडम्बरपूर्ण रथयात्रा, प्रतिष्ठा महोत्सव, घंटा-घड़ियालों आदि विविध वाद्ययन्त्रों के तुमुल घोष के साथ प्रातः सायं देवार्चन
और एक-दूसरे से अधिक मूल्य की प्रभावनाएं बांटने आदि की सभी चैत्यवासी गच्छों में परस्पर प्रतिस्पर्धापूर्ण होड़ सी लग गई। श्रमरणों के लिये परमावश्यक स्वाध्याय, ध्यान, शास्त्रवाचन, अध्यात्मचिन्तन-मनन आदि दैनिक कर्तव्यों को ताक में रखकर चैत्यवासी प्राचार्य, साधुवर्ग, साध्वीवर्ग और उनके उपासक श्रावकश्राविकावर्ग इन प्रारम्भ-समारम्भ एवं आडम्बरपूर्ण क्रियाकलापों को ही मोक्ष प्राप्ति का धर्मसंघ के अभ्युत्थान का साधन समझ कर अहर्निश इन भौतिक प्रपंचों में ही जुट गये।
विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के पण्डित जिनेश्वरगणि द्वारा अपने गुरु वर्द्ध मानसूरि को प्रार्थना के रूप में कहे गये--"अस्मिन् प्रस्तावे विज्ञप्तं पण्डित जिनेश्वरगणिना-"भगवन् ! ज्ञातस्य जिनमतस्य किं फलम, यदि कुत्रापि गत्वा न प्रकाश्यते । गूर्जरत्रादेशः प्रभूतो देवगृहवास्याचार्यव्याप्तः श्रू यते। अतस्तत्र गम्यते ।" इस वचन से निर्विवादरूपेण यही प्रकट होता है कि वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक के चैत्यवासियों के उत्कर्ष काल में जैन समाज एक पीढ़ी से अनेक प्रपीढियों तक प्रतिदिन नितान्त बाह्याडम्बरपूर्ण उपयुक्त कार्यकलापों को धार्मिक कृत्यों के रूप में करते रहने के कारण वस्तुतः द्रव्यार्चन का, द्रव्यपूजा का पूर्णरूपेण अभ्यस्त हो गया था। (चैत्यवासियों द्वारा धर्म के नाम पर प्रचालित किये गये प्रशास्त्रीय विधि-विधान एवं अन्यान्य प्राडम्बरपूर्ण कार्यकलाप जैन समाज में वार्मिक कृत्यों के रूप में रूढ़ हो गये थे। जैन धर्मावलम्बियों का एक बहत बड़ा भाग धर्म की मूल आत्मा प्राध्यात्मिकता को एक प्रकार से भूल सा गया था। चैत्यवासियों द्वारा प्रशास्त्रीय तथाकथित धर्ममार्ग
' खरतरगच्छ वृहद्गुर्वावलिः, पृष्ठ १
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org