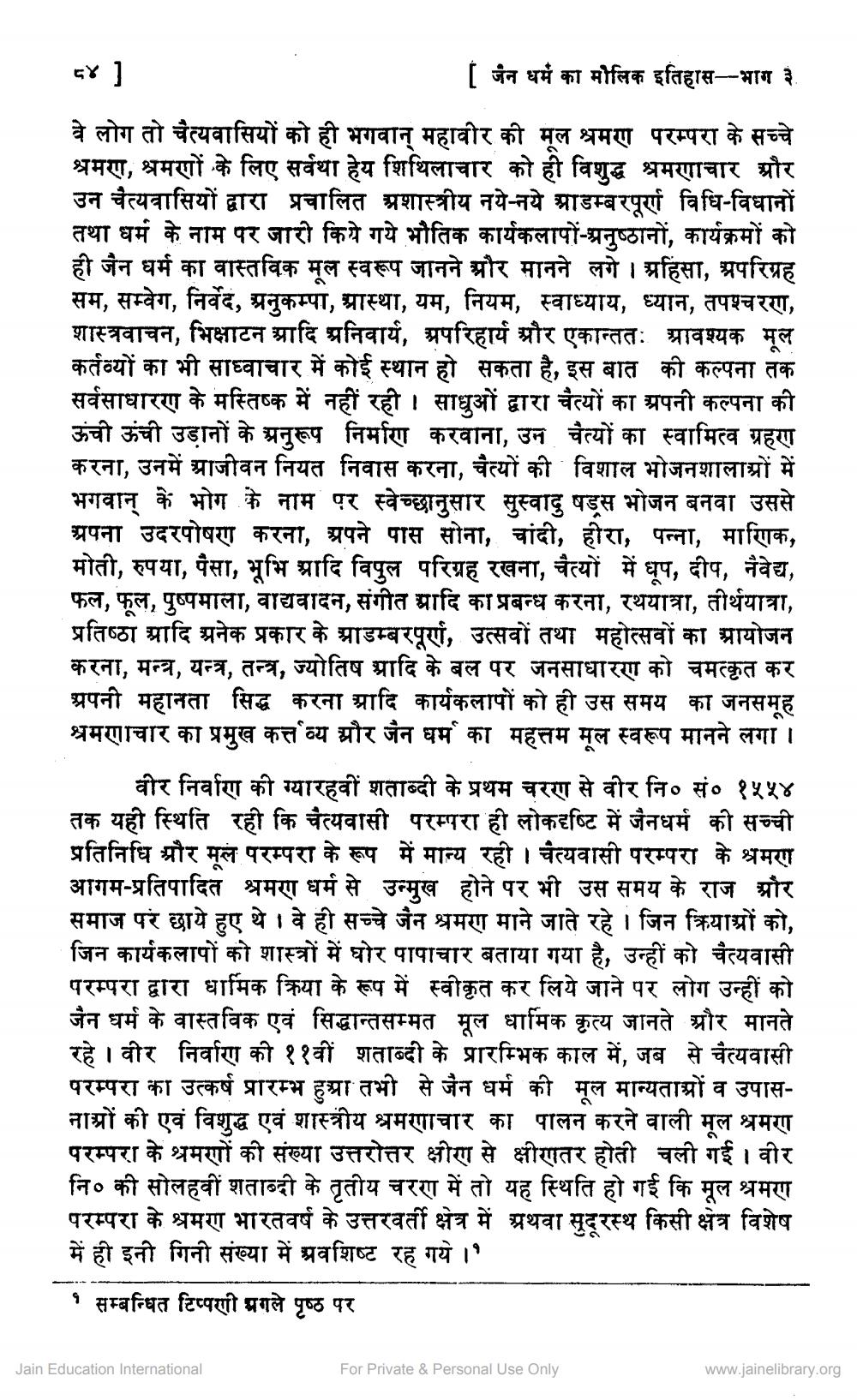________________
८४ ]
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ३ वे लोग तो चैत्यवासियों को ही भगवान् महावीर की मूल श्रमण परम्परा के सच्चे श्रमण, श्रमणों के लिए सर्वथा हेय शिथिलाचार को ही विशुद्ध श्रमणाचार और उन चैत्यवासियों द्वारा प्रचालित अशास्त्रीय नये-नये आडम्बरपूर्ण विधि-विधानों तथा धर्म के नाम पर जारी किये गये भौतिक कार्यकलापों-अनुष्ठानों, कार्यक्रमों को ही जैन धर्म का वास्तविक मूल स्वरूप जानने और मानने लगे । अहिंसा, अपरिग्रह सम, सम्वेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्था, यम, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, तपश्चरण, शास्त्रवाचन, भिक्षाटन आदि अनिवार्य, अपरिहार्य और एकान्ततः अावश्यक मूल कर्तव्यों का भी साध्वाचार में कोई स्थान हो सकता है, इस बात की कल्पना तक सर्वसाधारण के मस्तिष्क में नहीं रही। साधुओं द्वारा चैत्यों का अपनी कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ानों के अनुरूप निर्माण करवाना, उन चैत्यों का स्वामित्व ग्रहण करना, उनमें आजीवन नियत निवास करना, चैत्यों की विशाल भोजनशालाओं में भगवान् के भोग के नाम पर स्वेच्छानुसार सुस्वादु षड्स भोजन बनवा उससे अपना उदरपोषण करना, अपने पास सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, रुपया, पैसा, भूभि आदि विपुल परिग्रह रखना, चैत्यों में धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, पुष्पमाला, वाद्यवादन, संगीत आदि का प्रबन्ध करना, रथयात्रा, तीर्थयात्रा, प्रतिष्ठा आदि अनेक प्रकार के आडम्बरपूर्ण, उत्सवों तथा महोत्सवों का आयोजन करना, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, ज्योतिष आदि के बल पर जनसाधारण को चमत्कृत कर अपनी महानता सिद्ध करना आदि कार्यकलापों को ही उस समय का जनसमूह श्रमणाचार का प्रमुख कर्तव्य और जैन धर्म का महत्तम मूल स्वरूप मानने लगा।
वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण से वीर नि० सं० १५५४ तक यही स्थिति रही कि चैत्यवासी परम्परा ही लोकदृष्टि में जैनधर्म की सच्ची प्रतिनिधि और मूल परम्परा के रूप में मान्य रही। चैत्यवासी परम्परा के श्रमरण आगम-प्रतिपादित श्रमण धर्म से उन्मुख होने पर भी उस समय के राज और समाज पर छाये हुए थे । वे ही सच्चे जैन श्रमण माने जाते रहे । जिन क्रियाओं को, जिन कार्यकलापों को शास्त्रों में घोर पापाचार बताया गया है, उन्हीं को चैत्यवासी परम्परा द्वारा धार्मिक क्रिया के रूप में स्वीकृत कर लिये जाने पर लोग उन्हीं को जैन धर्म के वास्तविक एवं सिद्धान्तसम्मत मूल धार्मिक कृत्य जानते और मानते रहे । वीर निर्वाण की ११वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में, जब से चैत्यवासी परम्परा का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ तभी से जैन धर्म की मूल मान्यताओं व उपासनाओं की एवं विशुद्ध एवं शास्त्रीय श्रमणाचार का पालन करने वाली मूल श्रमण परम्परा के श्रमरणों की संख्या उत्तरोत्तर क्षीरण से क्षीणतर होती चली गई। वीर नि० की सोलहवीं शताब्दी के तृतीय चरण में तो यह स्थिति हो गई कि मूल श्रमण परम्परा के श्रमण भारतवर्ष के उत्तरवर्ती क्षेत्र में अथवा सुदूरस्थ किसी क्षेत्र विशेष में ही इनी गिनी संख्या में प्रवशिष्ट रह गये।'
१ सम्बन्धित टिप्पणी अगले पृष्ठ पर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org