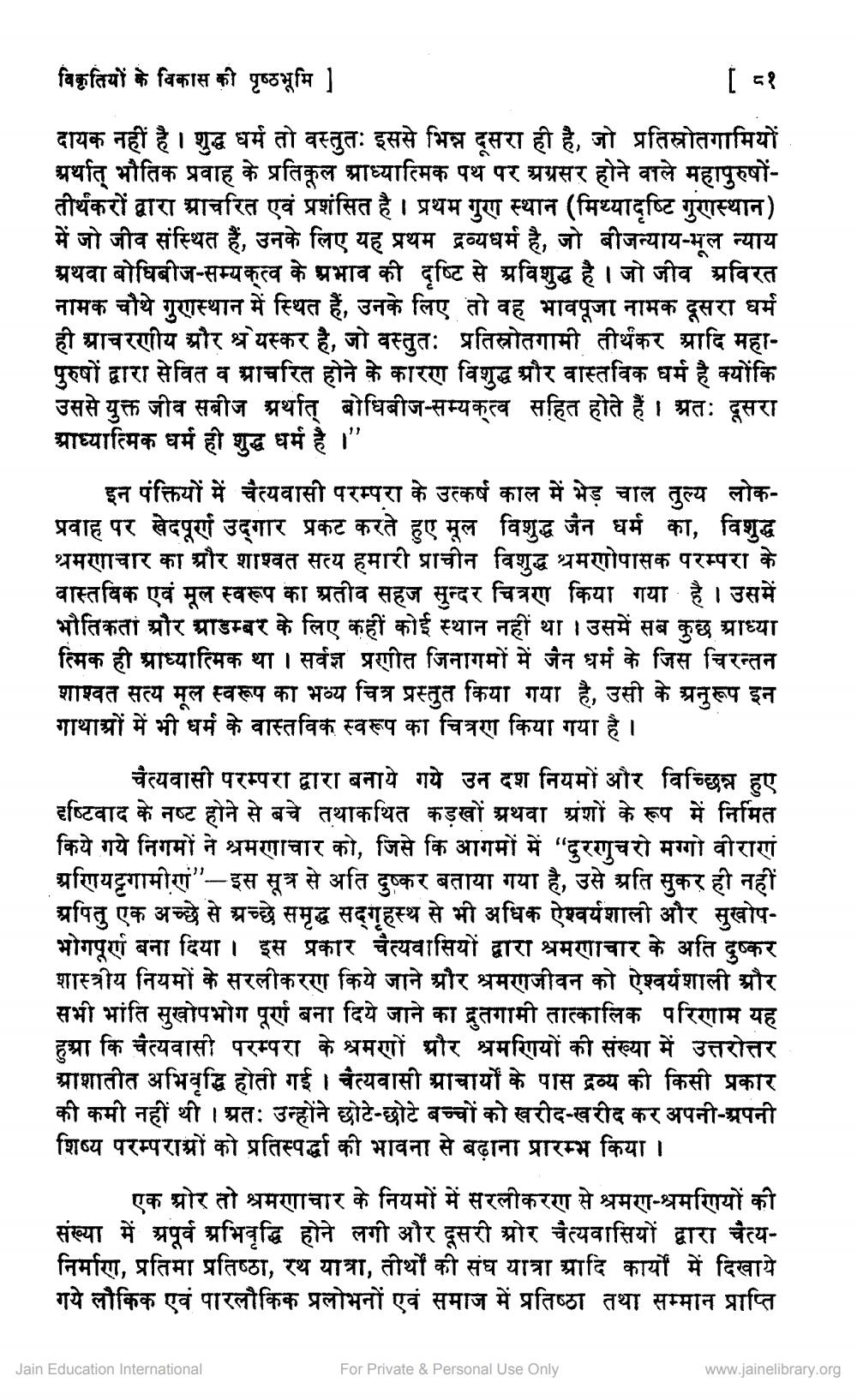________________
विकृतियों के विकास की पृष्ठभूमि ]
[ ८१ दायक नहीं है । शुद्ध धर्म तो वस्तुतः इससे भिन्न दूसरा ही है, जो प्रतिस्रोतगामियों अर्थात् भौतिक प्रवाह के प्रतिकूल प्राध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाले महापुरुषोंतीर्थंकरों द्वारा प्राचरित एवं प्रशंसित है । प्रथम गुण स्थान (मिथ्यादृष्टि गुणस्थान) में जो जीव संस्थित हैं, उनके लिए यह प्रथम द्रव्यधर्म है, जो बीजन्याय-मल न्याय अथवा बोधिबीज-सम्यक्त्व के प्रभाव की दृष्टि से अविशुद्ध है । जो जीव अविरत नामक चौथे गुणस्थान में स्थित हैं, उनके लिए तो वह भावपूजा नामक दूसरा धर्म ही आचरणीय और श्रेयस्कर है, जो वस्तुत: प्रतिस्रोतगामी तीर्थंकर आदि महापुरुषों द्वारा सेवित व पाचरित होने के कारण विशुद्ध और वास्तविक धर्म है क्योंकि उससे युक्त जीव सबीज अर्थात् बोधिबीज-सम्यक्त्व सहित होते हैं । अतः दूसरा आध्यात्मिक धर्म ही शुद्ध धर्म है ।" ।
इन पंक्तियों में चैत्यवासी परम्परा के उत्कर्ष काल में भेड़ चाल तुल्य लोकप्रवाह पर खेदपूर्ण उद्गार प्रकट करते हए मूल विशुद्ध जैन धर्म का, विशुद्ध श्रमणाचार का और शाश्वत सत्य हमारी प्राचीन विशुद्ध श्रमणोपासक परम्परा के वास्तविक एवं मूल स्वरूप का अतीव सहज सुन्दर चित्रण किया गया है । उसमें भौतिकता और आडम्बर के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था । उसमें सब कुछ प्राध्या त्मिक ही आध्यात्मिक था । सर्वज्ञ प्रणीत जिनागमों में जैन धर्म के जिस चिरन्तन शाश्वत सत्य मूल स्वरूप का भव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसी के अनुरूप इन गाथाओं में भी धर्म के वास्तविक स्वरूप का चित्रण किया गया है ।
चैत्यवासी परम्परा द्वारा बनाये गये उन दश नियमों और विच्छिन्न हुए दृष्टिवाद के नष्ट होने से बचे तथाकथित कड़खों अथवा अंशों के रूप में निर्मित किये गये निगमों ने श्रमणाचार को, जिसे कि आगमों में "दुराचरो मग्गो वीराणं अरिणयट्टगामीरगं"-इस सूत्र से अति दुष्कर बताया गया है, उसे अति सुकर ही नहीं अपितु एक अच्छे से अच्छे समृद्ध सद्गृहस्थ से भी अधिक ऐश्वर्यशाली और सुखोपभोगपूर्ण बना दिया। इस प्रकार चैत्यवासियों द्वारा श्रमणाचार के अति दुष्कर शास्त्रीय नियमों के सरलीकरण किये जाने और श्रमणजीवन को ऐश्वर्यशाली और सभी भांति सुखोपभोग पूर्ण बना दिये जाने का द्रुतगामी तात्कालिक परिणाम यह हुया कि चैत्यवासी परम्परा के श्रमणों और श्रमरिणयों की संख्या में उत्तरोत्तर आशातीत अभिवृद्धि होती गई। चैत्यवासी प्राचार्यों के पास द्रव्य की किसी प्रकार की कमी नहीं थी । अतः उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को खरीद-खरीद कर अपनी-अपनी शिष्य परम्पराओं को प्रतिस्पर्द्धा की भावना से बढ़ाना प्रारम्भ किया।
एक ओर तो श्रमणाचार के नियमों में सरलीकरण से श्रमण-श्रमणियों की संख्या में अपूर्व अभिवृद्धि होने लगी और दूसरी ओर चैत्यवासियों द्वारा चैत्यनिर्माण, प्रतिमा प्रतिष्ठा, रथ यात्रा, तीर्थों की संघ यात्रा आदि कार्यों में दिखाये गये लौकिक एवं पारलौकिक प्रलोभनों एवं समाज में प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्ति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org