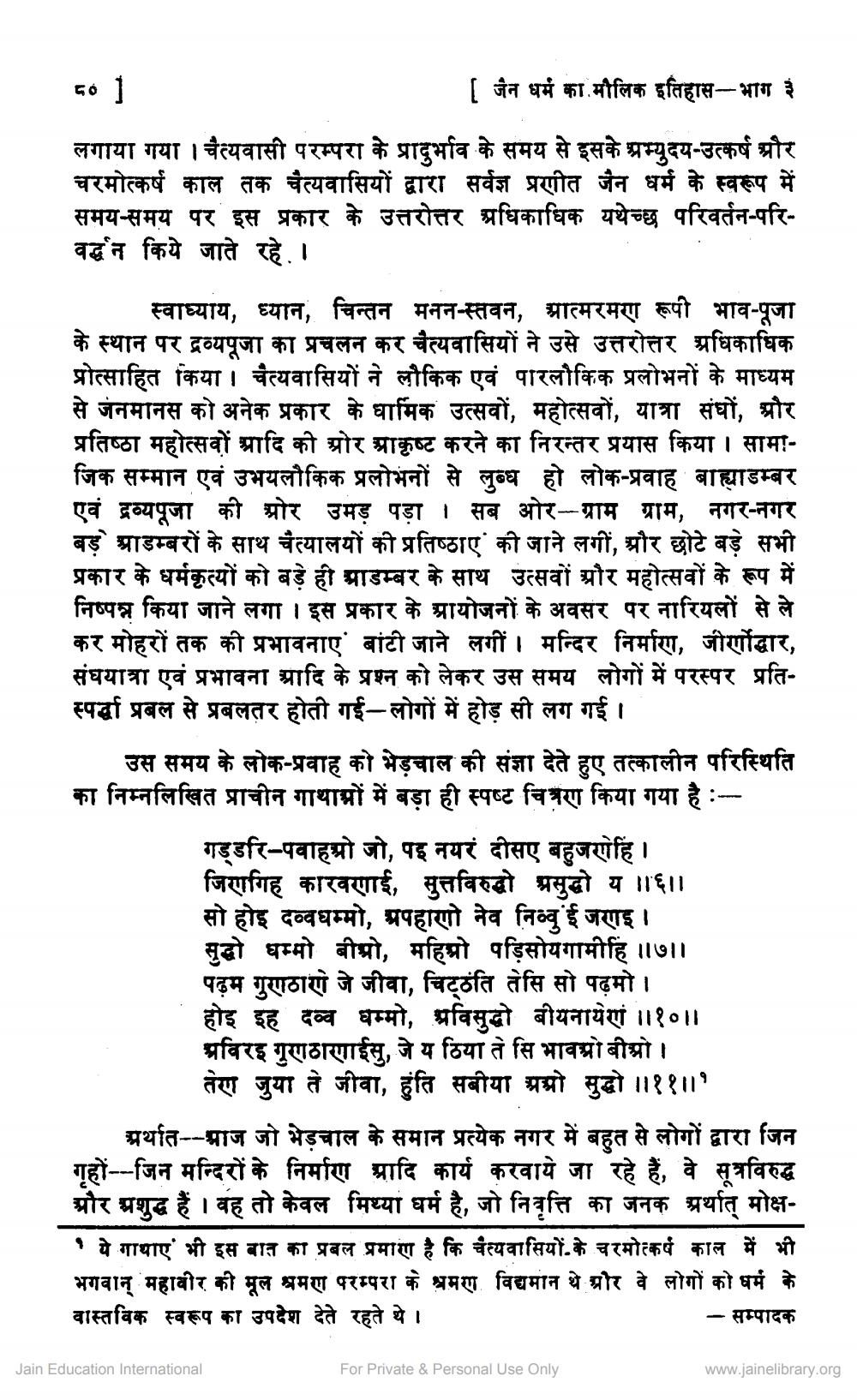________________
८० 1
[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास - भाग ३
लगाया गया । चैत्यवासी परम्परा के प्रादुर्भाव के समय से इसके अभ्युदय उत्कर्ष और चरमोत्कर्ष काल तक चैत्यवासियों द्वारा सर्वज्ञ प्ररणीत जैन धर्म के स्वरूप में समय - समय पर इस प्रकार के उत्तरोत्तर अधिकाधिक यथेच्छ परिवर्तन-परिवर्द्धन किये जाते रहे ।
स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन मनन- स्तवन, आत्मरमरण रूपी भाव - पूजा के स्थान पर द्रव्यपूजा का प्रचलन कर चैत्यवासियों ने उसे उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रोत्साहित किया । चैत्यवासियों ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रलोभनों के माध्यम से जनमानस को अनेक प्रकार के धार्मिक उत्सवों, महोत्सवों, यात्रा संघों, और प्रतिष्ठा महोत्सवों आदि की ओर आकृष्ट करने का निरन्तर प्रयास किया । सामाजिक सम्मान एवं उभयलौकिक प्रलोभनों से लुब्ध हो लोक-प्रवाह बाह्याडम्बर एवं द्रव्यपूजा की ओर उमड़ पड़ा । सब ओर - ग्राम ग्राम, नगर- नगर बड़ े आडम्बरों के साथ चैत्यालयों की प्रतिष्ठाएं की जाने लगीं, और छोटे बड़े सभी प्रकार के धर्मकृत्यों को बड़े ही आडम्बर के साथ उत्सवों औौर महोत्सवों के रूप में निष्पन्न किया जाने लगा । इस प्रकार के आयोजनों के अवसर पर नारियलों से ले कर मोहरों तक की प्रभावनाएं बांटी जाने लगीं । मन्दिर निर्मारण, जीर्णोद्धार, संघयात्रा एवं प्रभावना आदि के प्रश्न को लेकर उस समय लोगों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा प्रबल से प्रबलतर होती गई- लोगों में होड़ सी लग गई ।
उस समय के लोक-प्रवाह को भेड़चाल की संज्ञा देते हुए तत्कालीन परिस्थिति का निम्नलिखित प्राचीन गाथानों में बड़ा ही स्पष्ट चित्ररण किया गया है :
----
गड्डरि-पवाहो जो पइ नयरं दीसए बहुजणेहिं । जिराहि कारवाई, सुत्तविरुद्ध असुद्धो य ॥ ६ ॥ सो होइ दव्वधम्मो, अपहारणो नेव निव्वु ई जरगइ । सुद्धो धम्मो बीश्रो, महिनो पड़िसोयगामीहिं ॥ ७ ॥ पढ़म गुरगठाणे जे जीवा, चिट्ठति तेसि सो पढ़मो । होइ इह दव्व धम्मो, श्रविसुद्धो बीयनायेणं ।। १० ।। अविर गुरगठागाईसु, जे य ठिया ते सि भावप्रो बीओो । ते जुया ते जीवा, हुति सबीया अनो सुद्धो ॥ ११ ॥ १
अर्थात --माज जो भेड़चाल के समान प्रत्येक नगर में बहुत से लोगों द्वारा जिन गृहों -- जिन मन्दिरों के निर्माण आदि कार्य करवाये जा रहे हैं, वे सूत्रविरुद्ध और अशुद्ध हैं । वह तो केवल मिथ्या धर्म है, जो निवृत्ति का जनक अर्थात् मोक्ष
' ये गाथाएं भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि चैत्यवासियों के चरमोत्कर्ष काल में भी भगवान् महावीर की मूल श्रमण परम्परा के श्रमण विद्यमान थे और वे लोगों को धर्मं के वास्तविक स्वरूप का उपदेश देते रहते थे ।
सम्पादक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org