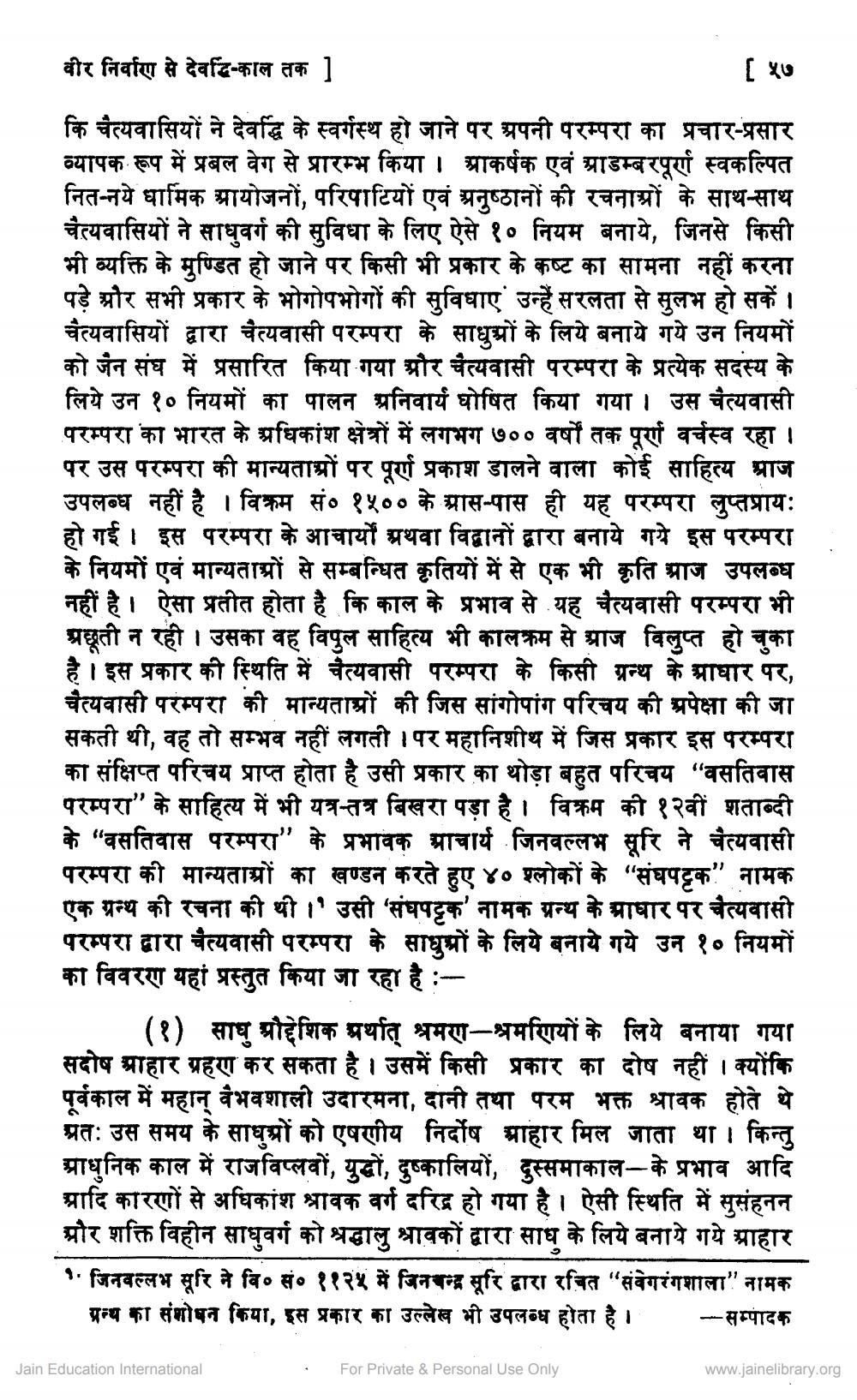________________
वीर निर्वाण से देवद्धि-काल तक ]
[ ५७
कि चैत्यवासियों ने देवद्धि के स्वर्गस्थ हो जाने पर अपनी परम्परा का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप में प्रबल वेग से प्रारम्भ किया । आकर्षक एवं ग्राडम्बरपूर्ण स्वकल्पित नित-नये धार्मिक आयोजनों, परिपाटियों एवं अनुष्ठानों की रचनाओं के साथ-साथ चैत्यवासियों ने साधुवर्ग की सुविधा के लिए ऐसे १० नियम बनाये, जिनसे किसी भी व्यक्ति के मुण्डित हो जाने पर किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़े और सभी प्रकार के भोगोपभोगों की सुविधाएं उन्हें सरलता से सुलभ हो सकें । चैत्यवासियों द्वारा चैत्यवासी परम्परा के साधुओं के लिये बनाये गये उन नियमों को जैन संघ में प्रसारित किया गया और चैत्यवासी परम्परा के प्रत्येक सदस्य के लिये उन १० नियमों का पालन अनिवार्य घोषित किया गया । उस चैत्यवासी परम्परा का भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग ७०० वर्षों तक पूर्ण वर्चस्व रहा । पर उस परम्परा की मान्यताओं पर पूर्ण प्रकाश डालने वाला कोई साहित्य प्राज उपलब्ध नहीं है । विक्रम सं० १५०० के आस-पास ही यह परम्परा लुप्तप्रायः हो गई । इस परम्परा के आचार्यो अथवा विद्वानों द्वारा बनाये गये इस परम्परा के नियमों एवं मान्यताओं से सम्बन्धित कृतियों में से एक भी कृति प्राज उपलब्ध नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि काल के प्रभाव से यह चैत्यवासी परम्परा भी
छूती रही। उसका वह विपुल साहित्य भी कालक्रम से आज विलुप्त हो चुका है । इस प्रकार की स्थिति में चैत्यवासी परम्परा के किसी ग्रन्थ के आधार पर, चैत्यवासी परम्परा की मान्यताओं की जिस सांगोपांग परिचय की अपेक्षा की जा सकती थी, वह तो सम्भव नहीं लगती । पर महानिशीथ में जिस प्रकार इस परम्परा का संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है उसी प्रकार का थोड़ा बहुत परिचय " वसतिवास परम्परा" के साहित्य में भी यत्र-तत्र बिखरा पड़ा है। विक्रम की १२वीं शताब्दी के " वसतिवास परम्परा" के प्रभावक प्राचार्य जिनवल्लभ सूरि ने चैत्यवासी परम्परा की मान्यताओं का खण्डन करते हुए ४० श्लोकों के "संघपट्टक" नामक एक ग्रन्थ की रचना की थी ।' उसी 'संघपट्टक' नामक ग्रन्थ के आधार पर चैत्यवासी परम्परा द्वारा चैत्यवासी परम्परा के साधुनों के लिये बनाये गये उन १० नियमों का विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :
(१) साधु प्रौद्दे शिक प्रर्थात् श्रमण - श्रमणियों के लिये बनाया गया सदोष आहार ग्रहण कर सकता है । उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं । क्योंकि पूर्वकाल में महान् वैभवशाली उदारमना, दानी तथा परम भक्त श्रावक होते थे अतः उस समय के साधुनों को एषणीय निर्दोष प्राहार मिल जाता था । किन्तु आधुनिक काल में राजविप्लवों, युद्धों, दुष्कालियों, दुस्समाकाल - के प्रभाव आदि श्रादि कारणों से अधिकांश श्रावक वर्ग दरिद्र हो गया है । ऐसी स्थिति में सुसंहनन और शक्ति विहीन साधुवर्ग को श्रद्धालु श्रावकों द्वारा साधु के लिये बनाये गये प्राहार १. जिनवल्लभ सूरि ने वि० सं० ११२५ में जिनचन्द्र सूरि द्वारा रचित "संवेगरंगशाला" नामक ग्रन्थ का संशोधन किया, इस प्रकार का उल्लेख भी उपलब्ध होता है ।
-सम्पादक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org